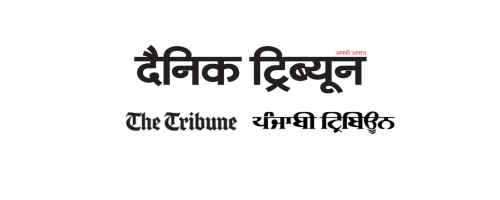कवि और आलोचक डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी से बातचीत
अरुण नैथानी
पद्मश्री डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की पहली पहचान आलोचक व कवि के रूप में रही है। वे साढ़े चार दशक से निरंतर प्रकाशित हो रही साहित्यिक पत्रिका ‘दस्तावेज’ के संस्थापक संपादक हैं। वर्ष 2013 से 2017 तक साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं। उन्हें 2011 में व्यास सम्मान तथा 2019 में ज्ञानपीठ का मूर्तिदेवी सम्मान दिया गया है। साल 1940 में कुशीनगर के रायपुर भैंसही-भेडिहारी गांव में जन्मे प्रो. तिवारी गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष रहे हैं। उन्हें मास्को में पुश्किन सम्मान समेत दर्जनों प्रतिष्ठित सम्मान मिले हैं। देश-विदेश की कई भाषाओं में उनके सृजन का अनुवाद हुआ है। उनके शोध व आलोचना के 13 ग्रंथ, छह कविता संग्रह, चार यात्रा संस्मरण, तीन लेखक संस्मरण व साक्षात्कार की चार पुस्तकें प्रकाशित हुईं। उन्होंने डायरी, आत्मकथा विधा में लिखने के अलावा करीब दो दर्जन पुस्तकों का संपादन किया। पिछले दिनों वे चंडीगढ़ में थे, उनसे हुई बातचीत :-
कविता और आलोचना की दोनों धाराओं को साधना कितना कठिन था?
जितने आलोचक हुए कवि भी हुए हैं। लेखक प्राय: कविता से ही शुरू करता है। हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल व नामवर सिंह ने कविता से शुरुआत की। विश्व स्तर पर बड़े नाम लिये जाएं तो टी.एस़ इलियट की जितनी प्रतिष्ठा कविता में है उतनी ही आलोचना में भी। उनकी कृति द वेस्टलैंड को नोबेल मिला। कविता, आलोचना में देखा जाए तो इलियट को उद्धृत करूंगा। उन्होंने कहा कि कविता में भी आलोचनात्मक प्रक्रिया चलती रहती है। आलोचना में भी एक रचनात्मक स्रोत होता है। दोनों को एक-दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि पूरक माना जाना चाहिए। यह दूसरी बात है कि कुछ लोग कविता में ही विशेष रूप से रह जाते हैं। कुछ लोग आलोचना में रह जाते हैं। कविता ही दिल के करीब है। गहरी संवेदना व सृजनात्मकता कविता में होती है।
आपकी दृष्टि में कविता क्या है?
आज तक ये सवाल सभी लोगों के सामने रहे हैं। सभी कवि व लेखकों ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल का मशहूर निबंध है ‘कविता क्या है’। इसका कोई अंतिम उत्तर तो नहीं दिया जा सकता। मेरी एक किताब ही छपी ‘कविता क्या है’, राजकमल प्रकाशन से छपी है। कविता में तीन चीजें जरूरी होनी चाहिए। एक-भाषा की सृजनात्मकता। दूसरा संवेदना और तीसरा न्याय बोध। ये तीन चीजें कविता में जरूरी हैं। कविता और गद्य में अंतर यह है कि कविता कम से कम शब्दों में प्रतीकों, बिंबों और मिथकों आदि का सहारा लेकर अपनी कथन भंगिमा को सृजनात्मक बनाती है। यानी विवरण और व्याख्या को कविता में स्थान नहीं है। कविता में कहने का ढंग महत्वपूर्ण होता है। जिसको गालिब ने अंदाज़-ए-बयां कहा है।
छंदमुक्त कविता को कैसे देखते हैं?
कविता में छंद का होना जरूरी है। छंद जरूरी नहीं कि तुक और मात्राओं में हो। संस्कृत की सारी कविता तुक और मात्राओं से अलग है। लेकिन उसमें ऐसी लय और प्रवाह है कि वह उसे छंदबद्ध करके संगीतात्मक बना देती है। जिसे नयी कविता बताया जा रहा है, उनमें अधिकांश गद्यात्मक है। उनमें छंद है ही नहीं। जिन बहुत सारी कविताओं को पत्रिकाओं में नई कविता के रूप में पढ़ते हैं, वे अधिकांश बचेंगी नहीं। उसमें कुछ ही रह जाएंगी। निराला, जिन्होंने छंदों की मुक्ति की घोषणा की, बाद में पंत जी ने भी की। दोनों छंद के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे। दोनों ने छंद में लिखा। इन्होंने छंद का विरोध नहीं बल्कि तुकबंदियों और मात्राओं को घटाने-बढ़ाने का विरोध किया। जिससे कविता बंध रही थी। भाव बंध रहे थे। छंद यानी जैसे नदी का प्रवाह होता है, वह कविता के लिये बहुत जरूरी है।
भक्तिकाल में रचनाएं छंद की बाध्यता से मुक्त थीं लेकिन उन कवियों की रचनाएं लोगों की जुबान पर चढ़ी रहीं, कैसे संभव हुआ?
छंद तो था। उस समय दोहा, चौपायी ,घनाक्षरी छंद में बंधे थे। लय और प्रवाह जिसको छंद पैदा कर देता है। लोकानुभव था जो बांधता है। तुलसी व कबीर में लोक का अनुभव गहरा था। एक सहजता थी। कृत्रिमता नहीं थी। तो केवल छंद के कारण वह कविता लोकप्रिय नहीं हुई। लोकानुभव के कारण है। मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृत्यु ही होती है। नैतिक आचरण से कैसे इसका मुकाबला किया जाये, उन भक्त कवियों ने बताया। हर मनुष्य के लिये इसलिए भी जरूरी है। इसलिए भी स्वीकार्यता बढ़ी सामाजिक नैराश्य के वातावरण में।
कविता का आज सतहीकरण किये जाने को कैसे देखते हैं जब वह विलासिता में उपजती है?
इस समय फेसबुक आदि पर कविता लिखी जा रही है, बहुत जल्दबाजी में लिखी जा रही है। और आज कविता सस्ती लोकप्रियता हासिल करने को लिखी जा रही। कविता जल्दीबाजी में नहीं लिखी जा सकती। अपनी गहरी संवेदनशीलता को भाषा का सृजनात्मक रूप देना पड़ता है। इसलिये कविता एक प्रकार से बनायी भी जाती है। कविता की सहजता का मतलब यह नहीं कि जो शब्द अनायास मन में आए उसे कविता के रूप में रख दीजिए।
आलोचना का मौजूदा परिदृश्य कैसे देखते हैं?
आलोचना का परिदृश्य अन्य विधाओं की तुलना में धुंधला दिखायी देता है। आलोचना में दलबंदी-गुटबंदी ने उसे पक्षपातपूर्ण और अविश्वसनीय बनाने का कार्य किया। जहां तक व्यावहारिक आलोचना की बात है सैद्धांतिक आलोचना को भी विचारधाराओं की कट्टरता से मुक्त होना चाहिए।
लंबे समय तक खास दृष्टिकोण के आलोचकों का वर्चस्व रहा है। क्या आलोचना के साथ न्याय हो पाया है?
जब भी किसी खास, बहुत ही कट्टर या संकीर्ण नजरिये से रचना को देखा जायेगा तो रचना की बहुआयामिता छिप जायेगी। रचनाओं के आयाम बहुत होते हैं। उनको सहानुभूति के साथ देखा जाना चाहिए। जब एक दृष्टि से देखते हैं तो अन्य आयाम छिप जाते हैं। ऐसी दृष्टि से देखी गई आलोचना ने रचनाओं के साथ न्याय नहीं किया ।
आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल व हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे आलोचक क्यों नहीं मिलते?
दोनों आलोचकों ने बड़े श्रम से साहित्य के व्यापक संस्कार प्राप्त किये। उसमें संस्कृत भाषा, अंग्रेजी व संस्कृत के साहित्य का व्यापक अध्ययन था। जिसमें व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, कालीदास जैसे महाकवियों का गहरा अध्ययन था। उन्होंने अपने आलोचना के प्रतिमान महाकाव्यों और काव्यशास्त्रीय चिंताओं से ग्रहण किये थे। इसीलिए वे आलोचक बड़े हैं। यानी आलोचना के लिये व्यापक अध्ययन जरूरी है, कविता लिखने के लिये नहीं है, तभी बड़ी आलोचना पैदा होती है।
समय बदला है, रोजगार प्राथमिकता है। छात्र मानविकी संकाय की तरफ कम जा रहे हैं। वे धीर-गंभीर अध्येता नहीं हैं। संक्रमणकाल में साहित्य की संभावना कैसे देखते हैं?
देखिये, बिल्कुल सही कहा। यह वर्तमान समय है टेक्नालॉजी का, पूंजी के प्रवाह का, भोगवाद का, उत्तर-आधुनिक समय है। इस समय में संवेदना और पुराने मूल्यों का कम होना या क्षीण होना स्वाभाविक है। मगर इसी समय साहित्य की जरूरत भी ज्यादा है। क्योंकि साहित्य ही है जो इन मूल्यों को प्रेरित कर सकता है।
कहीं न कहीं तकनीक का युग लोगों को संवेदनहीन व निर्मम बना रहा है?
इस समय दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है हिंसा। जो कट्टरता के कारण है। दूसरों के प्रति सहिष्णुता न होने के कारण। साहित्य इस हिंसा का अहिंसक प्रक्रिया से मुकाबला करता है। लेकिन बाकी सारे व्यवहार हिंसक ढंग से मुकाबला करते हैं। चारों तरफ जो हिंसा दिखायी पड़ रही है इसमें परिवर्तन होना चाहिए। साहित्य इस हिंसा को बदलने की अहिंसक प्रक्रिया है। जबकि राजनीति व अन्य चीजों में हिंसा प्रवेश कर चुकी है।
एक साहित्यकार के रूप से इस प्रक्रिया का क्या समाधान देखते हैं?
भाषा के अलावा कोई हथियार नहीं होता है साहित्यकार के पास। अत्यंत पवित्र सृजनात्मकता इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। सबसे पहले हिंसा भाषा में शुरू होती है। अगर लेखक अपनी भाषा को अहिंसक नहीं बनाता है तो बड़ी मुश्किल है। उदाहरण देखिए कि जब एक देश की टीम हारती है ताे- ‘फलां टीम को रौंदा’। हिंसा की शब्दावली से लेखक को बचना चाहिए। भाषा ही हिंसा की जमीन पर हिंसा पैदा करती है। राजनेताओं का व्यवहार देखिए, किसी के माता या पिता के बारे में ऐसी शब्दावली प्रयोग कर रहा है, जो घातक है। भाषा में हिंसा का आना खतरनाक है। चाहे बोलचाल में हो या सृजन में हो।
देश के आभिजात्य वर्ग व नेताओं के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। उसी भाषा में उनके नायक हैं, वैसी ही दृष्टि बनती है। ऐसी में भारतीय भाषाएं कितनी प्रभावी होंगी?
भारतीय भाषाओं का विकास और आदर होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। जहां तक हिंदी का सवाल है हिंदी तो अब अपनी ऊर्जा से ही आगे बढ़ेगी। अब वह ऐसी भाषा नहीं कि कोई दबा सके। अब ज्ञान-विज्ञान की चीजें उसमें आ रही हैं। भारत में अंग्रेजी को रोजगार की अनिवार्यता से खत्म कर दिया जाये तो यहां की मातृभाषाओं का विकास होगा।
साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कैसे प्रयोग किये?
मेरी कोशिश रही कि साहित्य अकादमी का विकेंद्रीयकरण हो। न केवल राजधानी बल्कि महत्वपूर्ण शहरों में उसके कार्यक्रम हों, छोटे शहरों व कस्बों में कार्यक्रम हों। साल के 365 दिन में चार सौ कार्यक्रम हुए। इसी प्रकार पुस्तकों का प्रकाशन सभी भाषाओं में हो। ये सारे कार्य रिकॉर्ड तोड़कर हुए। साहित्य अकादमी साहित्य की संस्था है तो ध्यान साहित्य पर होता है। सभी भाषाओं को आदरपूर्वक देखा जाये। चौबीस भाषाओं की अकादमी है। सभी को आदर मिले चाहे छोटी हों या बड़ी। आगे भी ऐसा हो।
साहित्य की यात्रा को किस तरह देखते हैं?
मैं संतुष्ट हूं अपनी साहित्य यात्रा से। जितना किया उतना मिला। लेखक लिखना भी बहुत अच्छा चाहता है। जितना भी लिखा उससे बेहतर लिखना चाहता है। तो ये आकांक्षा तो अभी बनी हुई है।
साहित्यकारों के साथ दिक्कत रही कि साहित्य साधना में शरीर की अनदेखी करते हैं? आप क्या करते हैं?
कोशिश तो करता हूं। स्वास्थ्य की गड़बड़ियां रहती हैं। सूक्तियों में कहा गया है स्वास्थ्य ठीक रहे तो धर्म की साधना हो पाती है। स्वस्थ रहने के लिये कोशिश करता हूं मगर जैसे कि कसरत टहलना नियमित नहीं। बहुत ही शुद्ध शाकाहारी और सादा भोजन करता हूं।