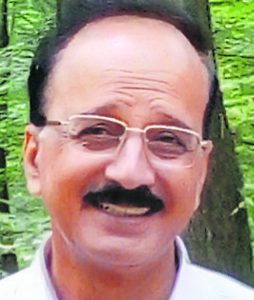तरक्की के आंकड़ों संग सुधरे देश की सेहत
देविंदर शर्मा यदि आजादी के 76 साल बाद भी, 74 फीसदी से भी अधिक भारतीय स्वास्थ्यवर्धक भोजन का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं तो कुछ तो है जो गलत हो रहा है। यह भी तब जबकि देश दुनिया की...
देविंदर शर्मा
यदि आजादी के 76 साल बाद भी, 74 फीसदी से भी अधिक भारतीय स्वास्थ्यवर्धक भोजन का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं तो कुछ तो है जो गलत हो रहा है। यह भी तब जबकि देश दुनिया की सबसे तेज गति से तरक्की कर रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और संवृद्धि दर अनुमानों के लिहाज से जिन्हें यह लगभग हासिल कर ही लेगा, लगभग 2027 तक भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था का आकार जो भी हो, और वह भी अधिकांश अस्वस्थ आबादी से निर्मित हो तो वह इस बात का स्पष्ट संकेतक है कि ग्रोथ मैट्रिक्स यानी संवृद्धि का सांचा देश के स्वास्थ्य से मेल नहीं खाता है।
यह निश्चित तौर पर चिंताजनक है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ की अवधि पांच साल और बढ़ाने की घोषणा की, जिसके तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिलना जारी रहेगा, तो इससे पूरी तरह स्पष्ट था कि सरकार ने जरूरत समझी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत निर्धारित 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर सब्सिडी वाले खाद्यान्न, जिसके हकदार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, के अलावा 5 किलोग्राम मुफ्त राशन भी दिया जाये। क्योंकि एनएफएसए आबादी के 67 प्रतिशत हिस्से की जरूरत पूरी करता है, इसके साथ ही अन्य 10 फीसदी भाग ऐसा है जिसके खुराक के स्तर को बेहतर बनाने की तुरंत जरूरत है।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने अपने खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्रीय अवलोकन 2023 में ये हैरान कर देने वाले आंकड़े उजागर किये। यह वर्ष 2021 के लिए अनुमानों पर आधारित था, जो महामारी का साल था, परंतु अध्ययन बताता है कि क्षेत्र का उसी तरह के प्रभावों के फैलाव से ग्रस्त रहना जारी है। निराशाजनक रूप से, रिपोर्ट बताती है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पोषण के लिहाज से 37.07 करोड़ गरीब लोग मौजूद हैं जो वैश्विक स्तर पर कुपोषित जनसंख्या के आधे से ज्यादा है। भारत के अलावा पाकिस्तान में 82.8 प्रतिशत और बांग्लादेश में 66.1 फीसदी आबादी कुपोषित है। जबकि नेपाल में 76.4 फीसदी, श्रीलंका में 55.5 फीसदी और भूटान में 45.2 प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण से ग्रस्त है। इस तरह से दक्षिण एशियाई क्षेत्र वैश्विक अल्पपोषित मानचित्र पर हावी है।
एफएओ की रिपोर्ट यह भी बताती है कि देश की 53 प्रतिशत महिलाओं में रक्ताल्पता की समस्या है, और पांच साल से कम आयु के 31.7 फीसदी बच्चों की हाइट उम्र के लिहाज से कम है, इसके साथ ही 18.7 प्रतिशत बच्चों का वजन तकनीकी तौर पर उनकी ऊंचाई के अनुरूप कम है। रोचक बात यह है कि यही अनुमान पूर्व में वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआई) में चिन्हित किये गये थे जिन्हें भारत ने यह कहकर नकार दिया था कि इनके लिए अपनाई गयी कार्यप्रणाली सही नहीं है। जबकि एफएओ का कहना है कि जब तक बढ़ रही आय का स्तर बढ़ रही खाद्य कीमतों के बराबर नहीं होता है, अस्वास्थ्यकर भोजन की प्रवृत्ति घटेगी नहीं।
जहां तक आय स्तर का संबंध है तो भारत की अधिकांश जनसंख्या लगातार उस स्तर पर है जो सब-सहारा अफ्रीका में मौजूद है। देश के एक अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र में 10 अगस्त, 2022 में प्रकाशित लेख ‘फोकस ऑन द बेस ऑफ ए पिरामिड’ में ये अनुमान था कि 90 करोड़ भारतीय उतनी ही आय में निर्वाह कर रहे थे जितनी आमदन सब सहारा अफ्रीका में है। इतने निम्न आय स्तर के साथ, जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि के बावजूद जारी है, अस्वास्थ्यकर खुराक कायम रहेगी। इसे प्रमाणित करने के लिए, विश्व बैंक की हालिया गणना से मालूम हुआ कि ब्रिक्स देशों में, भारत की 91 प्रतिशत आबादी 280 रुपये रोजाना (4 डॉलर प्रतिदिन) से कम में जीवन यापन करती थी। यह वृद्धिमान अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है, इतने ही आय स्तर पर 51 प्रतिशत आबादी के साथ दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर आता था।
स्वास्थ्यकर खुराक प्राप्त करने को लेकर, जवाब यही है कि पिरामिड की सतह पर प्रचलित आय स्तर को बढ़ाया जाये। यह मुश्किल लगता है, और कुछ तो इसे असंभव ही कहेंगे, पर हकीकत में औसत आय स्तर को बढ़ाना कठिन नहीं है। मैंने अकसर कहा है कि चूंकि ग्रामीण परिवारों का करीब 70 फीसदी हिस्सा कृषि पर आश्रित है तो खेती को व्यवहार्य और लाभकारी उद्यम बनाने में ही इसका जवाब निहित है। कृषि क्षेत्र में कार्यरत जिस 47 फीसदी कार्यबल को व्यवहार्य आय स्तर से लगातार वंचित रखा जा रहा है, वे कभी पोषण से भरपूर आहार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कई अध्ययनों ने इंगित किया कि ग्रामीण मजदूरी जो किसी भी रूप में निम्नतम है, फिर से कम हुई या स्थिर रही। और जब गरीब परिवारों में आय कम होती है तो वे अपने द्वारा लिये जाने वाले भोजन में ही कटौती करते हैं।
महंगाई नियंत्रण के मकसद से कृषि क्षेत्र को जानबूझकर दरिद्र बनाये रखने के चलते मैक्रो इकनॉमिक नीतियों ने कृषि को व्यवहार्य विकल्प बनाने के प्रयासों को दबा दिया है। यह मुझे राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर एक त्रुटिपूर्ण ग्रंथ की याद दिलाता है जिसे नीति आयोग ने साल 2020 में देशभर में एक आम आदमी द्वारा भुगतान की जाने वाले भोजन (थाली) की लागत को मापने के मकसद से तैयार किया था। द ट्रिब्यून में 8 फरवरी, 2020 को प्रकाशित मेरे एक लेख ‘थाली इकोनॉमिक्स गेट्स इट रॉन्ग’ में मैंने व्याख्या की है कि कैसे थाली इकोनॉमिक्स, जैसा कि इसे कहा गया, केवल यह संदेश देने के लिए थी कि खाद्य कीमतें एक औसत आदमी की पहुंच में हैं। असल में, रिपोर्ट में यह बात चतुराई से छुपा ली गयी थी कि सस्ते खाद्यान्न उगाने के लिए किस तरह से किसानों को ‘दंडित’ किया जा रहा है।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल इंडिया मासिक आधार पर विश्लेषण करती है, और मैंने देखा कि फोर्ब्स इंडिया मैगज़ीन ‘हाउ इंडिया ईट्स’ शृंखला के तहत प्रकाशित करती है। कई दूसरे अखबार भी रिपोर्ट को नियमित तौर पर छापते हैं। सितंबर, 2023 के लिए विश्लेषण के मुताबिक, प्याज-टमाटर के दाम कम होने से औसतन एक शाकाहारी थाली की लागत 27.9 रुपये थी। यह लागत उससे 17 फीसदी कम थी जो एक माह पहले एक आम शहरी को घर पर भोजन तैयार करने में पड़ती थी। इसी तरह नॉन-वेजिटेरियन थाली की लागत आंकी गयी।
यह देखते हुए कि एफएओ के खाद्य और कृषि की स्थिति (एसओएफए) 2023 के मुताबिक खाद्य उत्पादन की वैश्विक लागत 12.7 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है, और भारत में छिपी हुई लागत 1.1 ट्रिलियन डॉलर मापी गई है, तो अब वक्त आ गया है कि क्रिसिल के मासिक अनुमानों पर रोक लगायी जाये। हर माह वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन थाली का चार्ट सामने लाकर असल में क्रिसिल सेहतमंद व खरे खाद्य पदार्थ पैदा करने की लागत को छुपा रही है। यह ध्यान में रखते हुए कि भारत में 74 फीसदी लोग स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन का खर्च उठाने में समर्थ नहीं हैं तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से व्याख्या करने के लिए जरूर कहना चाहिये कि यदि अस्वस्थ जनसंख्या का बढ़ना जारी है तो उसके द्वारा लागत को प्रदर्शित करने के प्रयास कितने प्रासंगिक हैं। किसी देश के लिए विकास का अंतिम मापक एक सेहतमंद राष्ट्र होना चाहिये।
लेखक कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञ हैं।