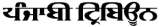राष्ट्रहित में नहीं भाषाई अस्मिता की जंग
हम किसी को इसलिए ‘सज़ा’ का पात्र न मान लें कि वह हमारी भाषा नहीं जानता। पिछले कुछ दिनों में मुंबई में भाषा के जानने, न जानने को लेकर जिस तरह मारपीट की घटनाएं हुई हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं...
हम किसी को इसलिए ‘सज़ा’ का पात्र न मान लें कि वह हमारी भाषा नहीं जानता। पिछले कुछ दिनों में मुंबई में भाषा के जानने, न जानने को लेकर जिस तरह मारपीट की घटनाएं हुई हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई किसी भाषा को नहीं जानता इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाना चाहिए कि वह उस भाषा का अपमान कर रहा है।
पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले एडवोकेट उज्ज्वल निकम को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। निकम के अनुसार यह सूचना उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने टेलीफोन पर संपर्क करके दी थी। प्रधानमंत्री ने फोन पर एडवोकेट निकम से कहा था, ‘मी मराठी बोलूं का हिंदी?’ इस पर निकम कुछ हंस दिये, पर प्रधानमंत्री ठहाका लगाकर हंसे थे। वैसे प्रधानमंत्री का मराठी में बोलना और निकम एवं मोदी जी का हंसना स्वाभाविक-सी बात है, पर हाल के दिनों में महाराष्ट्र में भाषा की जो राजनीति चल रही है उसे देखते हुए यह प्रकरण सामान्य से थोड़ा हटकर लग रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा निकम के साथ मराठी में बोलने वाली यह बात जिस दिन अखबार में छपी, उस दिन एक अन्य समाचार भी अखबार के पहले पृष्ठ पर छपा था। यह समाचार मुंबई के उपनगर विरार का था, जहां उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक रिक्शा वाले की इसलिए पिटाई कर दी कि वह मराठी में नहीं बोल पा रहा था– हिंदी में बोल रहा था। रिक्शा चालक उत्तर प्रदेश का था और शिवसेना के कार्यकर्ताओं का मानना था कि उसे अपनी कर्मभूमि की भाषा मराठी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी न बोल पाना मराठी भाषा का अपमान कैसे हो गया, पता नहीं, पर प्रधानमंत्री द्वारा एडवोकेट निकम से मराठी में बोलना यह संकेत तो दे ही रहा है कि राज्य में भाषा को लेकर फिर से उठा यह विवाद अप्रिय स्थितियां उत्पन्न कर रहा है।
महाराष्ट्र में आकर जीविका कमाने वाले को राज्य की भाषा आनी चाहिए, इस बात से किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सच बात तो यह है कि एक से अधिक भारतीय भाषाएं जानने वाले भारतीय को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि वह बहुभाषी है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र नहीं है, भाषा हमारी अस्मिता है, पहचान है। हमारे संविधान में हिंदी को देश की राजभाषा का स्थान दिया गया है, लेकिन संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित की गयी सभी बाईस भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं। सब पर हमें गर्व है। इनमें से किसी एक का भी अपमान समूची भारतीयता का अपमान है। अर्थात् स्वयं अपना अपमान। कोई क्यों करना चाहेगा भला अपना अपमान? सच तो यह है कि अपनी भाषाई विविधता पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। भाग्यशाली हैं हम कि हमारे पास भाषाओं का इतना बड़ा खज़ाना है।
हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि यह अहसास हम सब में जगे। लेकिन यह भी एक पीड़ादायक सच्चाई है कि अक्सर भाषा को राजनीति का हथियार बनाया जाता है। महाराष्ट्र में इन दिनों चल रहे भाषाई-विवाद के पीछे भी कुछ ऐसी ही राजनीति है। कुछ अरसा पहले महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा-नीति में परिवर्तन संबंधी शासनादेश जारी किया था, जिसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि प्राथमिक कक्षाओं में तीन भाषाएं पढ़ाई जाएं– मातृभाषा यानी मराठी, अंग्रेजी और हिंदी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को यह राजनीतिक स्वार्थ साधने का अवसर दिखा। उसने इसे हिंदी-मराठी का विवाद बना दिया और तरीका वही अपनाया जो बीस साल पहले आजमाया जा चुका था– यानी मराठी माणूस और मराठी अस्मिता की बात। साथ ही जोर-जबरदस्ती वाली नीति। उद्धव ठाकरे को भी इसमें अवसर दिख गया। मराठी के अपमान का नारा लगाकर राजनीति सधने लगी। राजनीतिक स्वार्थ का ही तकाज़ा था कि महाराष्ट्र सरकार को भी तीन भाषाओं वाला शासनादेश वापस लेना पड़ा। अब एक समिति बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। पर मुद्दे की आंच ठंडी नहीं हुई। उज्ज्वल निकम से प्रधानमंत्री का हल्के-फुल्के अंदाज में पूछा गया भाषा वाला सवाल और विरार में रिक्शा चालक की पिटाई वाला प्रकरण इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भाषाई-विवाद वाली राजनीति की आंच अभी सुलग रही है और इसे अभी और सुलगाया जायेगा। ‘मनसे’ और ‘उबाठा’ की कोशिश रहेगी कि मुंबई महानगरपालिका समेत राज्य में नगर निकायों के चुनाव तक यह आंच सुलगती रहे, ताकि उनकी राजनीति की रोटियां सिकती रहें। पहले भी समय-समय पर स्थानीय और पर प्रांतियों का मुद्दा राजनीति का हथियार बनता रहा है, अब भी बनेगा। इसका किसको कितना लाभ मिलेगा, यह तो भविष्य ही बतायेगा, पर भाषाई अस्मिता और प्रांतीयता के नाम पर लड़ी जा रही यह लड़ाई किसी भी दृष्टि से राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं कहीं जा सकती।
महाराष्ट्र की राजनीति में अपना स्थान खोजती ‘मनसे’ और अपना खोया स्थान फिर से प्राप्त करने की कोशिश में लगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को इस ताज़ा विवाद के सहारे जुड़ने का मौका भले ही मिल गया हो, पर राष्ट्रीय हितों को देखते हुए भाषाई अस्मिता के नाम पर लड़ी जा रही इस लड़ाई का समर्थन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि यह राजनीति और भाषा के नाम पर लड़ी जाने वाली लड़ाई सिर्फ महाराष्ट्र में ही हो रही है। देश के अन्य राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु, कर्नाटक, असम आदि में भी इस तरह की विभाजनकारी प्रवृत्तियां समय-समय पर सिर उठाती रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे राजनेता अपनी राजनीति को चमकाने की इस राष्ट्र-विरोधी प्रवृत्ति से उबरें।
यह राष्ट्र हम सब का है। हम यानी हम सब भारतीयों का। हमारा संविधान देश के हर नागरिक को देश में कहीं भी जाने-बसने का अधिकार देता है। भाषा, धर्म, जाति आदि के नाम पर देश के किसी भी नागरिक से उसके वे अधिकार छीनने की कोशिश स्वीकार्य नहीं हो सकती जो संविधान ने उसे दिये हैं।
यह सही है कि देश की सारी भाषाएं हम सब की हैं फिर भी क्षेत्र-विशेष की अपनी मातृ-भाषा के प्रति अनुराग और गर्व का भाव होना ग़लत नहीं कहा जा सकता। पर हमारी भाषाएं हमारे आंगन की दीवार नहीं हैं, पुल हैं हमारी भाषाएं जो हमें एक-दूसरे से जोड़ती हैं। यहीं इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि हिंदी को मात्र इसी आधार पर राजभाषा का दर्जा दिया गया था कि देश की बहुत बड़ी आबादी हिंदी बोलती-समझती है। जहां तक प्राचीनता और समृद्धि का सवाल है तमिल, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं हिंदी से कहीं अधिक समृद्ध हैं। अपनी सब भाषाओं के प्रति हम में आदर का भाव होना चाहिए। इसी आदर का यह भी तकाज़ा है कि हम किसी को इसलिए ‘सज़ा’ का पात्र न मान लें कि वह हमारी भाषा नहीं जानता। पिछले कुछ दिनों में मुंबई में भाषा के जानने, न जानने को लेकर जिस तरह मारपीट की घटनाएं हुई हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई किसी भाषा को नहीं जानता इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाना चाहिए कि वह उस भाषा का अपमान कर रहा है। किसी भाषा को न सीख पाने के भी कई कारण हो सकते हैं। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि हम जितनी भाषाएं सीख सकें, सीखें। विनोबा भावे अनेक भाषाएं जानते थे, 46 वर्ष की आयु में उन्होंने अरबी और फारसी सीखी थी। जीवन के अंतिम दिनों में वह जापानी भाषा सीख रहे थे! मराठी उनकी मातृभाषा थी पर उन्होंने कभी किसी से अपेक्षा नहीं की कि वह उनकी भाषा में पारंगत हो। हां, वे स्वयं अवश्य कई भाषाओं में पारंगत हो गये थे।
बहरहाल, भाषा के नाम पर जिस तरह देश में द्वेष का वातावरण पनप रहा है, वह किसी भी विवेकशील नागरिक की चिंता का विषय होना चाहिए। किसी रिक्शा वाले को, किसी दुकानदार को, किसी सरकारी कर्मचारी को ‘कान के नीचे बजाने’ की भाषा में धमकी देना किसी भी दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता। भाषा की अपनी मर्यादा होती है उसका पालन होना ही चाहिए। भाषा के नाम पर की जाने वाली राजनीति को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, इस राजनीति की भर्त्सना ज़रूरी है। आज भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में जो कुछ रहा है, उसके औचित्य पर सवालिया निशान लगना ही चाहिए और उत्तर हर विवेकशील नागरिक को देना है।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।