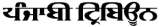अवसरवादिता का शिकार होने की नियति
विश्वनाथ सचदेव हमारे समय के शीर्ष व्यंग्यकारों में से एक हरिशंकर परसाई का एक बहुचर्चित व्यंग्य है- प्रजावादी समाजवादी। इस लेख में उन्होंने दशकों पहले राजनीति के दलबदलू का एक चित्र खींचा था और आश्चर्य किया था इस बात पर...

हमारे समय के शीर्ष व्यंग्यकारों में से एक हरिशंकर परसाई का एक बहुचर्चित व्यंग्य है- प्रजावादी समाजवादी। इस लेख में उन्होंने दशकों पहले राजनीति के दलबदलू का एक चित्र खींचा था और आश्चर्य किया था इस बात पर कि दक्षिण और उत्तरी ध्रुव जैसी बात करने वाले सत्ता के लिए कैसे एक-दूसरे से मिल लेते हैं? कैसे बड़ी आसानी से धुर-विरोधी सिद्धांतों-नीतियों की बात करने वाले बिना किसी संकोच के एक-दूसरे के अपने हो जाते हैं। परसाई के उस आलेख की शुरुआत एक ऐसे ही राजनेता के आत्मालाप से होती है, जो जयप्रकाश नारायण के चित्र के सामने खड़ा हो रो रहा था, प्रलाप कर रहा था। पूछने पर वह बताता है कि प्रलाप का यह कार्यक्रम रोज़ चलता है, बस आधार बदल जाता है। कभी उसका रोना होता है जयप्रकाश नारायण के सामने, कभी राजाजी के सामने और कभी गुरु गोलवलकर के सामने। उसके कमरे में देश के अलग-अलग दलों के नेताओं की तस्वीरें टंगी थीं।
नेहरू के चित्र के सामने खड़ा होकर वह प्रलाप करता, ‘अवाडी कांग्रेस में तुमने हमारा समाजवाद ही छीन लिया। 1947 में ही कह देते तो हम कोई और पार्टी देख लेते। जनसंघ में ही चले जाते।’ समाजवाद और जनसंघ के बेमेल समझौते के बचाव में उनका तर्क था- ‘यह शब्द पुराने पड़ गये हैं। पार्टी का कोई नाम तो होना चाहिए, इसलिए हमने यह नाम रख लिया। मूल मंतव्य है सत्ता हासिल करना...’ फिर इन नेताजी ने कहा था, ‘जो सरकार बनाने वाला हो, उसके साथ रहना चाहिए।’ परसाई के इस आलेख में जैसे भविष्य के भारत का एक नक्शा दिख रहा था।
सोच रहा था अगर परसाई जी आज होते तो इस लेख में क्या लिखते? वही सब लिखते जो दशकों पहले लिखा था। बस व्यक्तियों और पार्टियों के नाम बदल जाते। वही सब जो उन्होंने तब लिखा था, आज भी देश की राजनीति में हो रहा है। परसाई के नेताजी को तो फिर भी शर्म आती थी। वे नहीं चाहते थे कि सत्ता के लिए रोने-गिड़गिड़ाने वाला उनका चेहरा बाहर लोगों को दिखाई दे। पर सत्ता की राजनीति में लिप्त आज के नेता तो ऐसा कोई झीना-सा पर्दा भी नहीं चाहते। सारा खेल ‘खुल्ला फर्रुखाबादी’ है। दल-बदलने में किसी को ज़रा-सा भी संकोच नहीं होता। शर्म आने की बात तो बहुत बाद की है।
वैसे यह दलबदल वाली बात मुझे उत्तर प्रदेश के एक नेता जी के भाजपा के साथ जुड़ने की खबर से याद आयी। राजभर नाम है इन नेताजी का। कुछ अर्सा पहले भी वे भाजपा के एनडीए में थे। फिर उन्हें सत्ता में आने के ज्यादा अवसर अखिलेश यादव के दल में दिखे। वह समाजवादी दल में आ गये। बात बनी नहीं वहां। अब वे फिर भाजपा की शरण में आ गये हैं। सिद्धांतों की, मूल्यों की कोई बात नहीं। बात सिर्फ सत्ता की है, सत्ता से जुड़ने की है। शर्म न उन्हें आ रही है और न भाजपा को। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही खेल चल रहा है-- तीन-चार साल पहले रात के अंधेरे में राष्ट्रवादी पार्टी के अजित पवार भाजपा के फड़नवीस से जाकर मिले और सुबह सूरज उगने के पहले ही राजभवन में जाकर दोनों ने सरकार बनाने की शपथ भी ले ली! पर कमाल यह नहीं था, कमाल तो यह था कि उपमुख्यमंत्री बनने के सिर्फ 72 घंटे बाद अजित पवार फिर अपने चाचा के दल में लौट आये। इस नाटक की उपलब्धि यह थी कि सत्तर हज़ार करोड़ के घपले का उन पर लगाया गया आरोप वापस ले लिया गया था। ज्ञातव्य है कि इससे पहले भाजपा नेता फड़नवीस उन्हें जेल में चक्की पीसने की धमकी दे रहे थे। यह धमकी साथ मिलकर सरकार बनाने से पहले की थी। तीन साल बाद फिर महाराष्ट्र में भाजपा सत्ता में आयी तो अब फिर राष्ट्रवादी दल के नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस बार आरोप स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने लगाया। आरोप लगाने के और अपराध की सजा देने की गारंटी देने के दो दिन बाद ही अजित पवार फिर भाजपा के साथ मिलकर सत्ता में पहुंच गये। शर्म इस सारे नाटक के किसी भी पात्र को नहीं आ रही।
हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे राजनेता किसी भी प्रकार की शर्म से स्वयं को उबरा हुआ मानने लगे हैं। गालिब की पंक्ति में थोड़ा परिवर्तन करके कहने का मन करता है- शर्म इनको मगर नहीं आती।
यह शर्म तब भी नहीं आती थी, जब परसाईजी ने लिखा था, इस्तीफा मांगना उन नेताजी का सार्वजनिक मामला था, और सत्ता में हिस्सा मांगना ‘प्राइवेट’ है- ‘बाहर वीर रस होता है, भीतर करुण रस’। सच बात तो यह है कि सिद्धांत और मूल्य-विहीन राजनीति के इस खेल में घाटा सिर्फ उस मतदाता का होता है, जो अपने वोट से सरकार बनवाता है। उसके बाद तो सब कुछ सरकार बनाने वाले के हाथ में चला जाता है। जनतंत्र को जनता का राज कहा जाता है। पर यह राज उसी क्षण का होता है जब मतदाता वोट दे रहा होता है। उसके बाद तो उसे यह पूछने का हक भी नहीं होता कि नेताजी मैंने तो आप की नीतियों, घोषणाओं और सिद्धांतों के लिए आपको वोट दिया था, और आप बिना कुछ पूछे ही चुपचाप उन नीतियों, घोषणाओं और सिद्धांतों के विरोधियों के साथ चले गये?
आये दिन हमारे राजनेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पाले में आते-जाते दिखते हैं। और यह प्रवृत्ति किसी एक दल के नेताओं में नहीं है। सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। हमारी सारी राजनीति सत्ता का घटिया खेल बनकर रह गयी है और इस खेल में वास्तविक हार उस आम नागरिक की होती है जिसे जनता की जगह प्रजा बना कर रख दिया गया है। इस नागरिक को खुले सपने दिखाकर भरमाया जाता है, और फिर अगले चुनाव आने तक वह अपने आप को कोसता ही रह जाता है।
दल-बदल की एक बीमारी का शिकार होता जा रहा है हमारा जनतंत्र। सिर्फ सत्ता के लिए की जाने वाली राजनीति में जनतंत्र एक मिथ्या शब्द बनता जा रहा है। यह स्थिति नेताओं को रास आती है, पर इस स्थिति को बदलने का दायित्व देश के नागरिक का बनता है। मेरा और आपका दायित्व है यह। हमें अपने सिद्धांतहीन, दलबदलू नेताओं से पूछना होगा कि स्वयं को जनता का सेवक कहते-कहते वे स्वयं को राजा क्यों समझने लगते हैं? यह क्यों मान लेते हैं कि उनके पाप की कालिख किसी को नहीं दिखेगी और उनकी अवसरवादी राजनीति को जनतंत्र की जनता चुपचाप स्वीकारती-सहती रहेगी? वैसे, यह सवाल हमें स्वयं से ही पूछना चाहिए कि हम कब तक राजनेताओं की अवसरवादिता के शिकार होते रहेंगे?
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।