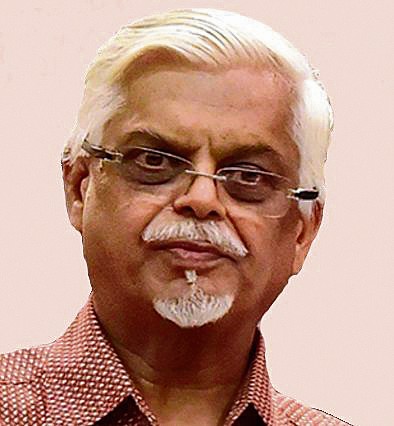संबंध बहाली के लिए सेनाएं पीछे हटाने पर सहमति
संजय बारू राजनयिक और राष्ट्रों के बीच संबंधों के जारी हालात पर टिप्पणी की पेशकश करने वाले लोग सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच हुए समझौते के विवरण पर ध्यान देने के अभ्यस्त हैं। कज़ान (रूस) में अपनी...
संजय बारू
राजनयिक और राष्ट्रों के बीच संबंधों के जारी हालात पर टिप्पणी की पेशकश करने वाले लोग सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच हुए समझौते के विवरण पर ध्यान देने के अभ्यस्त हैं। कज़ान (रूस) में अपनी बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीजों को बृहद परिदृश्य में रखकर देखा और एक दूरंदेशी ब्यान पर हस्ताक्षर किए। हो सकता है विवरण के विस्तार में कुछ छिपी चालाकियां हों, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों में बात जिससे बिग़ड़ती है, वह है जमीनी हकीकत और ऐतिहासिक दावों के बीच का फर्क। उस अंतर को पाटने का काम किसी और दिन के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। शायद, किसी और युग के लिए। फिलहाल तो, दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि उनके सैनिक पीछे हटेंगे ताकि देशों में फिर से जुड़ाव बन सकें।
अंतिम सीमा समझौता पारस्परिक सहमति से केवल सीमा की निशानदेही करना नहीं है। यह सही मायने में तभी होगा जब दोनों मुल्क अपने-अपने आधिकारिक एवं अधिकृत नक्शों में बदलाव करने को राज़ी हों। परंतु, न तो प्रधानमंत्री मोदी और न ही राष्ट्रपति जिनपिंग अपने लोगों को देश का नया मानचित्र पेश करने की स्थिति में हैं। वह दिन आने तक, शांति और सौहार्द बनाए रखना पड़ेगा।
चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ करना राष्ट्रपति जिनपिंग की अदूरदर्शिता और हनक का नतीज़ा था। क्या पता इसके पीछे की वजह 2014-19 के दौरान आयोजित तीन शिखर बैठकों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनके प्रति दर्शाई अतीशयी भंगिमा रही हो। उम्मीद है कि दोनों ने अपने-अपने सबक सीख लिए होंगे। कज़ान में हुई बैठक से पता चलता है कि दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के देश के बारे में जो आकलन किया है, उसमें हकीकत का ख्याल अधिक रखा गया है। दोनों नेताओं ने स्थिर, पूर्वानुमानित और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है और उम्मीद जताई है कि वे ‘बहुध्रुवीय एशिया और बहुध्रुवीय दुनिया’ के निर्माण में योगदान देंगे। उन्होंने विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए संबंधों के लिए दीर्घकालिक और रणनीतिक पहलू की आवश्यकताओं पर जोर दिया।
पांच साल पहले जब महाबलीपुरम में मोदी और शी की मुलाकात हुई थी, तब से लेकर दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई है। भारत चाहेगा कि जिनपिंग-युग से पहले रही अपेक्षाकृत स्थिरता वाले माहौल की वापसी हो जाए, लेकिन वक्त को पूरी तरह पीछे नहीं मोड़ा जा सकता। सीमा मुद्दे के प्रबंधन पर, राजीव गांधी-देंग शियाओपिंग के बीच बनी समझ - यहां तक कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान संवाद भी - जो शक्ति समीकरण को परिभाषित करने के लिए जानी गयी, वह पिछले दो दशकों में चीन के तेजी से बढ़ते कद के कारण बाधित हो गई। शी जिनपिंग ने भारत और दुनिया पर प्रभाव जमाने की कोशिश की है।
भारतीय राजनीतिक और रणनीतिक नेतृत्व इस बदले हुए शक्ति समीकरण को समझने से बचते रहे और चीन पर दबाव बनाने के मंतव्य से संयुक्त राज्य अमेरिका के पाले में जुड़ने की कोशिशें की। हालांकि, पश्चिमी जगत का इस किस्म का समर्थन करने की कीमत भी है, जिसे चुकाने को लगता है मोदी सरकार तैयार नहीं है। महज चीन विरोधी गठबंधन का हिस्सा बनने का जोखिम उठाने के बजाय, मोदी ने अमेरिका और यूरोप के साथ संबंध मजबूत बनाए रखते हुए चीन-रूस के साथ भी रिश्ते बेहतर बनाने वाला विकल्प चुना। व्यावहारिक रूप से यही है बहु-मित्रता।
एक ऐसा तरीका जिसमें भारत में चीन के निवेश को अनुमति देकर संबंधों को एक प्रकार से सामान्य दिखाना। चीन की अर्थव्यवस्था पूंजी-बहुल है, हालांकि अब धीमी पड़ रही है। जबकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसे तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की जरूरत है, विशेषकर विनिर्माण में। चीनी निवेश में बढ़ोतरी होने से, चीन के पक्ष में जो व्यापार असंतुलन है, उसे कुछ हद तक ठीक करने में भी मदद मिल सकेगी। इस साल की शुरुआत में, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया था कि वैश्विक और क्षेत्रीय भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक संदर्भों को देखते हुए, भारत को चीन के साथ किस किस्म के आर्थिक संपर्क रखने चाहिए।
सर्वेक्षण में पूछा गया कि ऐसे वक्त पर, जब कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं चीन से ‘जोखिम कम करने’ के प्रयास में हैं और चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने के साथ उसकी नई ‘चीन प्लस वन’ रणनीति अपनाने की कोशिश में हैं, भारत के पास कौन से अवसर उपलब्ध हैं? यहां यह बात सही ढंग से समझी गई है कि दुनिया भर की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं चीन से ‘परे नहीं हट रहीं’ बल्कि सिर्फ ‘जोखिम कम’ कर रही हैं।
सर्वेक्षण में यह भी पूछा गया : ‘क्या ‘चीन प्लस वन’ नीति के परिणामस्वरूप चीन से व्यापारिक लेन-देन पूरी तरह खत्म हो जाएंगे’? तो उत्तर था कि यह नहीं होगा। मेक्सिको, वियतनाम, ताइवान और कोरिया जैसे देश इसका उदाहरण हैं, जो चीन से अमेरिका का व्यापार घटने के प्रत्यक्ष लाभार्थी रहे। जहां ये मुल्क अमेरिका को निर्यात में अपनी भागीदारी बढ़ाने में लगे थे वहीं उन्होंने अपने मुल्क में चीन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। इसलिए, भले ही अपनी ‘चीन प्लस वन’ नीति को बढ़ावा देने में लगी है, दुनिया उसको पूरी तरह नजरअंदाज करना गवारा नहीं कर सकती’।
यह वह आकलन है जो सर्वेक्षण की समझ को आगे परिभाषित करता है। इसमें आगे पूछा गया कि क्या चीन की आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बने बिना, भारत का वैश्विक आपूर्ति शृंखला में बने रहना संभव है? चीन से वस्तु आयात और पूंजी आयात के बीच सही संतुलन क्या हो? सर्वेक्षण तब सुझाव देता है कि ‘भारतीय विनिर्माण को गति देने और भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बनाए रखने के लिए, यह अपरिहार्य है कि भारत खुद को चीन की आपूर्ति शृंखला में शामिल करे’। चाहे हम ऐसा केवल आयात पर निर्भर करके करें या आंशिक रूप से चीनी निवेश के माध्यम से, ये वह विकल्प हैं जो भारत को चुनने हैं’।
सर्वेक्षण की अपनी संस्तुति यह थी कि भारत को घरेलू विनिर्माण में चीनी निवेश की अनुमति देते हुए ठीक इसी दौरान उससे आयात को घटाना चाहिये। केवल व्यापार पर निर्भर रहने की बजाय ‘चीन प्लस वन’ नीति को लाभ उठाने का औजार बनाया जाए, लिहाजा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आमद वाला रास्ता चुनना अधिक फायदेमंद होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन भारत का शीर्ष आयात भागीदार है, और उसके साथ व्यापार असंतुलन बढ़ता जा रहा है। चूंकि अमेरिका और यूरोप अपना फौरी आयात चीन की बजाय कहीं और से कर रहे हैं, इसलिए चीनी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करना और फिर यहां उत्पादित वस्तुओं को उनके बाजारों में निर्यात करना अधिक प्रभावी होगा, बजाय इसके कि चीन से बना-बनाया माल आयात कर, मूल्य में न्यूनतम बढ़ोतरी करके, उसे पुनः यूरोप-अमेरिका निर्यात करें’।
यह दलील काफी समझदारी भरी है और भारत के अपने हित पर आधारित है। लेकिन तब यह सवाल उठता है कि भारत और चीन ऐसे समय में सामान्य आर्थिक संबंध कैसे आगे बढ़ा सकेंगे जबकि राजनीतिक रिश्ते ‘सामान्य’ नहीं हैं और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की कार्रवाइयों से अस्थिर बने हुए हैं। इसी संदर्भ में, दोनों देशों ने सामान्य आर्थिक संबंधों की बहाली को बल देने के वास्ते सीमा विवाद मुद्दे पर अपनी स्थिति को तूल न देकर अक्लमंदी से काम लिया है।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।