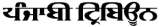डॉ. विमल कालिया ‘विमल’
स्टेज पर से पर्दा उठा। नृत्य नाटिका का अंतिम दृश्य था। कथकली के पात्र, अपने भारी-भरकम वस्त्रों में, उससे भी भारी मुकुटों और मुखौटों में, और चेहरे पर मेकअप की भारी परतों के बीच से, अपनी काजल से सजी आंखों से भाव-भंगिमाएं बनाते हुए, मृदंग और घंटी की थाप पर थिरकते हुए स्टेज पर आ गये।
नरसिंह अवतार अपने रौद्र रूप में स्तंभ से प्रकट हुए। उनका रूप भय पैदा करने वाला था। सिर शेर का और शरीर मनुष्य जैसा। आधे सिंह और आधे मानव को सामने देख, हिरण्यकश्यप पीछे हट गया। उसे तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, जो उसने मांगा था।
‘न मुझे मनुष्य मार सके और न ही जानवर,
न मुझे कोई दिन में मार सके और न ही रात में,
न मुझे कोई आकाश में मार सके और न ही पृथ्वी पर,
न मुझे कोई घर में मार सके और न ही घर से बाहर
न कोई मुझे अस्त्र से मार सके और न कोई शस्त्र से।’
वह डर कर भागने लगा। नरसिंह उसे घसीटते हुए दरवाजे की चौखट तक ले गये। वह न घर के अन्दर का हिस्सा था, न बाहर का। उसे उन्होंने अपनी गोद में बैठा लिया, सो वह न आकाश में था, ना धरती पर।
सांझ का समय था, स्टेज पर हल्की रोशनी थी, कि न ही दिन था, न ही रात्रि का समय—और नरसिंह बने पात्र ने हिरण्यकश्यप को अपने पंजों के नाखूनों से, जो न अस्त्र थे और ना ही शस्त्र, चीड़-फाड़ कर दिया। उसका वध कर, दहाड़ते हुए नरसिंह सिंहासन पर बैठ गये। मुंह में खून और आंख में ज्वाला। संगीत अपने चरम पर था और अचानक प्रह्लाद दिखाई दिये। नरसिंह के चेहरे पर मार्मिक भाव प्रकट हुए, और निर्भीक प्रह्लाद उनकी गोद में बैठ गये। संगीत नर्म हो गया, और पर्दा धीरे-धीरे गिरने लगा।
तालियों की आवाज़ अभी बंद भी नहीं हुई थी कि हम दोनों सहेलियां थियेटर से बाहर निकलने की जल्दी में, एग्जिट की ओर बढ़ गयीं। घर पहुंचना था और कल आफिस भी था।
इस पूरी नाटिका के मर्म को समेटे हुए और उस आखिरी दृश्य के अंशों को संजोये मैं ऑटो खोजने लगी। वह नरसिंह अवतार, वह पंजों से हिरण्यकश्यप का उदर चीरना और प्रह्लाद को देखते ही अपने भाव बदल लेना —करुणामय संवेदना और दया दर्शाते हुआ भाव, मेरे साथ ही चला आया। मैं घर पहुंच गयी।
सुबह का सूरज, जाने कहां से उदयमान हो रहा था। पाताल से निकलता सूरज ऐसा प्रतीत होता जैसे वराह अवतार के दांतों से छीन कर किसी ने एक नारंगी गेंद की नाईं आसमान की ओर उछाल दिया हो।
सूरज धीमी गति से धीरे-धीरे आसमान के माथे पर टंकने के लिए बढ़ता जाता और अपना रंग लाल कर लेता, बिंदी की तरह और फिर सभी रंगों का समावेश करता दिन सफेद हो जाता— और आसमान नीला।
मैंने भी पहनने के लिए नीली साड़ी निकाली और सोचा आज सफेद बिंदी लगाऊंगी माथे पर।
***
जहां पुरानी दिल्ली खत्म होती है और नई दिल्ली शुरू होती है, दोनों के बीच की गलियों में रहती हूं मैं। तंग गलियां जो गलियों से होती हुई एक बड़ी गली में समाहित होती और फिर और बड़ी गलियों से गुज़रती हुई, बड़ी सड़क पर पहुंचती। गलियों में राशन की एक कक्षीय दुकानें, पंक्चर वाले अपने टायर लटकाये, दूध-दही-पनीर बेचने वाले हलवाई- सभी छोटे दुकानदारों ने अपने बाज़ार सजाये होते।
इन्हीं तंग गलियों से रोज़ गुज़रती थी, सो आज भी ऑफिस के लिए निकली। जल्दी-जल्दी डग भरती जा रही थी, एक गली से दूसरी गली ताकि बड़ी सड़क तक पहुंच पाऊं और वहां से बस स्टाप तक।
मैं चली जा रही थी। पीठ पर एक सरसराहट-सी महसूस हुई। लगा, कोई पीछे से मुझे देख रहा है। ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई हमें ध्यान से ताड़े तो छठी इन्द्री इस बात का संज्ञान देती है कि कोई हमें देख रहा है। और, हम मुड़ कर देखते हैं। इस वक्त भी मुझे कुछ ऐसा ही अहसास हुआ।
मैंने मुड़ कर देखा। एक घटिया-सा गुंडा किस्म का लड़का मुझे ही देख रहा था। इस देखने की कोई धर्म या जात नहीं होती। वो तो बस ताड़ता है। आप को अंदर से बाहर तक। एक एमआरआई भी इतनी बारीकी से नहीं देखता, जैसे वो देख रहा था।
मेरे पोर-पोर से ज़हर बह निकला। सांप के गरल में भी इतना ज़हर न था, जितना मेरे अंग-अंग से फूट रहा था। वह मुझे घूर रहा था, एकटक। मैं गुस्से में थी, वह घूरे जा रहा था। मन था कि उसकी आंखें नोच लूं। उसे तार-तार कर दूं। अभी सही वक्त नहीं था। अभी तो सुबह थी और वह धरती पर था।
मैं मुड़ी और आगे बढ़ गयी, तेज़ कदमों से। शरीर में कीड़ियां रेंगने लगीं। एक अंजाना-सा भय भी हुआ। रुक कर मुड़ने का मन हुआ, लेकिन मैंने मन को काबू में किया। मैं आगे बढ़ गयी। परिस्थिति कुछ अनुकूल-सी नहीं लगी। लोग थे, पर बहुत निरीह और तन्हा-सा महसूस हुआ। मैंने चाल कुछ और तेज़ कर ली। अब कुछ देखता-सा महसूस नहीं हुआ।
मैं बस स्टाप तक पहुंच चुकी थी। मुंह में एक लार थी, जो भर भर गयी थी। थूकना चाहती थी, पर उसे निगलना मजबूरी थी। सांस जो इतनी देर से रुकी हुई थी, उसे भी तो बाहर का रास्ता सुझाना था। सो उस गलीज़ थूक को अन्दर किया और सांस को बाहर छोड़ा। साड़ी के पल्लू से पसीने को पोंछा और अपने आप को स्थिर किया। पीठ पसीने से भीग चुकी थी और टांगों में एक कंपन था। कुछ कमजोरी-सी महसूस होने लगी।
धीरे-धीरे डर का ज्वर शांत होने लगा, कि वही लड़का बस स्टाप पर आ खड़ा हुआ। वह मुझे ही देख रहा था, और मैं दफन हुई जा रही थी। भीड़ में अड़ता-निकलता वह मेरे साथ सटकर खड़ा हो गया। मुझे जैसे कुछ देर को फालिज-सा (पैरालिसिस) हो गया।
लकवे के हालात से मैं जल्द निकली। पसीने से नहा गयी थी मैं। ब्लाउज पूरा भीग गया था। क्रोध में आंखों से ज्वाला निकली और लावा बनकर ठहर गयी। बेचारगी के आलम में, मैंने भीड़ की ओर देखा। भीड़ की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। सभी अपने अस्तित्व में मसरूफ थे। व्यस्त थे मोबाइल पर। मैं टूटने-सी लगी। मैं बिखरने-सी लगी। थोड़ी-सी सरक गयी। बस स्टाप से सड़क पर आ गयी। वो भी सरक आया। भीड़ में एक हरकत हुई। बस के आते ही, मैं उसमें चढ़ गयी। सोचा, शायद इस अजाब से पीछा छूट जायेगा। ऑफिस और काम का ख्याल ही ज़हन से मिट गया। फिक्र थी, तो बस अपनी।
चलती बस के पीछे दौड़ कर वह पायदान पर एक पैर जमा, बस में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद ही मुझे वह महसूस हुआ। उसका घटिया परफ्यूम, उसकी हैसियत और मौजूदगी का अहसास करवा रहा था। वह मुझ पर गिरने ही लगा।
इतना मैला-मैला-सा महसूस हुआ, कि गंगा की सैकड़ों लहरें उस मैल को न धो पातीं। मैं सिकुड़ गयी। पत्तझड़ के पत्ते-सी कांपने लगी। एक कमज़ोर बेल की तरह, बस में लगे डंडे को पकड़, उसे सहारा बना खड़ी रही किसी तरह। हथेलियों और तलवों से पसीना बहने लगा। डंडे पर से हाथ छूटते रहे और पैरों से सैंडिल फिसलने लगीं। कुछ ही देर में बस स्टाप आ गया। मैं बस के रुकने से पहले ही कूद गयी। पांव जमीन पर लगे और मैं कुछ संभली! फिर ऑफिस की तरफ बढ़ गयी। पसीने में उस कमीने की हबक अब भी थी। पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती थी। आफिस पहुंच जाना चाहती थी।
ऑफिस की इमारत सामने थी। जैसे ही उसके आने का अहसास हुआ, मेरी चाल में और तेजी आ गई। शरीर कुछ ठंडा हुआ। एक सांस आराम से ली और धड़कन ने कुछ संभला-सा महसूस किया।
चार सीढ़ियां, एक चबूतरा-सा और वह शीशे की इमारत मुझे समेट लेगी। उसे प्रशिक्षण है, मुझे पूर्णता देने का। मेरे सर्वत्र को प्राणवान करने के लिए। शीशे का दरवाज़ा सामने था। उस पर परिवर्तक फिल्म चढ़ी हुई थी। मैं जैसे ही दरवाज़े के पास पहुंची, शीशे में उसी शख्स का प्रतिबिंब दिखा। वह मेरा पीछा करता हुआ यहां तक आ पहुंचा था। मैं तेज़ी से इमारत के प्रकोष्ठ में दाखिल हुई। वह भी उसी दरवाज़े से घुस आया। मेरा ऑफिस, मेरा सुरक्षा सुरक्षित ज़ोन था। रिसेप्शन के आईने में उसकी कुटिल मुस्कुराहट दिखाई दी। बिल्कुल हिरण्यकश्यप की तरह।
मेरा डर क्रोध में परिवर्तित हो गया। एक मवाद-सा बह निकला, पुराने गुबार की तरह। एक फोड़ा सदियों से सालता रहा था। ज़हर मेरे पोर-जोर से फूटने लगा। नफरत का लावा बह निकला। मेरी पीठ उसकी तरफ थी। बंधे बाल खुल गये। मेरी बाहें फड़कने लगीं; मेरे हाथ खुलने लगे; मैं फैलने लगी; मेरा विस्तार विकरालता की ओर बढ़ गया।
मैं मुड़ी। मेरा रूप परिवर्तित हो चुका था। मैंने नरसिंह का अवतार ले लिया था। बड़ी-बड़ी आंखें क्रोध से लाल थीं। नथुनों में फड़कन थी। मेरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। मैं न तो अंदर थी, न ही ऊपर आसमान था। मैं देहरी से ज़रा-सा अंदर प्रकोष्ठ में थी। न अलसुबह थी, न दोपहर; एक मिला-जुला वक्त था।
वह मनुष्य के रूप में शैतान था, तो मैं भी नरसिंह-सी हो गई थी। मेरी भीरुता ओझल हो चुकी थी- मैं कुछ-कुछ नारी जैसी और कुछ-कुछ नर जैसी हो गई थी।
वातावरण में मृदंग, नगाड़े, घुंघरू, ढाल, ढफ, मंजीरे- सभी गूंजने लगे। वही वातावरण जो कल थियेटर के स्टेज पर था। मैं ताकतवर और खूंखार हो गई। थोड़ी-सा एक टांग को झुका कर, दूसरी टांग को उस पर रख, एक गोद-सी बना ली।
उस आदमजात को गोद में रखकर मैंने नाखूनों से उसकी अंतड़ियों निकाल दीं, उसकी छाती को मुक्कों से छिन्न-भिन्न किया। वह मर गया था। मेरा सर्वस्व पवित्र हो गया। सारी कायनात जड़वत् थी।
मैं यह कल्पना कर रही थी कि लिफ्ट के पहुंचने की घंटी सुनाई दी। मैंने चारों ओर देखा, प्रकोष्ठ को महसूस किया और अपनी उखड़ी सांस को संभाला। लिफ्ट के आसपास भीड़ थी। मैं भीड़ में खो गई। एक औरत बनकर शर्मीली, भीरु, निरीह, रेशम-सी सरल, विनम्र, ममतामयी हो गई। लिफ्ट के दरवाजे खुले और मैं सभी के साथ उसमें चढ़ गई। मैंने सहयात्रियों को एक नर्म-सी मुस्कान दी। लिफ्ट ऊपर की ओर चल पड़ी।
सूरज बाहर शिखर पर पहुंच रहा था। मेरी माथे की बिंदिया चमकने लगी और सफेद रोशनी में तब्दील हो गई।
एक आकाशवाणी हुई, ‘ए स्त्री - एक अवतार ले, वक्त हो गया है।’