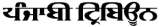मौजूदा दौर के सिनेमा में सद्भाव का सन्नाटा
हेमंत पाल हमारे देश में समय के बदलाव को फिल्मों के कथानक के जरिये व्यक्त करने की परंपरा बहुत पुरानी है। जब जैसा माहौल रहता है, तब वैसी फ़िल्में बनती हैं। युद्धकाल में हमारे फिल्मकारों ने जंग पर आधारित फ़िल्में...
हेमंत पाल
हमारे देश में समय के बदलाव को फिल्मों के कथानक के जरिये व्यक्त करने की परंपरा बहुत पुरानी है। जब जैसा माहौल रहता है, तब वैसी फ़िल्में बनती हैं। युद्धकाल में हमारे फिल्मकारों ने जंग पर आधारित फ़िल्में बनाई, युवाओं का आक्रोश उभरा तो ऐसे विषय को चुना गया, कई फिल्मों में तो प्राकृतिक आपदा को भी फिल्म का विषय बनाया गया। यहां तक कि अंतरिक्ष में देश को सफलता मिली तो उसे भी विषय बनाया गया। लेकिन, अब हिंदू-मुस्लिम एकता वाले कथानकों पर फ़िल्में बननी बंद हो गई! जबकि, ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने से कुछ साल पहले तक अलग-अलग कथानकों के जरिये सामाजिक सद्भाव बढ़ाने की कोशिश की गई थी। अब शायद इसलिए ऐसी फ़िल्में नहीं बनती कि वे माहौल में मेल नहीं खाती। फिल्मकार भी इसलिए कोशिश नहीं करते कि उसकी रचनात्मकता पर आंच न आए और न वे किसी आक्रोश का निशाना बनें। आज यदि विवेक अग्निहोत्री की ‘द कश्मीर फाइल्स’ को धुआंधार सफलता मिलती, तो उसी तरह की फिल्मों की बाढ़ आ जाती। फिर ‘द केरल स्टोरी’ बनाई जाती है और उसके रियल स्टोरी होने के तर्क दिए जाते हैं। आशय है कि समाज के एक वर्ग को नायक और दूसरे को खलनायक की तरह पेश किया जाने लगा।
जबकि, हिंदी सिनेमा का इतिहास सद्भाव वाली फिल्मों से भरा पड़ा है। साल 1941 में वी शांताराम ने ‘पड़ोसी’ नाम से दो दोस्तों की कहानी पर फिल्म बनाई थी। फिल्म की खासियत यह थी, कि इसमें पंडित का किरदार मजहर खान ने और मुस्लिम का गजानन जागीरदार ने निभाया था। फिल्म के अंत में एक ही मकसद के लिए दोनों साथ में जान दे देते हैं। इसके कुछ साल बाद पीएल संतोषी ने ‘हम एक हैं’ (1946) बनाई, जिसमें सामाजिक सौहार्द दिखाया गया था। उस समय समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य जैसा कोई भाव नहीं था, तो ऐसी फिल्मों को मनोरंजन की ही तरह देखा जाता था। तब इन फिल्मों के डायलॉग भी ‘क्रांतिवीर’ की तरह जोशीले नहीं थे कि रोंगटे खड़े कर दें! यश चोपड़ा की फिल्म ‘धूल का फूल’ (1959) भी ऐसी ही फिल्म थी। एक मुस्लिम एक हिंदू बच्चे को जंगल में लावारिस देखता है, उसे पालता है। इस फिल्म का गीत ‘तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा’ काफी चर्चित रहा। आज के दौर में सांप्रदायिक सौहार्द और मानवता से जुड़ी फिल्मों में ‘बजरंगी भाईजान’ और ‘मुल्क’ ही बनी।
धर्म को तवज्जो ज्यादा दी जाने लगी
हिंदी सिनेमा में धर्म कभी विवाद का मसला नहीं रहा। इस विषय को कभी हवा भी नहीं दी गई, क्योंकि फिल्मों को मनोरंजन के नजरिये से देखा जाता रहा। लेकिन, अब फिल्मों में धर्म को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दी जाने लगी। दर्शक भी विचारधारा में बंट गया। इसे पब्लिसिटी स्टंट भी बनाया जाने लगा, ताकि फिल्म को हिट करवाया जा सके। इसलिए कि फिल्मों का मूल स्वर भी अब सद्भाव से हटने लगा। फिर भी दर्शकों को सिनेमाघर तक लाने के लिए शाहरुख खान आज भी परदे पर राज और आर्यन ही हैं। आमिर खान को भी भुवन, रवि और लाल सिंह चड्ढा की तरह पसंद किया जाता है। सलमान खान को भी सबसे ज्यादा चुलबुल पांडे के किरदार में पसंद किया गया। अमिताभ बच्चन तो विजय के साथ इकबाल भी हैं और एंथोनी भी। फिल्मों में हर रूप में सद्भाव जिंदा रहा, पर अब उसका लोप होता जा रहा है।
आजादी के बाद सद्भाव अहम कथानक
देश की आजादी के बाद सभी का पहला मकसद बिखरे समाज से नए देश का निर्माण था। लोगों के पास सामाजिक और आर्थिक बराबरी, समृद्धि और खुशहाली के सपने थे। इसलिए ‘मदर इंडिया’, ‘दो बीघा जमीन’ और ‘नया दौर’ जैसी फिल्में सफल हुई और आज भी ये मील का पत्थर हैं। देश के विभाजन के बाद उस त्रासद सच्चाई को कभी फिल्म का विषय नहीं बनाया गया। ऐसी फ़िल्में बनी भी तो बरसों बाद। कोशिश यही थी कि विभाजन के दर्द को भूलकर सांप्रदायिक एकता को बढ़ाया जाए। कुंभ के मेले या ट्रेन में बिछुड़े दो भाइयों की कहानी जैसे कथानक रचे गए। ये दोनों भाई बिछड़कर अलग-अलग धर्मों वाले दो परिवारों में पलते हैं। इसी दौर में गांधीवादी विचारधारा को भी बढ़ाकर छुआछूत और जातिवाद को ख़त्म करने की पहल की गई। कई फिल्मों में जमींदारी प्रथा और साहूकारी का विरोध किया गया। नए रूप में आज भी ये सारी बुराइयां समाज में हैं, पर फिल्म का विषय नहीं बनाई जातीं।
‘शोले’ के इमाम साहब को याद करो
देवानंद की फिल्म ‘अल्लाह तेरो नाम’ (1961) में सद्भाव की अजब मिसाल पेश की गई थी। ‘शोले’ (1975) में छोटे से रोल में इमाम साहब सभी की तुलना में अधिक साहसी और प्रेरक व्यक्ति के रूप में दिखाए गए। कच्चे धागे (1999) में हिंदू और मुस्लिम सौतेले भाई अपनी मां मरियम को बचाने के लिए एकजुट होते हैं। सिर्फ यही नहीं, सात हिंदुस्तानी (1969), क्रांति (1981), देश प्रेमी (1982), कर्मा (1986) व लगान (2001) जैसी फिल्मों का जिक्र किया जा सकता है।
मदद के बहाने सद्भाव दिखाया गया
ऐसी भी फिल्में आई जिनमें मुस्लिम को हिंदू किरदार के हित में भले आदमी की भूमिका में दिखाया गया। अमिताभ की फिल्म ‘जंजीर’ (1973) में विलेन शेर खान (प्राण) हिंदू पुलिस अधिकारी की मदद करता है। इकबाल (2005) भी ऐसी ही फिल्म थी, जिसमें मूक-बधिर नायक इकबाल क्रिकेट में कामयाब होना चाहता है, जिसका कोच हिंदू होता है। 2006 में आई फिल्म ‘डोर’ में हिंदू और मुस्लिम दो महिलाओं के बीच संवेदनशील रिश्ता दिखाया गया। ‘खुद्दार’ (1982) में एक मुसलमान दो भाईयों को आश्रय देता है। ‘खुदा गवाह’ (1992) में अमिताभ बच्चन काबुल के एक पठान की भूमिका निभाते हुए एक हिंदू पुलिस अधिकारी से मदद लेते हैं।
ऐसी फिल्मों का जिक्र बहुत लंबा है। ‘हे राम’ (2000) में अमजद खान नाम का किरदार अंततः हिंदू नायक को गांधी की हत्या करने से रोकता है। ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ (2003) में जहीर की मौत कहानी में मोड़ लाती है। यशराज की फिल्म ‘चक दे इंडिया’ (2007) में मुस्लिम हॉकी कोच महिला हॉकी टीम को जिताता है। ऐसी फिल्मों की संख्या सैकड़ों में है जिनमें हिंदू और मुसलमान दोस्त या मददगार के रूप में दिखाई देते हैं। अमिताभ की फिल्म ‘अंधा कानून’ में विजय और खान दोनों ही समाज में अपराधियों से पीड़ित हैं। ‘ए वेडनसडे’ (2008) में कई आतंकवादी मुस्लिम हैं। लेकिन, ईमानदार पुलिस वालों में से एक किरदार भी मुस्लिम है। तात्पर्य यह कि ऐसी फिल्मों को पसंद करने वालों के लिए उस तरह का माहौल भी जरूरी है, जो अभी दिखाई नहीं देता। सभी चित्र : लेखक