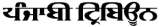देश में लंबे समय से यह मुद्दा सार्वजनिक विमर्श में रहा है कि विषम परिस्थितियों में एक त्रासदी से मुक्ति हेतु इच्छामृत्यु की अनुमति दी जाए या नहीं। समय-समय पर अदालती फैसलों ने मार्गदर्शक भूमिका निभाई है। साथ ही कोशिश की गई है कि इस छूट का दुरुपयोग न किया जा सके। हाल ही में एक ज्वलंत प्रसंग पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी थी कि हमें अब कुछ करना होगा, इस तरह के त्रासद जीवन की कोई तार्किकता नहीं है। दरअसल, यह मामला एक 32 वर्षीय युवक का है, जो पिछले 13 सालों से कोमा जैसी स्थिति में है। यह अब केवल महज चिकित्सीय त्रासदी का मामला नहीं रह गया है। अब यह एक महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक प्रश्न भी बन चुका है। निश्चित रूप से शीर्ष अदालत की टिप्पणी देश में जीवन के अंतिम क्षणों में गरिमापूर्ण व्यवहार के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। निश्चय ही यह प्रसंग अतीत में बहुचर्चित अरुणा शानबाग के मामले की यादें फिर से ताजा कर देता है। इस प्रसंग ने ही देश को पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु के प्रश्न का सामना करने के लिये बाध्य किया था। वर्ष 2011 में, सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग के मामले में फैसला सुनाते हुए, सैद्धांतिक रूप से निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी। दरअसल, अरुणा शानबाग एक भयानक हमले के बाद से ही 42 वर्षों से कोमा जैसी स्थिति में रही थीं। भले ही अदालत ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, लेकिन साथ ही उसके साथ कुछ प्रतिबंधात्मक सुरक्षा उपायों के अनुपालन के भी निर्देश दिए थे। निश्चित रूप से इस मामले में अदालती फैसला नैतिक प्रेरणा का स्रोत भी बना। कालांतर में जिसके चलते वर्ष 2018 में एक संविधान पीठ ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की। साथ ही इसके लिये एक आवश्यक प्रक्रिया भी निर्धारित की थी। जिसका मकसद था कि समाज में कहीं इस छूट का दुरुपयोग आपराधिक स्वार्थों के लिये न किया जा सके।
वर्ष 2023 में, अदालत ने इन दिशानिर्देशों को और सरल बनाने का प्रयास किया। जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि प्राथमिक और माध्यमिक चिकित्सा बोर्डों द्वारा स्थिति के मूल्यांकन की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल देश में वही प्रक्रिया आज भी चल रही है। बहरहाल, वर्तमान मामले में बार-बार की गई अपीलें, इससे जुड़ी खामियों को भी उजागर करती हैं। दरअसल, ऐसे मामलों में पीड़ित को घर में दी जाने वाली देखभाल अपर्याप्त ही साबित होती है। वहीं दूसरी ओर राज्य का समर्थन भी पर्याप्त नहीं रहा है। इसके अलावा ऐसे मामलों से जुड़ी अनसुलझी नैतिक दुविधाएं असमंजस की स्थिति पैदा करती रही हैं। निस्संदेह, इस मामले में किसी युवा वयस्क के लिये निष्क्रिय इच्छामृत्यु की पहली स्पष्ट स्वीकृति हो सकती है। आज देश में हजारों मरीज कोमा जैसी अवस्था में नारकीय जीवन जी रहे हैं। जो उनके परिवारों के लिये भी एक त्रासदी की स्थिति है। जहां परिवार एक ओर भावनात्मक संकट से जूझ रहे होते हैं, वहीं रोगी के उपचार से जनित आर्थिक बोझ भी निरंतर बढ़ता जाता है। दूसरी ओर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार पर भी सवाल उठते रहे हैं। निस्संदेह, अदालत को जटिल परिस्थितियों में जैविक अस्तित्व के कठोर विस्तार के बजाय रोगी की मुक्ति और परिवार की पीड़ा को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे में यदि एम्स 17 दिसंबर तक मामले में जीवन की निरर्थकता की पुष्टि करता है, तो निष्क्रिय इच्छामृत्यु की स्वीकृति एक मिसाल कायम कर सकती है। इसके बाद दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों को भी स्पष्ट किया जा सकेगा। साथ ही जीवन के अंतिम विकल्पों का सम्मान किया जा सकेगा। देश के नीति-नियंताओं को कोमा जैसी अवस्था में सालों जूझते लोगों के मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाने चाहिए, जिससे ऐसे रोगियों की उपचारात्मक देखभाल और परामर्श को एकीकृत किया जा सके। मानवीय करुणा की मांग है कि जीवन की पवित्रता और पीड़ा की क्रूरता के बीच संतुलन बनाया जाए। इच्छामृत्यु जब सहमति से होगी तो मानवता को कायम रखा जा सकता है। न्यायपालिका को ऐसा न्याय देना चाहिए, जो रोगी को पीड़ा से मुक्त करे और एक करुणामय भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे।