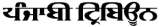जनतंत्र को मजबूत भी बनायें ये चुनाव
विश्वनाथ सचदेव यूं तो पिछले एक अर्से से हमारा देश ‘चुनावी मोड’ में ही चल रहा है, पर अब तो आम चुनाव से पहले के सेमीफाइनल की बाकायदा घोषणा भी हो गयी है। शंखनाद हो चुका है। दिसंबर तक पांच...

यूं तो पिछले एक अर्से से हमारा देश ‘चुनावी मोड’ में ही चल रहा है, पर अब तो आम चुनाव से पहले के सेमीफाइनल की बाकायदा घोषणा भी हो गयी है। शंखनाद हो चुका है। दिसंबर तक पांच राज्यों में नयी सरकारें भी बन ही जाएंगी। सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, सवाल यह है कि इन चुनाव के बाद हमारा जनतंत्र कुछ मज़बूत होगा या कमजोर?
हम जनतंत्र का अमृत महोत्सव मना चुके हैं। अब हमारा अमृत-काल चल रहा है। क्या मतलब होता है इस अमृत-काल का, यह तो वही जाने जिन्होंने यह जुमला उछाला है, पर यह तय है कि जुमलेबाजी हमारी राजनीति का एक महत्वपूर्ण हथियार बन गयी है। पिछले आठ-दस सालों में हमने इस हथियार की धार भी देख ली है। होना तो यह चाहिए था कि अपना ‘अमृत-महोत्सव’ मनाने वाला हमारा लोकतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं को मज़बूती देते हुए दिखता, पर चुनावी बिसात पर सजे मोहरे बता रहे हैं कि सारा ज़ोर येन-केन-प्रकारेण मुकाबला जीतने का है। हम देख रहे हैं, और यह स्पष्ट कहा भी जा रहा है कि मैदान में उन्हीं उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है, जिनके जीतने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है। यहां तक तो बात फिर भी ठीक लगती है, पर उम्मीद पूरी करने के अराजक तौर-तरीकों का स्वीकार लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरे की घंटी ही माना जाना चाहिए। यह घंटी बज रही है, ज़ोरों से बज रही है, पर क्या हम इसे सुन रहे हैं? सच बात तो यह है कि हम शायद इसे सुनना भी नहीं चाहते।
जनता के शासन का नाम है जनतंत्र। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। चुनावों का होना या फिर वोट देना मात्र ही इस बात का प्रमाण नहीं है कि हमारा जनतंत्र फल-फूल रहा है। वोट मांगने वाले और वोट देने वाले, दोनों, का दायित्व बनता है कि वह जनतंत्र की इस पूरी प्रक्रिया में ईमानदारी से हिस्सा लें। आज हमें स्वयं से यह पूछने की आवश्यकता है कि क्या हमारी राजनीति में ईमानदारी नाम की कोई चीज बची है? झूठे वादे करना, धर्म और जाति के नाम पर मतदाताओं को बरगलाना, आधारहीन आरोपों के शोर में विवेक की आवाज़ को दबा देना, यह सब तो जनतंत्र नहीं है।
दुर्भाग्य यह भी है कि जनतांत्रिक मूल्यों के नकार के इस खेल में कोई पीछे रहना नहीं चाहता। सब अपने-अपने महिमा-मंडन में लगे हैं। आत्म-प्रशंसा से लेकर पर- निंदा तक फैला हुआ है हमारा बदरंग इंद्रधनुष। होना तो यह चाहिए कि राजनीतिक दल अपनी-अपनी रीति-नीति का ब्योरा लेकर जनता के पास जाएं, पर हमारी समूची राजनीति ‘पहले की सरकारों’ को कोसने से लेकर अपना ढोल बजाने तक सीमित होकर रह गयी है। जो अपने आप को जितना बड़ा नेता समझता-कहता है, वह उतने ही ज़ोर से विरोधी पर लांछन लगाने में लगा है। अपेक्षित तो यह है कि सत्ता-पक्ष चुनाव के मौके पर अपनी उपलब्धियों का लेखा-जोखा मतदाता के समक्ष प्रस्तुत करे और विपक्ष सत्ता-पक्ष की कमज़ोरियों और अपनी रीति-नीति के बारे में बताए। बताए कि वह कैसे और क्या बेहतर करेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। चुनाव के संदर्भ में जो हो रहा है वह एक तो यह है कि विरोधी को नीचा दिखाने की कोशिश और दूसरे रेवड़ियां बांटने की प्रतिस्पर्धा। बड़ी बेशर्मी से मतदाता को लुभाने की होड़-सी लगी है।
एक और प्रवृत्ति जो पिछले एक अर्से से हमारी राजनीति में पनपी है वह मतदाता को अपमानित करने वाली है। हमारे राजनेताओं ने मान लिया है कि देश का मतदाता कुछ रुपयों से खरीदा जा सकता है। दो तरीकों से मतदाता को रुपये बांटे जा रहे हैं–एक तो यह कि चुनाव के मौके पर नोट के बदले वोट दिया जाये और दूसरे वैध तरीके से कभी बेटियों के नाम पर, कभी माताओं-बहनों को नगद राशि दी जाये। स्कूलों में बच्चों की फीस माफ हो, गैस-बिजली आदि की दरें कम की जाएं, सस्ती दरों पर जरूरतमंदों को अनाज बांटा जाये, यह तो फिर भी समझ में आता है, पर यह समझना मुश्किल है कि लाभार्थियों के खातों में पैसे जमा करना रिश्वत नहीं तो और क्या है? रिश्वत लेना या देना अपराध है पर यह अपराध हमारे राजनीतिक दल खुलेआम कर रहे हैं। न उन्हें कोई सज़ा मिलती है और न उन्हें कोई डर है इसका।
था एक ज़माना जब मतदान की यज्ञ से तुलना की जाती थी और वोट को तुलसी-दल की पवित्रता प्राप्त थी। अब तो यह चुनाव ऐसी लड़ाई बन गया है जिसमें सब कुछ जायज मान लिया गया है। यहां तक कि विरोधी को अपशब्द कहते हुए भी किसी को कोई शर्म नहीं आती। बहुत पुरानी बात नहीं है जब संसद तक में ऐसे शब्द काम में लिये गये थे, जो किसी भी सभ्य समाज में उचित नहीं माने जा सकते। इसमें संदेह नहीं कि चुनाव जीतने के लिए ही लड़े जाते हैं, पर किसी भी कीमत पर जीत हमारे जनतंत्र को खोखला ही बनायेगी। संप्रदायवादी ध्रुवीकरण और अवसरवादी राजनीति के सहारे खड़ा किया गया सत्ता का महल भीतर से खोखला ही होता है, यह बात हमारे राजनीतिक दलों को समझनी ही चाहिए। हमारे राजनेताओं को भी यह सीखना होगा कि इस तरह की अनैतिक राजनीति उन्हें तात्कालिक सफलता भले ही दे दे, पर इस राजनीति का ज़हर हमारे जनतंत्र को असाध्य बीमारी का शिकार बना देगा। इस बीमारी से देश को बचाना हमारे अस्तित्व की शर्त है, जनतंत्र के बने रहने की शर्त है।
अभी पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, फिर लोकसभा के लिए चुनाव होंगे। चुनाव के इस माहौल में यह बात समझना ज़रूरी है कि चुनाव जीत कर सरकार बनाने में सफलता ही जनतंत्र की सार्थकता नहीं है। यह सार्थकता तभी उजागर होगी जब मतदाता के पास चुनने का अधिकार ही नहीं, अवसर भी होगा। सांपनाथ और नागनाथ में से चुनने की विवशता कुल मिलाकर जनतंत्र का नकार ही है। इसका सीधा-सा मतलब यह है कि एक तरह की राजनीतिक बेईमानी का शिकार हो रही है हमारे देश की जनता। इस स्थिति से उबरने का रास्ता भी हमारे बड़बोले राजनेता अथवा घटिया राजनीति नहीं खोजेगी। मतदाता को स्वयं खोजना होगा यह रास्ता। अपने विवेकपूर्ण निर्णय से ही देश का मतदाता उस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है जो किसी भी सुव्यवस्था के लिए अपेक्षित है।
आने वाले कुछ दिन राजनीति का घटिया खेल खेलने वाले राजनेताओं द्वारा मतदाता को बरगलाने की कोशिश का अवसर हैं। लच्छेदार भाषा में अपना ढोल पीटने वाले राजनीति के ठेकेदारों को यह समझाने का अवसर भी यही है कि कुछ समय के लिये कुछ लोगों को भले ही मूर्ख बनाया जा सके, पर हमेशा सबको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह बात मतदाता और राजनेताओं, दोनों, को समझनी है। यह समझ जितनी जल्दी आ जाये, जनतंत्र के स्वास्थ्य के लिए उतना ही बेहतर है।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।