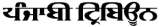सरकारी धन से चुनावी रेवड़ियां बांटने के खतरे
चुनावी समय में सरकारों द्वारा नकद या मुफ्त सुविधाएं देकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति ‘रेवड़ी संस्कृति’ बन गई है, जो लोकतंत्र, वित्तीय अनुशासन और राजनीतिक नैतिकता को कमजोर करती है। बिहार में चुनावों की तारीखें घोषित होने के साथ...
चुनावी समय में सरकारों द्वारा नकद या मुफ्त सुविधाएं देकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति ‘रेवड़ी संस्कृति’ बन गई है, जो लोकतंत्र, वित्तीय अनुशासन और राजनीतिक नैतिकता को कमजोर करती है।
बिहार में चुनावों की तारीखें घोषित होने के साथ ही ‘राजनीतिक रिश्वतखोरी’ की बातें चलने लगी हैं। राजनीतिक रिश्वतखोरी यानी मतदाता को रेवड़िया बांटकर उन्हें अपने पक्ष में वोट देने के लिए लुभाना। कहा यह भी जा रहा है कि चलो अब कुछ दिन रेवड़ियां बांटने की घोषणाओं से तो पीछा छूटेगा। यहां रेवड़ियों का मतलब वह ‘मुफ्त की सेवाएं’ हैं जिनका लालच देकर राजनेता मतदाता को बरगलाते हैं। पहले बिजली-पानी जैसी जीवनोपयोगी चीज़ें मतदाता को दी जाती थीं, देने का वादा किया जाता था, और अब तो यह नकद पैसा बांटा जा रहा है। बिहार सरकार ने कुछ ही दिन पहले एक करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में दस हज़ार रुपये जमा करवा कर इस रेवड़ी संस्कृति को एक नया आयाम दे दिया है। एक करोड़ महिलाओं का मतलब एक करोड़ परिवारों तक पहुंचना है। महिलाओं के सशक्तीकरण के नाम पर यह सीधी रिश्वत है।
सवाल यह पूछा जा रहा है कि किसी सरकार द्वारा इस तरह की नकद राशि बांटना क्या सरकार के पैसों से चुनाव जीतना नहीं है? यदि ऐसा है तो फिर इसे अपराध की श्रेणी में क्यों न रखा जाये, और यदि यह अपराध है तो फिर इसकी कोई सज़ा तय क्यों नहीं होनी चाहिए? पूछा तो यह भी गया है कि सरकार द्वारा मुफ्त राशन बांटना भी क्या एक तरह से रेवड़ी बांटना नहीं है?
आश्वासन वाली राजनीति कोई नयी चीज नहीं है। और ऊपरी तौर पर देखें तो यह उतनी ग़लत भी नहीं लगती। आखिर जनता के हित की बात सोचना सरकार का काम है, और जनता को वित्तीय सहायता देकर जनता की सहायता ही तो की जाती है। पर सवाल उठता है कि जनता की यह ‘मदद’ सरकारों और राजनीतिक दलों को चुनावों से पहले ही याद क्यों आती है? सवाल यह भी उठाना चाहिए कि राजनीति में ‘तोहफे’ बांटने की यह परंपरा अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं आनी चाहिए?
चुनाव से कुछ अरसा पहले, या वैसे भी, हमारी सरकारें जनता की मदद की घोषणाएं शुरू कर देती हैं और मीडिया में इसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के तोहफे के रूप में प्रचारित किया जाता है। कुछ ही साल पहले चुनाव-प्रचार के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री ने बिहार में खुले आम तोहफों की बोली लगायी थी। एक चुनाव-सभा में उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, ‘कितने दूं, दस करोड़?, सौ करोड़?, हजार करोड़? या लाख करोड़?’ उनकी घोषणा पर श्रोताओं ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया था, निश्चित रूप से इस तोहफे का कुछ असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ा होगा। पर चुनावी लाभ के लिए जनता के पैसों के तोहफे इस तरह बांटने की घोषणा क्या विद्रूप पहल नहीं मानी जानी चाहिए? सच तो यह है कि इसे तोहफा या उपहार कहना ही ग़लत है। यह अनुचित आर्थिक लेन-देन ही है– और रिश्वत देना या लेना दोनों अपराध हैं! इस अपराध की सज़ा क्यों तय नहीं होती? इस सवाल का सीधा-सा जवाब यह है कि यह अपराध सबकी मिली-भगत से हो रहा है। राजनेताओं को, सरकारों को, राजनीतिक दलों को रेवड़ियां बांटने, या कहना चाहिए रिश्वत देकर अपना काम निकालने का यह एक आसान तरीका लगता है। ऐसे में पारस्परिक लाभ के इस सौदे में भला किसी को कुछ ग़लत क्यों लगेगा?
पर यह ग़लत परंपरा है जन-कल्याण की योजनाएं बनाना, उन्हें ईमानदारी के साथ क्रियान्वित करना सरकारों का काम है। पर यह काम चुनावों से ठीक पहले ही क्यों? एक करोड़ महिलाओं को बिहार की नीतीश सरकार द्वारा दस हज़ार रुपये देने और विपक्ष द्वारा पच्चीस सौ रुपये प्रति माह देने का वादा करने में कोई विशेष अंतर नहीं है। कहा जा सकता है कि इस तरह की घोषणाएं वर्तमान या भावी सरकार की रीति-नीति बताती हैं, पर बताने की यह आवश्यकता चुनावों के समय पर ही किसी को याद क्यों आती है?
ऐसा नहीं है कि इस तरह के सवाल पहले कभी उठे नहीं हैं। उठते रहे हैं ये सवाल, पर राजनीतिक नफा-नुकसान का गणित इन सवालों को उठाने वाली नैतिकता पर अक्सर हावी हो जाता है। कभी महिला मतदाताओं को साड़ियां बांटकर तमिलनाडु की जयललिता ने वोट के लिए रिश्वत की इस परंपरा की शुरुआत की थी। द्रमुक के ही करुणानिधि ने दो रुपये किलो चावल बांटकर इस शुरुआत को चुनाव जीतने की एक कला के रूप में विकसित किया। फिर तो जैसे देश के अलग-अलग हिस्सों में इस कला को निखारने की एक प्रतिस्पर्धा ही चल पड़ी। ऐसा भी नहीं है कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की ज़रूरत की ओर किसी का ध्यान न गया हो। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने इस ‘रेवड़ी संस्कृति’ को मुद्दा बनाया था। पर जल्दी ही उन्हें यह अहसास हो गया कि यह संस्कृति तो स्वयं उनके लिए भी लाभदायक है और वे भी लाभ लुटाकर लाभ कमाने की इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गये।
अब तो हमारे राजनीतिक दल यह सोचना भी नहीं चाहते कि इस प्रतियोगिता में राज्यों का बजट घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है—यह घाटा खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। यही सब देखते हुए यह मांग भी उठी थी कि मुफ्त संस्कृति वाली इस राजनीति के वित्तीय अनुशासन के बारे में भी कुछ नियम-कायदे बनने चाहिए। कहा यह भी गया कि चुनाव घोषणापत्रों में ऐसी युक्तियों-योजनाओं के साथ उन पर होने वाले व्यय का ब्योरा भी दिया जाना चाहिए, यह भी बताया जाना चाहिए कि इन योजनाओं पर होने वाले खर्च की व्यवस्था कैसे होगी। इस संदर्भ में रसोई घर की मुफ्त सिलेंडर वाली योजना के हश्र की बात भुलाई नहीं जानी चाहिए। इस बात का भी लेखा-जोखा होना चाहिए कि मुफ्त सिलेंडर कैसे मिलेंगे और कैसे मिलते रह सकेंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। होता दिख भी नहीं रहा।
यहां यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि उच्चतम न्यायालय ने भी इस संदर्भ में हस्तक्षेप किया था। न्यायालय ने तो यह भी कहा था कि राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में ऐसी योजनाओं की घोषणा को किसी तरह की कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। पर, जो होना चाहिए, और जो हो रहा है, हमारी राजनीति में उसमें बहुत अंतर है। यह अंतर कब और कैसे पटेगा, पता नहीं। लेकिन यह तय है कि हमारे राजनेता इस बारे में लगातार सक्रिय हैं कि यह अंतर मिटाने की बात ही न हो। वे मानते हैं कि जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। इसलिए, राजनीति की रेवड़ी संस्कृति के बारे में कभी-कभार बात तो कर ली जाती है, पर इस संस्कृति के खतरों से बचने की आवश्यकता किसी को महसूस नहीं होती।
राजनीतिक नैतिकता का तकाज़ा है की राजनीति की यह घटिया संस्कृति समाप्त हो, पर राजनीतिक आवश्यकता इस नैतिकता को कहीं पीछे छोड़ देती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर हमारे नेता तो यह भी जानते हैं कि चुनाव की आदर्श आचार संहिता का मजाक कैसे उड़ाया जा सकता है–बिहार में चुनावों की तारीख की घोषणा के ठीक पहले मेट्रो लाइन के उद्घाटन का लालच मुख्यमंत्री छोड़ नहीं पाये। सुना है, यह लाइन अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं है! स्पष्ट है, राजनीतिक स्वार्थ किसी भी अनुशासन को स्वीकार नहीं करते।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।