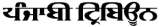इस जटिलता की मार्गदर्शक व्याख्या वाजपेयी से बेहतर कोई नहीं कर सका, जब 2003 में उन्होंने श्रीनगर यात्रा में कहा, ‘भारत कश्मीरियों से इंसानियत, कश्मीरियत और जम्हूरियत के दायरे में बात करेगा’।
दिल्ली उच्च न्यायालय में यासीन मलिक का शपथपत्र, जिससे एक बड़ा बवाल खड़ा हो सकता था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि यह रहस्योद्घाटित करता है कि पिछले तीन दशकों में विभिन्न विचारधाराओं वाली सरकारों ने कैसे इस कश्मीरी अलगाववादी नेता को कभी दुलारा तो कभी झटक दिया। यह हल्फनामा उसी माह में आया है जब एक साल पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए थे।
शायद कुछ लोग उबासी लेते हुए पूछेंगे, कौन यासीन मलिक? अन्य, जिन्हें 1989 में तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया के अपहरण और 1990 में कश्मीर में चार वायुसेना अधिकारियों की निर्मम हत्या में यासीन की भूमिका के बारे में पता होगा। उन्हें पता होगा कि यासीन को तब से लेकर अब तक, हर प्रधानमंत्री- चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के अलावा प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में भी वार्ताकारों ने डोरे डाले। एक तरह से, मलिक का हलफनामा पिछले दशकों के कश्मीर का कहानीनामा है। यह शक्तिशाली भारतीय राज्य द्वारा इस अशांत क्षेत्र में शांति लाने हेतु अनेक प्रयोगों को समेटे हुए है-यासीन जैसे अतिवादी और मीरवाइज़ उमर फारूक जैसे उदारवादी नेताओं के अतिरिक्त हिज़बुल मुजाहिदीन के नेताओं को लुभाना, इस आस में, कि ये अलगाववादी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को नया अध्याय बनाने पर मना लेंगे- और यह भारत और पाक के नेताओं के बीच एक ठोस वार्ता प्रक्रिया की ज़मीन तैयार करने में मददगार रहेगा।
कम-से-कम 16 सालों तक, 1998 में बाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने से लेकर 2014 में मनमोहन सिंह के सत्ता गंवाने तक, भारतीय राज्य ने ऐसी महत्वाकांक्षी त्रिकोणीय वार्ताओं की कोशिशें जारी रखी– भारत के कश्मीरी अलगावादियों और पाकिस्तान के मध्य, भारतीय कश्मीरी नेताओं और केंद्र सरकार के बीच, और भारत एवं पाकिस्तान के बीच। इसकी व्याख्या वाजपेयी से बेहतर कोई नहीं कर सकता था, जब 2003 में उन्होंने श्रीनगर यात्रा में कहा, ‘भारत कश्मीरियों से इंसानियत, कश्मीरियत और जम्हूरियत के दायरे में बात करेगा’। यहां ‘संविधान’ शब्द का ज़िक्र नहीं था, फिर भी हर कोई जानता था कि लक्ष्मण रेखा क्या है- हिंसा नहीं; क्योंकि ये बातचीत के दरवाज़े बंद कर देती है।
इसलिए जब मनमोहन सिंह ने वाजपेयी के काम को आगे बढ़ाया, तो देश ने श्लाघा की। यह कभी न भूलें कि मनमोहन सिंह ने न केवल 2006 में नेपाल में नेपाली लोकतंत्र में मदद की, बल्कि उन्होंने पहली बार कश्मीरी नेताओं को नियंत्रण रेखा के परे पाक जाने को प्रोत्साहित किया ताकि गुंझलदार और बंद पड़ी सीमारेखा को लचीला बनाया जा सके। इस बीच, सिंह के विशेष दूत और पूर्व राजनयिक सतिंदर लांबा, दुबई और लंदन में अपने पाक समकक्षों से मिल कर चार-सूत्रीय फ़ॉर्मूला का मसौदा तैयार कर रहे थे। जिससे कि न केवल कश्मीर में शांति बहाल हो बल्कि उस संत्रास का हल भी, जिससे भारत-पाक को 1947 में गुजरना पड़ा। उपमहाद्वीप में रोमांच था कि क्या यह दीर्घकालीन सुखद स्थिति होगी।
यासीन मलिक के बारे में एक कहानी है, जो कश्मीर मामलों के जानकार और 1990 के दशक के भयावह दिनों में कश्मीर में नियुक्त रहे आईएएस अधिकारी वज़ाहत हबीबुल्लाह बताते हैं। यह 2002 के घटनाक्रम के बारे में है, जब जम्मू-कश्मीर में चुनाव होने वाले थे, तब हबीबुल्लाह ने यासीन, मीरवाइज़ और हुर्रियत के लोगों से कहा कि अगर वे चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे तो उनसे कश्मीर के हक में बोलने की उम्मीद कैसे करें?
हुर्रियत नेता सहमत हो गए, लेकिन भारत के चुनाव आयोग पर अविश्वास जताने पर हबीबुल्लाह ने यह बेचैनी तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त जेम्स लिंगदोह से व्यक्त की। उनका सुझाव था कि एक राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जा सकता है। कश्मीरी नेताओं ने पेशकश पर विचार-विमर्श किया और यासीन मलिक से कहा कि इस आयोग का हिस्सा बनने हेतु विश्वसनीय लोगों को राज्य संस्थान में शामिल करें- कर्ण सिंह को बतौर अध्यक्ष लिया।
बेशक, कर्ण सिंह कश्मीर के अंतिम हिंदू महाराजा हरि सिंह के पुत्र हैं, जो 1947 के अक्तूबर माह तक भी भारत में विलय को लेकर असमंजस में रहे, जब तक कि नेहरू-पटेल ने सेना भेजकर उन्हें अंतिम मौका नहीं दिया; कर्ण सिंह ने बतौर केंद्र का प्रतिनिधि शासक, अपने पिता की जगह 1949 में ली और अंतिम सदर-ए-रियासत बने। निस्संदेह, मौजूदा कालखंड कम संशय, अधिक स्पष्टता और कहीं कम विडंबनाओं भरा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, ऑपरेशन बालाकोट में रह गई गलतियों को ऑपरेशन सिंदूर ने सुधार दिया। एक साल पहले, और अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के पांच साल बाद, बतौर केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में, फिर से चुनाव हुए। लेकिन अपने मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का उत्साह अब मायूसी में बदल चला है, क्योंकि निर्णायक फैसले लेते उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दौर में पूर्ण राज्य दर्जा बहाली की संभावना दिखती नहीं। यहां तक कि सवाल भी टेढ़े हैं। अब वह बात नहीं रह गईः ‘मत पूछो कि देश कश्मीर के लिए क्या कर सकता है’, बल्कि यह हैः ‘कश्मीर देश के लिए क्या कर सकता है’। क्या यह चुनाव जीतने में मददगार होगा, जैसे बिहार में?
कश्मीरी कहानी कई तरीकों से लिखी जा सकती है- यासीन मलिक के हलफनामे के ज़रिए, जो 2022 से तिहाड़ जेल में बंद है, जब उसे 20 साल पहले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इस मामले में उसने अपना अपराध स्वीकार किया है; या एएस दुलत की लिखी किताबों के जरिए, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख और वाजपेयी के विशेष सलाहकार रह चुके हैं– ‘द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई’ नामक उनकी नवीनतम किताब ने अप्रैल में राष्ट्रीय स्तर पर तहलका मचा दिया था, क्योंकि इसमें उन्होंने बेबाक रहस्योद्घाटन किया है कि भारतीय राज्य कश्मीर को किस प्रकार चलाता आया है।
शायद यही कहानी का सार है कि राज व्यवस्था मुख्यतः निर्दयी होती है, और जब वह यासीन मलिक जैसे किसी को छूट दे रही होती है, तो यह वास्तव में उसे आभास देना होता है मानो वह भू-राजनीतिक बिसात पर एक बड़ा पात्र है (या था)– जबकि वह डोर-चालित कठपुतली होता है।
पाक सैन्य प्रतिष्ठान के दंभ को भी कभी न भूलें। उसने भी इस मोड़ पर खड़ा किया है- परवेज़ मुशर्रफ़ का वाजपेयी और मनमोहन सिंह, दोनों के साथ समझौता बनाने से पीछे हटना, अदूरदर्शिता-मूर्खता का मिश्रण है, उस बेवकूफी का एक उदाहरण है। पाकिस्तानियों ने 2008 में मुंबई आतंकी हमले से भारत के मर्मस्थल को चोट दी। अप्रैल के पहलगाम नरसंहार ने जख्म कुरेदे तो ऑपरेशन सिंदूर ने इस याद का बदला लिया।
और इसलिए गत शनिवार की सुबह, कश्मीर-गाथा के पन्नों को पटलते वक्त, असमंजस था कि इस पर कैसे लिखा जाए। मुझे भान है कि इस विषय में मुझे उस एक लेखक की कमी हमेशा खलेगी, वह गैर कश्मीरी जिसे कश्मीर के अंदर तक की पूरी खबर रहती थी, जिनके लिखे को पढ़ना हमेशा बहुत आनंददायक था यानी विद्वान पत्रकार संकर्षण ठाकुर। उनके सारगर्भित लेख आशाओं, सपनों और आशंकाओं को, और सबसे बढ़कर, उस तर्क-वितर्क की लड़ाई, जिसने कश्मीरियों की कई पीढ़ियों को लील लिया, को व्यक्त करते रहे। वे होते तो, यासीन मलिक के हलफनामे को तोलकर उस पर विचार देते। उनके निधन से कश्मीर की असल कहानी जानने में और कमी बनेगी।
लेखिका ‘द ट्रिब्यून’ की प्रधान संपादक हैं।