सेवाओं की पेशेवराना दक्षता का क्षरण
गुरबचन जगत(मणिपुर के पूर्व राज्यपाल, पूर्व डीजीपी जम्मू व कश्मीर) कुछ हफ़्ते पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। यह बलात्कार और हत्या कांड इतना घिनौना था कि पूरे देश...
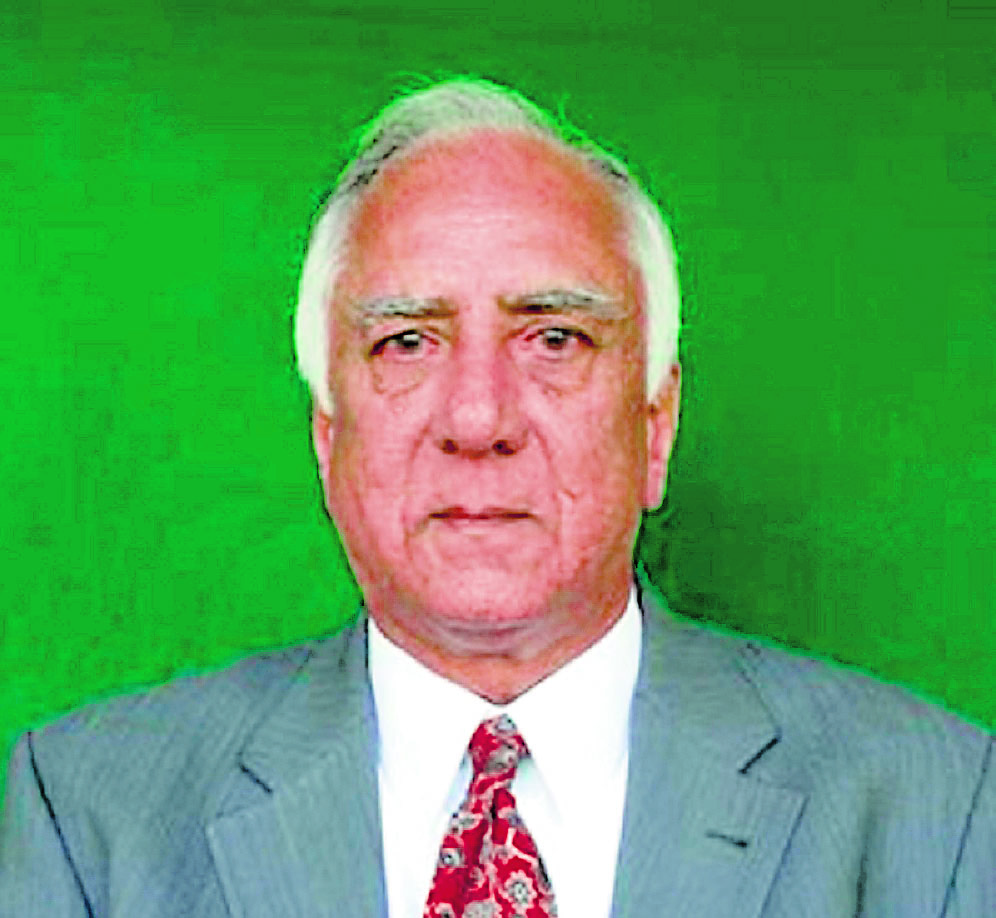
(मणिपुर के पूर्व राज्यपाल, पूर्व डीजीपी जम्मू व कश्मीर)
कुछ हफ़्ते पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। यह बलात्कार और हत्या कांड इतना घिनौना था कि पूरे देश को झकझोर दिया। स्वतःस्फूर्त गुस्से और पीड़ा की भावना की अभिव्यक्ति -हिंसक और अहिंसक- दोनों किस्म के प्रदर्शनों के रूप में हुई, खास तौर पर डॉक्टरों के समुदाय में, जिन्होंने देश भर में हड़तालें की। सीबीआई से जिस त्वरित परिणाम की अपेक्षा थी, वह पूरी नहीं हुई। इस हस्तक्षेप के बाद भी, पूरे देश में बलात्कार और हत्या जैसी अन्य कई जघन्य वारदातें हुईं, लेकिन अदालतों या अन्य सामाजिक समूहों ने उन पर उतना ध्यान नहीं दिया। पहले के मामलों में भी, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद ऐसे हिंसक बलात्कार और अन्य अपराध रुके नहीं और इस वाले से भी इनके रुकने की संभावना नहीं है। हालांकि, यह मामला सीबीआई को सौंपना पूरी तरह से उचित था, परंतु मेरे ज़ेहन में एक अलग विचार कौंध रहा है- क्योंकर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने राज्य पुलिस बलों की व्यावसायिकता और ईमानदारी पर भरोसा खो दिया? नागरिकों का राज्य पुलिस और पुलिस थानों पर से यकीन क्यों उठ गया? यहां तक कि राज्य सरकारों और निचली अदालतों से भी? क्या यह सब रातों-रात हुआ या धीरे-धीरे इसलिए बढ़ता गया क्योंकि अब राजनेता सर्व-शक्तिमान होते जा रहे हैं और वे पुलिस बल एवं सरकार के अंदर और बाहर बैठे आपराधिक तत्वों की मदद से यह सारा खेल चला रहे हैं।
इतिहास पर नज़र डालें तो, उस वक्त भ्रष्टाचार के केवल अति महत्वपूर्ण मामले ही अदालतों या राज्य अथवा केंद्र सरकारों द्वारा सीबीआई को सौंपे जाते थे। सूबों के अधिकारी मामलों के ऐसे हस्तांतरण पर तौहीन महसूस करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनकी कारगुजारी पर अंगुली उठती है। सीबीआई को अच्छे परिणाम भी मिले, क्योंकि एक तो इस पर काम का बहुत ज्यादा बोझ नहीं था, दूसरे इसकी शुरुआत केवल उच्च स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में हुई थी। किंतु राजनीतिक भुजा के लगातार मजबूत होते जाने और इससे जुड़े नैतिक पतन, एवं ईमानदारी में कमी होते देख लोगों ने मामले सीबीआई को सौंपने की मांग के साथ सीधे अदालतों का रुख करना शुरू कर दिया। राज्य और केंद्र सरकारें भी अपने-अपने वांछित परिणाम पाने को इसी राह का सहारा लेने लगीं, क्योंकि जब राजनीतिक निकाय का समग्र पतन हुआ तो सीबीआई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। अधिकारियों को विशेष रूप से नियुक्त किया गया ताकि तंत्र को और अधिक लचीला बनाया जा सके। सीबीआई ने भी विस्तार किया और अधिकांश राज्यों में शाखाएं खोलीं। हालांकि, इसने केंद्र सरकार की इच्छाशक्ति को और हवा दी और एक नई तफ्तीश संस्था के रूप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का जन्म हुआ, काम इसका भी जांच करना है लेकिन अधिक ध्यान उन आतंकी गतिविधियों पर केंद्रित है, जिनका प्रभाव-क्षेत्र अंतर्राज्यीय हो। यहां भी, केंद्र सरकार की मनमर्जी है कि कौन सा मामला इसे सौंपना है। गृह मंत्रालय (एमएचए) की ओर से लगातार बयान आते रहते हैं कि सभी राज्यों में एनआईए कार्यालय खोले जाएंगे।
हमारे पास पहले से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राष्ट्रव्यापी जांच क्षेत्र के अधिकार से सशक्त बनाई गई ईडी है,इनके अलावा आईबी और रॉ भी हैं। हमारे पास अर्धसैनिक बल भी हैं,उनका कार्यक्षेत्र भी अखिल भारतीय है। कानून-व्यवस्था के मामले जिनसे निबटना राज्य पुलिस बलों के बूते के परे माना जाता है,उनके लिए अर्धसैनिक बल बने हैं। जरूरत पड़ने पर राज्य सरकारें इन बलों की मांग गृह मंत्रालय से कर सकती हैं या गृह मंत्रालय राज्य सरकार की नाममात्र मंजूरी के साथ उन्हें सीधे राज्य में भेज सकता है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी आदि अनेक राज्यों में कई दशकों से लगातार तैनात हैं। कागज़ों पर वे राज्य पुलिस के अधीन काम करते हैं, लेकिन रोजमर्रा के कार्यों में स्वतंत्र हैं। तब फिर राज्य सरकार और इस तथ्य के बारे में क्या रह जाता है, जब कहा जाए कि संविधान के अनुसार कानून एवं व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है? पुलिस स्टेशन और जिले का एसपी पुलिस तंत्र के बुनियादी भाग होते हैं। लेकिन अतिरिक्त विभागीय हस्तक्षेपों ने दोनों को सत्तारूढ़ पार्टी का अनुचर बना डाला है। इस ह्रास की कीमत राज्य पुलिस की व्यावसायिकता ने चुकाई है, इस गिरावट का विशेष रूप से असर अग्रणी स्तर पर यानि पुलिस स्टेशन और जिला एसपी पर हुआ है। यह दो जगहें ऐसी हैं,जहां पुलिस एवं जनता के बीच सीधा राब्ता होता है, लेकिन इस सम्पर्क में बहुत कुछ करने की जरूरत है। यह वह राब्ता नहीं है जिसमें नागरिक इस विश्वास के साथ वहां जाए कि उसे न्याय मिलेगा, बल्कि वह एक ग्राहक या याचक के रूप में जाता है।
एक सुसंचालित और सुघड़ नेतृत्व वाला पुलिस स्टेशन वह होता है जिसके पास सर्वश्रेष्ठ मुखबिर तंत्र हो और यह सूचना एवं बढ़िया अभियान नीति होती है, जो सफलता दिलवाती है। हमने जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तर-पूर्व में आतंक व मध्य भारत, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश में माओवादी आंदोलनों में भी यही देखा है कि अभियान चलाने में सूचना सबसे सटीक वही होती है, जो पुलिस थाने से आती है। यही कारण है कि सेना सहित तमाम अभियान समूहों में स्थानीय पुलिस थाना एक महत्वपूर्ण घटक होता है। अपराध सामान्य हो या जटिल या फिर विद्रोही गतिविधियां, तमाम अभियानों में सफलता तभी मिलती है जब पुलिस के काम की धुरी यानी थाना पूरे जी-जान से शामिल रहे। अगर यह सही है तो फिर इसे कमजोर क्यों किया जा रहा है? कारण यह है कि वक्त की हुकूमत चाहती है कि पुलिस बल देश के कानून की बजाय उनके प्रति एक रीढ़ विहिनऔर वफादार बल बना रहे। केंद्र सरकार ने नाना प्रकार की जांच एजेंसियों की स्थापना करके और कौन सा मामला किसे सौंपना है, इसमें अपनी मनमर्जी चलाकर राज्य की जांच एजेंसियों को कमजोर कर डाला है। वहीं राज्य सरकारों ने भी पुलिस विभाग के आंतरिक प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप करके और शीर्ष पदों पर अवांछनीय तत्वों को नियुक्त करके बहुत नुकसान पहुंचाया है। पुलिस थानों पर लगभग पूरी तरह इन शक्तियों का कब्ज़ा हो गया है। ऐसा कहने का मतलब हर्गिज़ यह नहीं कि आज़ादी के समय की तुलना में कहीं ज़्यादा जनसंख्या वाले आधुनिक भारत की बढ़ती ज़रूरतों के मुताबिक बेहतर और ज़्यादा पेशेवर विशेष बलों की ज़रूरत नहीं है, मसलन साइबर अपराध। लेकिन मुख्य चीज़ है ऐसी पेशेवर एजेंसियों की स्थापना, जिनमें राजनीतिक दखलअंदाज़ी न्यूनतम हो और राज्य एवं केंद्र के बीच समन्वय उच्च मानकों के स्तर पर बना रहे।
पुलिस सुधार हो या अपराध की जांच या कानून-व्यवस्था बनाए रखना,इनसे संबंधित तमाम मामलों में जो एक सबसे बड़ी अड़चन है, वह है राजनीतिक प्रतिष्ठान। जब तक इस समस्या के निदान और पुलिस के कामकाज के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं बनती,तब तक स्थितियां और बदतर होती जाएंगी। यहां तक कि पुलिस सुधारों के बारे में उच्चतर न्यायपालिका के आदेश भी नौकरशाही की कागज़ी कलाबाज़ी में गुम हो गए हैं। हमारी शासन प्रणाली में सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित राजनीतिक दल के पास है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उक्त शक्ति बेलगाम है, क्योंकि संविधान और देश के विभिन्न कानूनों में प्रशासन चलाने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्तारूढ़ दल जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता शांति एवं न्यायपूर्ण प्रशासन चाहती है। क्या सुधारों और न्याय पाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा? उम्मीद है कि निर्वाचित सरकारें सड़कों से मिल रहे संदेश को समझगी।
लेखक ‘द ट्रिब्यून’ के ट्रस्टी हैं।






