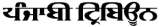मतदाता की जागरूकता से ही निरंकुशता पर अंकुश
यदि किसी नेता को यह भ्रम होने लगे कि वह सेवक नहीं, मालिक है तो यह एक तरह से जनतंत्र को नकारना ही होगा। ऐसा व्यक्ति बड़ी आसानी से निरंकुश हो सकता है, और यह स्थिति किसी भी दृष्टि से...
यदि किसी नेता को यह भ्रम होने लगे कि वह सेवक नहीं, मालिक है तो यह एक तरह से जनतंत्र को नकारना ही होगा। ऐसा व्यक्ति बड़ी आसानी से निरंकुश हो सकता है, और यह स्थिति किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।
बिहार का चुनाव भी हो गया। परिणाम कुल मिलाकर अप्रत्याशित तो रहे पर इतने अप्रत्याशित नहीं कि उन पर हैरान ही हुआ जाये। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह के हालात बनते दिख रहे थे, उनमें कहीं न कहीं यह तो लगने लगा था कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को जीत मिल सकती है पर इतनी बड़ी जीत होगी, ऐसा नहीं लग रहा था। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि महागठबंधन की इतनी बुरी हार होगी, ऐसा भी नहीं लग रहा था। पर ऐसा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी जीत और राजद की ऐसी हार अप्रत्याशित तो थी, पर यह भी समझना ज़रूरी है कि यह स्थिति चिंताजनक भी है। सत्तारूढ़ पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं, देश में जनतंत्र के भविष्य के लिए यह स्थिति चिंताजनक है।
हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था में मजबूत सरकार का होना कतई चिंता की बात नहीं है, पर विपक्ष का इतना कमज़ोर हो जाना निश्चित रूप से चिंता की बात होनी चाहिए। यह पहली बार नहीं है कि किसी विधानसभा में, या फिर संसद में भी, असंतुलित परिणाम आये हैं–इतने असंतुलित परिणाम कहना चाहिए इसे! और यह ‘इतने’ शब्द यहां चिंता की बात को प्रकट करता है। ऐसी जीत जीतने वाले को अति विश्वास से भर देती है और यह अति विश्वास उसे, कुछ भी कर सकता हूं, का अहसास दिलाने वाला होता है। अच्छा और मज़बूत होने का अहसास ग़लत नहीं है, पर यह मज़बूती यदि घमंड में बदल जाती है तो इसे सही नहीं कहा जा सकता। सही नहीं होने का यह खतरा आज हमारे जनतंत्र पर मंडरा रहा है।
ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थितियां पहले कभी नहीं बनीं। राज्यों में भी ऐसा हो चुका है, और केंद्र में भी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब चुनाव हुए थे तो राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को लोकसभा में चार सौ से अधिक सीटें मिली थीं। अति घमंड की स्थिति बन सकती थी। पर तब कांग्रेस को यह अहसास था कि उसे सहानुभूति की लहर का लाभ मिला है। पर अब बिहार में भाजपा की जीत के मामले में ऐसी बात नहीं है। उसके पक्ष में कोई ‘सहानुभूति लहर’ नहीं थी। भाजपा और ‘जदयू’ की जीत तथा कांग्रेस और राजद की हार के कारणों पर विचार होगा और भविष्य में भी होता रहेगा। पर इस बात पर विचार होना ज़रूरी है कि इस तरह के अप्रत्याशित परिणाम चिंता का कारण भी होने चाहिए। कोई जीत इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि जीतने वाला स्वयं को अपराजेय समझने लगे और कोई भी हार इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए कि हारने वाले को यह लगने लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची।
बहरहाल, बिहार के इन चुनाव- परिणामों पर दो दृष्टियों से विचार होना चाहिए–पहले तो इस दृष्टि से कि क्या जीतने वाला अपनी श्रेष्ठता के कारणों से ही जीता है और दूसरी यह कि हारने वाला कहां चूक गया। भाजपा की जीत पर उंगली उठाने वालों का मानना है कि चुनाव में ऊंच-नीच हुई है। यह सवाल चुनाव आयोग पर भी है। उस पर आरोप लग रहा है कि उसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों, से भाजपा की जीत में मदद की है। इस तरह के आरोप मतदान से पहले भी लगते रहे थे, अब भी लग रहे हैं। ऐसी ही किसी मदद से इनकार के अलावा और कोई ठोस प्रमाण चुनाव आयोग ने नहीं दिया। चुनाव आयोग से यह अपेक्षा और उम्मीद की जा रही है कि वह यह बतायेगा कि भाजपा की बिहार सरकार को एक करोड़ 10 लाख महिला मतदाताओं को चुनाव से ठीक पहले दस-दस हजार रुपये नकद सहायता देने से रोका क्यों नहीं गया? पहले भी सरकारें नकद रेवड़ियां बांटती रही हैं। महाराष्ट्र के पिछले चुनाव में भी ‘लाड़ली बहिना’ को नकद सहायता देने के आरोप लगे थे। तब आरोप यह भी था कि भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने तब हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव एक साथ नहीं कराये थे, जबकि पिछले 15 सालों से इन दोनों राज्यों में चुनाव साथ-साथ होते आये हैं। चुनाव आयोग पर आरोप लगा था कि महाराष्ट्र में चुनाव तीन-चार महीने टालकर उसने महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार को रेवड़ियां बांटने का पर्याप्त समय दिया था। आयोग ने इस आरोप का कोई विश्वसनीय उत्तर नहीं दिया था।
जहां तक बिहार में हारने वाले की चूक का सवाल है, इस बात के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं कि कांग्रेस और राजद दोनों ने वह ताकत नहीं लगायी जो जीतने के लिए ज़रूरी होती है। सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में दोनों ने एक तरह से अत्यधिक देरी की थी। नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत आरोप लगाने की नीति भी गलत सिद्ध हुई। उधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का चुनावों को हल्के में लेने का रवैया भी कुल मिलाकर आत्मघाती ही सिद्ध हुआ। महागठबंधन के साथी सहयोगियों को अपनी कमज़ोरी और गलतियों पर गंभीरता से विचार करना होगा।
पर गंभीरता से विचार करने का एक मुद्दा और भी है, और उसका सीधा रिश्ता हमारे जनतंत्र के भविष्य से है। बिहार विधानसभा में 200 से अधिक सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगियों के जीतने का एक अर्थ सत्तारूढ़ पक्ष का ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर होना भी है। ऐसी जीत की उम्मीद तो भाजपा को भी नहीं थी। पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने भी मतगणना के पूर्व अधिकतम 160 सीटें जीतने की बात कही थी– अर्थात् उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अधिक सीटें मिल सकती हैं। कारण कुछ भी रहे हों, चुनाव परिणामों ने भाजपा को अति विश्वास की सीमा तक तो पहुंचा ही दिया है।
बात सिर्फ अति विश्वास तक ही सीमित नहीं है। ऐसी स्थिति के दो परिणाम हो सकते हैं– पहला तो यह कि ऐसी जीत वाले दल या नेता को यह लगने लगता है कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता और दूसरा यह कि ऐसी जीत वाले नेता को अपने भूतो न भविष्यति होने का भ्रम होने लगता है। जनतंत्र की दृष्टि से यह दोनों परिणाम खतरनाक हैं। जनतंत्र का मतलब किसी नेता या दल का नहीं, जनता का शासन होता है। ऐसे में यदि किसी नेता को यह लगने लगे कि वह सर्वशक्तिमान है, अजेय है, तो यह उस मतदाता का घोर अपमान है, जो अपना नेता चुनता है। यह व्यक्ति वस्तुत: नेता नहीं होता, मतदाता का प्रतिनिधि होता है, जनता की ओर से चुना गया जनतंत्र का सेवक, जो जनता के लिए काम करता है।
जनतंत्र को जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार कहा जाता है। यदि किसी नेता को यह भ्रम होने लगे कि वह सेवक नहीं, मालिक है तो यह एक तरह से जनतंत्र को नकारना ही होगा। ऐसा व्यक्ति बड़ी आसानी से निरंकुश हो सकता है, और यह स्थिति किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर जनता का अंकुश ज़रूरी है, और ऐसा व्यक्ति कभी भी अंकुश स्वीकार करना नहीं चाहेगा!
इसलिए जनतंत्र में विपक्ष का मज़बूत होना ज़रूरी माना जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में एक बार संसद में विपक्ष बहुत कमज़ोर हो गया था। तब उन्होंने सदन में कांग्रेसी सदस्यों से कहा था कि वे सरकार के काम-काज पर निगाह रखें, ताकि सरकार या प्रधानमंत्री निरंकुश न हो जाये। यह निरंकुशता चुनावी तानाशाही तक ले जा सकती है। आज दुनिया के कई देशों में यह प्रवृत्ति पनप रही है। जनतांत्रिक मूल्यों-आदर्शों का तकाज़ा है कि इस प्रवृत्ति को रोका जाये। बिहार के चुनाव-परिणामों को इस दृष्टि से भी देखा जाना ज़रूरी है। बात सिर्फ चुनाव में ऊंच-नीच के आरोपों तक ही सीमित नहीं है। इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, पर जागरूक इस बात के लिए भी रहना होगा कि कोई राजनेता या राजनीतिक दल स्वयं को अपराजेय न समझने लगे। जरूरत यह समझने की भी है कि चुनाव परिणाम से चुनाव आयोग अथवा कोई भी पक्ष आरोपमुक्त नहीं हो जाता। इसलिए बात फिर मतदाता की जागरूकता पर आकर टिकती है। सतत जागरूकता पर।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।