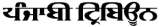अज्ञेय से पहली मुलाकात
संस्मरण
मृदुला गर्ग
अज्ञेय से मेरी पहली मुलाकात 1974 में हुई, जब मेरी बहन मंजुल भगत का पहला कहानी संग्रह गुलमोहर के गुच्छे भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। मैं दस बरस दिल्ली से बाहर रहने के बाद, तभी वापस लौटी थी। 1970-71 में हम दोनों ने, करीब-करीब एक साथ, लेखन शुरू किया था। मेरी तब तक कोई पुस्तक छपी न थी। मंजुल की पहली किताब के प्रकाशन की खुशी में सप्रू हाउस में चायपान था। लगे हाथों दो-चार लेखक-आलोचक किताब पर बातचीत भी करने वाले थे। एक दिन, अचानक, मंजुल मेरे घर आईं और बोलीं, ‘मजा तब आए जब जलसे में अज्ञेय आएं।’ मैंने कहा, ‘बुला लेते हैं।’
आप समझ गए होंगे, हम हिंदी साहित्य के राजनीतिक शिष्टाचार से किस कदर अनभिज्ञ थीं। अलबत्ता अज्ञेय के साहित्य से नहीं। ख़ूब पढ़ा था उन्हें। उन दिनों, अज्ञेय हिंदी साहित्य गगन पर सूर्य की तरह देदीप्यमान थे। पर चूंकि मंजुल ने एम.ए अंग्रेजी में नाम लिखवाया था, डिग्री भले न ली हो और मैंने एम.ए करके तीन साल अर्थशास्त्र पढ़ाया था, हमें हिंदी जगत के सोपानतंत्र और चरण-स्पर्शीय शिष्टाचार की आदत न थी। मिरांडा हाउस और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स में, नामी-गिरामी प्रोफेसरों और अर्थशास्त्रियों से हम बराबरी के दर्जे पर बहस करते रहे थे। घर का संस्कार भी बौद्धिक और उदार था, हर उम्र का सदस्य अपनी राय देने को सर्वथा स्वतंत्र था। दरअसल पिता जी का अज्ञेय से अच्छा परिचय था पर उन्होंने उनसे बात करने से इन्कार कर दिया। कहा, हम दोनों से अपना रिश्ता वे तभी जाहिर करेंगे जब वे हमारे पिता की तरह जाने जा सकें, हम उनकी बेटियों की तरह नहीं। तकदीर हमारी, ऐसे नैतिक जन हमारी ही किस्मत में लिखे थे!
हमने तय किया, अज्ञेय को फोन करके जलसे में आमंत्रित किया जाए। फिर हमने काल्पनिक सिक्का उछाला, जो हमेशा की तरह, मेरे विपरीत पड़ा। यानी फोन करने का जिम्मा मेरा हुआ। फोन मिलाया गया, अज्ञेय ने खुद उठाया या उन्हें दिया गया, याद नहीं। मैंने कहा, ‘वात्स्यायन जी, मेरा नाम मृदुला गर्ग है, आप मुझे नहीं जानते। मेरी बड़ी बहिन हैं, मंजुल भगत, उन्हें भी आप नहीं जानते। उनकी पहली किताब गुलमोहर के गुच्छे छप कर आई है। उस खुशी में हम फलां तारीख को फलां वक्त सप्रू हाउस में चायपान कर रहे हैं, आप आइए।’
पूछा गया, किताब कहां से छपी थी। मैंने बतलाया, भारतीय ज्ञानपीठ से।
तब मंजुल ने मेरे हाथ से फोन ले लिया और बोलीं, ‘यह वही भारतीय ज्ञानपीठ है जिसने सुमित्रानन्दन पंत को पुरस्कार दिया था।’
वात्स्यायन जी ने कहा,’समझ रहा हूं पर पुस्तक मेरे पास आई नहीं।’
‘ओहो, हम आ कर दे जाते हैं। बंगाली मार्केट से आपके घर कौन-से नंबर की बस आती है?’
‘रहने दीजिए,’ अज्ञेय ने कहा और फोन कट गया।
मैंने कहा,’अजीब अहमक है तू। उनसे बस का नंबर पूछने की क्या जरूरत थी। हम खुद पता कर लेते।’
वह बोली, ‘तू कौन कम बेवकूफ है। मैं मृदुला गर्ग हूं, आप मुझे नहीं जानते, वह मंजुल भगत है, आप उसे नहीं जानते… ऐसे भला कोई आता है।’
हमने तय पाया कि अज्ञेय नहीं आएंगे।
पर वे आए। सबसे पहले आए। देर तक रहे। किताब देखी, शायद एक कहानी पढ़ भी डाली, बोले, ‘ऐसी बहनों को देखने का मोह कैसे छोड़ता, जो अपनी पुस्तक की खुशी खुद मना रही हों।’मंजुल ने दबे स्वर में मुझसे कहा, ‘यह तो ऐसे है कि कोई पूछे, आप अपने जूते खुद पॉलिश करते हैं तो जनाब कहें, आप किसके करते हैं?’ यानी हम बौड़म समझ नहीं पाए कि अपनी किताब की खुशी खुद क्यों नहीं मनाई जा सकती। उनसे नहीं कहा तो उनके व्यक्तित्व के प्रभामण्डल के दबाव में। यह वह जमाना था, जब रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बाद किसी लेखक की सदेह छवि मोहित करती थी तो अज्ञेय की। अपनी छवि की तराश में वे सजग-सतर्क थे। एक शब्द में कहना हो तो उस छवि को यही नाम दूंगी, तराश। तराशी हुई दाढ़ी, तराश के साथ इस्तरी किया लिबास, तराशा-सधा स्वर, तराशे हुए तेवर। तराशा रचनाकर्म और चिंतन। तराशी हुई आत्मकथा यानी शेखर एक जीवनी। तराशी यायावरी। तराशा प्रेम, कई बार या एक बार भी नहीं? वैसा ही अहं। दूसरे के अहं को तराश कर बौना बनाने का माद्दा। साधारण को तराश कर सानुपातिक कर डालने का भी।
(हिंदी समय डॉट काॅम से साभार)
अगले अंक में पढ़ें:-
अज्ञेय-जैनेन्द्र तनातनी व अन्य के बारे में