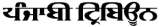समाजचेता उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद
पुष्पपाल सिंह क्या और भी किसी देश में इसी प्रकार का धर्म-संचय होता है ? जिन्हें आवश्यकता नहीं, उनको बिठाकर आदर से भोजन कराया जाए, केवल इस आशा से कि परलोक में वे पुण्य-संचय का प्रमाण-पत्र देंगे, साक्षी देंगे, और इन्हें, जिन्हें पेट ने सता रखा है, जिनको भूख ने अधमरा बना दिया है, जिनकी […]
पुष्पपाल सिंह
क्या और भी किसी देश में इसी प्रकार का धर्म-संचय होता है ? जिन्हें आवश्यकता नहीं, उनको बिठाकर आदर से भोजन कराया जाए, केवल इस आशा से कि परलोक में वे पुण्य-संचय का प्रमाण-पत्र देंगे, साक्षी देंगे, और इन्हें, जिन्हें पेट ने सता रखा है, जिनको भूख ने अधमरा बना दिया है, जिनकी आवश्यकता नंगी होकर वीभत्स नृत्य कर रही – वे मनुष्य, कुत्तों के साथ जूठी पत्तलों के लिए लड़ें, यही तो तुम्हारे धर्म का उदाहरण है।’
साहित्य के इतिहास की एक बड़ी भारी विसंगति यह देखी जा सकती है कि अपनी महती प्रतिभाओं को समुचित महत्त्व देते हुए भी, वह उनके कृतित्व का सर्वांगीण, सर्वपक्षीय, और सम्यक् मूल्यांकन नहीं कर पाता है। कभी किसी साहित्यकार के कुछ रचना-पक्ष इस तरह उभरकर आते हैं कि शेष पक्ष गौण या अनचीन्हे रह जाते हैं, या उनके सामने अपना सही परिप्रेक्ष्य नहीं खोज पाते हैं। जयशंकर प्रसाद के युग-प्रवत्र्तक व्यक्तित्व के साथ भी ऐसा ही घटित हुआ कि उनके कवि और नाटककार रूप के सामने उनका कथाकार अपनी पूरी पहचान नहीं करा पाया। उनके कहानीकार को फिर भी महत्त्व दिया गया और रोमांटिक भाव-धारा का उनका अलग ही ‘प्रसाद संस्थान’ – ‘प्रसाद स्कूल’ – कहानी में आज तक भी चला माना जाता रहा है। निर्मल वर्मा और कृष्णा सोबती तक उनकी वंश-परंपरा बतायी जाती रही। यह ओझल-सा हो गया कि जयशंकर प्रसाद के कथाकार के कितने गहरे सामाजिक सरोकार थे। प्रसाद जी की कहानी को तो गंभीरता से लिया भी गया किंतु इनके दोनों उपन्यासों – ‘कंकाल’ और ‘तितली’ को (अपूर्ण उपन्यास ‘इरावती’ की तो चर्चा क्या) बड़े चलताऊ ढंग से ‘धार्मिक संस्थाओं पर गहरे प्रहार’ और ‘हिंदू समाज की विकृतियों और अवैध संतानों के यथार्थ को उद्घाटित करने वाला’, ‘कंकाल’ तथा ‘तितली’ को ‘यथार्थ की पीठिका पर आदर्श की स्थापना अथवा प्रेमचंद की परंपरा का ‘आदर्शपरक’ उपन्यास कहकर कर्तव्य की इतिश्री मान ली गयी। वस्तुत: ध्यान से देखा जाए तो प्रसाद की औपन्यासिक चेतना बड़ी गहरी सामाजिक संलग्नता लिए हुए है। ‘कंकाल’ जिस तरह से सीधे-सीधे अपने समय के ज्वलंत प्रश्नों से टकराता है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि विराट सांस्कृतिक चेतना का यह कलाकार केवल अतीतजीवी नहीं था। उन्होंने अतीत को इतिहास की चिरंतन परंपरा के रूप में ग्रहण कर उसे वर्तमान के लिए प्रासंगिक बनाया था। उनका वर्तमान-बोध संस्कृति और दर्शन की वीथिकाओं से अपनी रोमानी धज में गुजरता है। कुछ वर्षों से साहित्य में ‘दो दुखियारों’ – स्त्री और दलित – का भरपूर शोर है, प्रसाद ‘कंकाल’ में गहरे जाकर स्त्राी-विमर्श में उतरते हैं। वे स्त्राी को समाज में अत्यंत उच्च, समाकृत स्थान की अधिकारिणी बताकर ही नहीं रुक जाते हैं अपितु उसे दलितोंं की पाँत में बिठा कर दोनों के साथ हो रहे सामाजिक अन्याय का प्रतिरोधी स्वर उपस्थित करते हैं – ”भगवान की भूमि भारत में स्त्रिायों पर तथा मनुष्यों को पतित बनाकर बड़ा अन्याय हो रहा है। करोड़ों मनुष्य जेलों में अभी पशु-जीवन बिता रहे हैं। स्त्रिायाँ विपथ पर जाने के लिए बाध्य की जाती हैं, तुमको उनका पक्ष लेना पड़ेगा। उठो !” उपन्यास में उनके स्वप्नों की संस्था ‘भारत संघ’ का घोषणा-पत्रा ”श्रेणीवाद, धार्मिक पवित्रातावाद, अभिजात्यवाद इत्यादि अनेक रूपों में फैले हुए सब देशों के भिन्न प्रकारों के जातिवाद का प्रतिरोध करता हुआ’, ‘श्रीराम ने शबरी का आतिथ्य स्वीकार किया था, श्रीकृष्ण ने दासी-पुत्र विदुर का आतिथ्य ग्रहण किया था, बुद्घदेव ने वेश्या के निमंत्रण की रक्षा की थी; इन घटनाओं को स्मरण करता हुआ भारत संघ मानवता के नाम पर सबको गले लगाता है।’ दलितों, भूख से बिलबिलाते आर्त गऱीबों को पत्तल से जूठन बीनते देख कर लेखक हिन्दू धर्म के उन ध्वजा-धारकों की अच्छी ख़्ाबर लेता है, जो इन भूखों को भोजन न करा, अघाए पंडितों को ससम्मान सुस्वादु भोजन खिलाकर पुण्य-अर्जन का काम करते हैं।
स्त्री-स्वातंत्र्य और विवाह संस्था के बेमानी होने के स्वर ने पिछली शती के उत्तराद्र्घ में ही ज़ोर पकड़ा है किंतु प्रसाद विवाह-संस्था की सार्थकता को प्रश्नांकित करते हुए स्वतंत्र प्रेम को जिस रूप में अपना समर्थन देते हैं, उस रूप में वे कदाचित् अपने समकालीन साहित्यकारों में सबसे आगे और अधिक क्रांतिकारी हैं। न केवल उनकी ‘धु्रवस्वामिनी’ (नाटक) धर्माधिकारी को धर्मशास्त्र के उन पृष्ठों को फाडऩे की बात कहती है अपितु ‘कंकाल’ में भी घंटी के संदर्भ में विजय मंत्रों के महत्त्व को नकारता हुआ, पूर्ण समर्पण और ‘स्वतंत्रा प्रेम की सत्ता को’ स्वीकारता है। आर्य समाज के प्रभाव से विधवा विवाह के जो प्रयत्न विभिन्न उपन्यासों में दिखाये गये हैं, उनसे आगे बढ़ कर प्रसाद का यह प्रेम-दर्शन एकदम आधुनिक स्त्री-स्वातंत्र्य के प्रकल्प और विमर्श के समकक्ष खड़ा है। इसीलिए घंटी और विजय का यह संदर्भ बिलकुल आज का बन जाता है। सुधारवाद से आगे जाकर यह क्रांतिकारी पग है। बहुत पहले प्रसाद ‘लिव-टुगेदर’ जीवन-शैली का समर्थन कर रहे हैं। विधवा विवाह का प्रसंग भी वे पूरी चिंता के साथ उठाकर उसका समुचित समाधान प्रस्तुत करते हैं, जो सहज अनुकरणीय बन जाता है। इसी प्रकार वेश्या को भी प्रसाद किसी आश्रम आदि में स्थापित कर कर्र्तव्य की इतिश्री नहीं मान लेते अपितु ‘मेरा विश्वास है कि उन्हें अवसर दिया जाए तो वे कुलवधुओं से किसी बात में कम न होतीं” – की धारणा रखते हैं।
प्रसाद सांस्कृतिक चेतना में जितने गहरे डूबे हैं, उससे यह अनुमानित करने की भूल का पर्याप्त अवकाश (स्पेस ) बनता है कि उन्होंने हिंदु, हिंदुत्व तथा धर्म के पारम्परिक रूप को प्रश्रय दिया होगा। स्थिति इसके बिलकुल विपरीत है। धर्म के छद्म, हिंदुत्व के मिथ्या दंभ, हिंदुओं के कदाचार की वे न केवल घोर निंदा ‘कंकाल’ में करते हैं, अपितु अपने पात्रों को इन सबके प्रतिरोध में खड़ा करते हैं- ”जब उस समाज का अधिकांश पददलित और दुर्दशाग्रस्त है, जब उसके अभिमान और गौरव की वस्तु धरापृष्ठ पर नहीं बची।” – ऐसे समय हिंदू होना वे ‘परम सौभाग्य’ की बात नहीं मानते। हिंदुओं की बद्घमूल और कूपमण्डूक दृष्टि का निषेध करते हुए वे तल्ख शब्दों में कहते हैं, ”हिंदुओं के पास निषेध के अतिरिक्त और भी कुछ है”, ”हिंदुओं को पाप को छोड़ पुण्य कहीं दिखलाई ही नहीं पड़ता।” हिंदुओं द्वारा समाज में फैलायी गयी छूतछात का वे खुला विरोध करते हैं। भिक्षाटन की प्रवृत्ति पर ‘कंकाल’ में कड़े शब्दों में यह कहा गया है- ”देखो यह बीसवीं सदी में तीन हज़ार बीøसीø का अभिनय।” पाप और पुण्य पर भी प्रसाद ‘कंकाल’ में वही बीज-विचार रखते हैं जिस कथ्य पर आगे चलकर भगवतीचरण वर्मा ने अपना अत्यंत लोकप्रिय उपन्यास ‘चित्रा लेखा’ लिखा – ”जो एक के यहां पाप है, वही दूसरे के लिए पुण्य है। ‘धर्म की व्याख्या जिस आधुनिकतापूर्ण दृष्टि से प्रसाद ‘कंकाल’ में करते हैं, वह तत्कालीन साहित्य में विरल है – ”धर्म मानवीय स्वभाव पर शासन करता है, न कर सके तो मनुष्य और पशु में भेद क्या रह जाए?” वे हिंदू धर्म के उस दकियानूसी दृष्टिकोण का तीव्र विरोध करते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित होने देने में बाधक बनता है – ”स्वतंत्रता और हिंदू धर्म – दोनों विरुद्घतावाची शब्द हैं।” प्रसाद मानते हैं कि व्यक्ति का आचरण ही उसके धर्म और जातीय श्रेष्ठता का मापक हो सकता है, इसीलिए वे ‘कंकाल’ में महर्षि वाल्मीकि को ‘सच्चे तपस्वी ब्राह्मण’ का गौरव देते हैं।
समाज और धर्म की अनेक ऐसी समस्याओं से ‘कंकाल’ में प्रसाद जूझते हैं जिनके समाधान के लिए हम वर्तमान में तरह-तरह के प्रयोग कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण स्कूल में बच्चों के पाठ्य-क्रम-निर्धारण का प्रश्न है। आज हम स्कूली पाठ्यक्रमों की नित नयी बहसों में उलझ रहे हैं किंतु मंगल के माध्यम से प्रसाद स्कूली पाठ्य-क्रम के विषय में यह दिशा देते हैं – ”मंगल ने स्वीकार किया कि वह पाठ्य-क्रम बदला जाएगा। सरल पाठों में बालकों के चरित्र, स्वास्थ्य और साधारण ज्ञान को विशेष सहायता देने का उपकरण जुटाया जाएगा। स्वावलम्बन का व्यावहारिक विषय निर्धारित होगा।” इतने समय पहले लिखे गए उपन्यास में ऐसी प्रखर वैचारिकता, ‘कंकाल’ को अपनी शैल्पिक न्यूनताओं में भी बहुत-बहुत समसामयिक और प्रासंगिक बनाते हुए अपने पुनर्पाठ की बाध्यता देती है। आज के सांस्कृतिक-सामाजिक कुहासे को छांटने के लिए बहुत कुछ दिशा देता है।