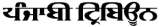अंधेरे का सैलाब
से.रा.यात्री
कहानी
इधर न जाने कुछ दिनों से क्या हो गया है-मैं रात को गणना करते हुए सोता हूं और जब भी मेरी आंखें खुलती हैं तो जाने अनजाने वही जोड़-घटाना फिर से दिल-दिमाग घेर लेता है। कभी-कभी सोचता हूं यह शायद जवानी ढलने का दौर तो नहीं है। नहीं, अभी मैं ढला कहां हूं-यह तो लम्बे कद की शख्सियतों के बौने बनते चले जाने के हालात हैं।
मैंने दीवाली के इस खास पर्व के लिए पहले से ही पांच सौ रुपए सहेजकर रख लिए थे। रुपए कम होते हैं तो चारों ओर के आमंत्रण देते आकर्षण आदमी को बहुत भरमाते हैं पर इस मामले में मैं थोड़ा खबरदार किस्म का जीव हूं। शायद यही वजह है कि खर्चे के मामले में भावुकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। कठिनाइयां आती हैं। मुझे मुंह चिढ़ाती हैं लेकिन मैं उन्हें दरगुजर करके दूसरी ओर मुंह फेर लेता हूं। इन रोजमर्रा की दुश्मनों से कौन लड़े?
पूरे पांच सौ का नोट मेरे खींसे में था। मैंने तय किया कि तीन सौ की मिठाई और दो सौ के पटाखे-फुलझड़ियां। दीगर सामान के लिए मैं अपनी पत्नी के खर्चे में बचाए हुए दो-चार सौ पर मुंह धोए बैठा था।
अगली शाम सारे घर में सोता पड़ जाने के बाद मैं मिठाई वगैरह लेकर घर में घुसा और आशा से बोला, “भली मानस! खयाल रहे-बच्चों को इसकी भनक न लगने देना।”
मुझे मेरी सतर्कता में कहीं पीछे धकेलते हुए आशा फुसफुसाई “कैसी बात करते हो? उनको इसकी हवा भी मिल गई तो परसों बड़ी दीवाली तक छंटाक भी नहीं बचेगी।”
पर मैं अगले दिन अपने फैसले पर अडिग नहीं रह पाया। सरगोशी में बोला, “भला यह भी कोई बात हुई कि जो चीज बच्चों के लिए ही ली गई है-उसी को उनसे छिपाकर रखा जाए।”
शायद आशा भी मेरी तरह ही सोच रही थी। वह बोली-“हां यह तो ठीक बात है। हम एक काम क्यों न करें-बच्चों को सारी चीजें दिखला दें जिससे उन्हें लगे कि हम लोगों के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इससे यह होगा कि हमारे दोनों बच्चे नदीदों की तरह दूसरों का सामान देखकर ललचाएंगे नहीं।”
और हमने यही किया। लेकिन इस नुमाइश का परिणाम कतई संतोषजनक नहीं निकला। बच्ची पटाखे छोड़ने की उसी वक्त जिद करने लगी। उधर से उनका ध्यान हटाने की सैकड़ों तदबीरों में से महज एक ही कामयाब हुई। मैंने रोशनदान में बैठे हुए कबूतर की टांग में रस्सी बांधकर उसका लपक-झपक करते हुए उड़ना दिखलाया तब कहीं जाकर वह पटाखाें का प्रकरण भुला पाई।
किसी तरह दिन गुजर गया। अगले दिन हम सब पैदल ही बाजार गए। जो भी खरीदा गया, उसे मैंने निर्विकार भाव से सहन किया। बेपनाह भीड़ से बच्चों को खींचते हुए मैं और आशा सब्जी मंडी से बाहर निकलने में बमुश्किल कामयाब हुए थे कि मेरे एक दूर के रिश्तेदार ‘डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज’ सामने पड़ गए। उनकी पत्नी, जिन्हें नौकर-चाकर, और बाहर से आने-जाने वाले मातहत अफसर सदा से ‘मेमसाब’ कहते चले आ रहे थे-हमें देखकर भरपूर मुस्कराईं और बोली, “कहिए! खरीददारी हो गई?”
हालांकि उनकी मुस्कान में रत्तीभर भी व्यंग्य नहीं था लेकिन उनकी जिज्ञासा ने मुझे अपने दोनों हाथों में लटके झोलों की याद दिला दी। बेखुदी में मैंने झोलों पर निगाह डाली। ये थैले साग-पात से ऊपर तक लबरेज थे और एक थैले से तो मूली के पत्ते खासी बेबाकी से बाहर झांक रहे थे। अपने से अलग हटकर मैंने स्वयं का जायजा लिया, तो मुझे अपनी बोसीदगी बहुत मनहूस लगी। मैं भीतर-ही-भीतर खीज उठा। गोया-उठाईगीरी करते पकड़ा गया होऊं।
मगर आशा और बच्चे हर तरह की तकलीफ से मुक्त थे। आशा के हाथ में महज किसी से उपहार में पाया हुआ एक वैनिटी बैग था, बच्चों के हाथों में गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां और मोमबत्तियों के पैकेट थे।
सबको मुस्कराते देखकर मैं भी खामखां बांछे खिलाने की कोशिश करने लगा पर मुस्कारने की कोशिश में मेरे चेहरे की नसें तनाव में खिंची जा रही थी। हाथों में लटके झोलों के अयाचित बोझ ने मुझ पर निरीहता का आक्रमण कर दिया था। मैं स्वंय को बुरी हालत में पकड़ा गया महसूस कर रहा था।
मैं डायरेक्टर महोदय और उनकी पत्नी से तुरन्त मुक्त होकर रिक्शा पकड़ने को उतावला हो रहा था लेकिन आशा मेम साहब को ‘मौसी जी’ कहकर बहुत आत्मीय स्तर पर बातें कर रही थी। हो सकता है, मेरी दुर्गति को सहज बनाने के लिए ही वह ऐसा कर रही हो। पर मैं अब किसी भी मुरव्वत के तहत वहां पैर पटकते घोड़े की तरह खड़ा नहीं रह सकता था। वैसे तो अक्टूबर के आखिरी दिन थे, मगर गर्मी का यह हाल था कि मेरी रीढ़ पर बहने वाला पसीना बेचैनी भरी सुरसुराहट पैदा कर रहा था। मुझे यह सोचकर चिढ़ हो रही थी कि इतने सुरुचि सम्पन्न आला अफसर की पत्नी बातों के रस में यह भी बिसरा बैठी थी कि वह सब्जी मंडी के मुहाने पर खड़ी साधारण स्तर की औरतों की मानिन्द बतिया रही थी।
शायद डायरेक्टर साहब मेरी असुविधा भांप गए। कहने लगे, “लगता है खरीद-फरोख्त तो आप कर ही चुके हैं। हमारे साथ ही चलिए। थोड़ी देर ठहरकर चले जाइयेगा।”
मैंने उनकी बात सुनकर एक झोला जमीन पर टिका दिया और अपनी थकान छिपाने के लिए तुरन्त ही उसे ऊपर उठा भी लिया।
मौसी जी के “हां….हां आशा चलो न चाय-वाय पीकर थोड़ी देर बाद चली जाना” की पेशकश पर आशा खुशी से सहमत हो गई और हम सब सब्जी मंडी के छोर पर खड़ी जीप की दिशा में बढ़ चले।
गोल सड़कों से बंगले का लम्बा चौड़ा लॉन पार करके बरामदे के नजदीक जाकर जीप खड़ी हो गई। सबसे पहले बच्चे कूदकर बाहर निकले। जब सब लोग उतर गए और ड्राइवर जीप पीछे लौटाने लगा तो मैं अपने थैले उतारने के लिए जीप की तरफ बढ़ने लगा।
डायरेक्टर साहब बोले, “आप रहने दीजिए, उन्हे ड्राइवर उठा लाएगा।” थैले जीप से उतारने की कतई जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें तो घर इसी वाहन से जाना था।
हम लोग अन्दर जाकर हॉल में बैठ गए। साहब की बड़ी बेटी फ्रिज से कुछ निकाल रही थी। हमें देखकर उसने अपने नए फैशन में कटे संवारे बाल एक ओर झटके और लापरवाही से अभिवादन करके भीतर चली गई। मैं थोड़ा सिकुड़कर कुर्सी में सिमट गया और दीवारों पर लगी विचित्र पेंटिग्स को देखने लगा जिन्हें सिर्फ बतौर दिखावटी वहां लगाया गया था। अखरोट की लकड़ी के तीन हंस थोड़े-थोड़े अंतर से टंगे थे जैसे वह एक-दूसरे का पीछा करते हुए उड़ान भर रहे हों।
मैंने स्वंय को आश्वासन दिया-इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। हमारे घर की दीवार भी तो नीले रंग से पुती है और हंस भी इसी तरतीब में टंगे हैं। बस यहां खासियत इतनी ही तो है कि यह साहब के बंगले में भव्य दिखाई पड़ते हैं। दूसरे के घरों की मामूली चीजें अगर किसी सम्पन्न के घर की हैं तो और भी भव्य लगती हैं। अब इन्हीं अनगढ़ पेंटिंग्स को लो, इनमें ऐसा क्या है? बच्चे अनजाने में उल्टे-सीधे रंग कागज पर पोत देते हैं तो अबूझ तस्वीरें नज़र आने लगती हैं।
मैं अभी दीवार पर ही अटका था कि साहब के मुलाकाती आने शुरू हो गए। हरेक के पीछे सिर पर फलों और मिठाइयों का झाबा लिए कोई नौकर नजर आ रहा था।
साहब ने अपने आसामियों से उठकर हाथ मिलाना शुरू कर दिया और तकल्लुफ दिखाते हुए कहने लगे-“अरे, इसकी क्या जरूरत थी!” और आगंतुक भी तोते की रटा हुआ वाक्य दोहराने लगे, “हें….हें, मैंने सोचा आपके दर्शन……!”
साहब इस ‘दर्शन’ की वास्तविकता से शायद युगों पहले परिचित हो चुके थे-इसलिए ‘दर्शन’ काे कठोर आदेश के नीचे कुचलते हुए रौब से चिल्लाए, “अरे कोई है?”
लड़खड़ाते कदमों से एक बूढ़ा हाजिर हुआ तो कड़ककर बोले, “पानी और पान लाओ।”
आने वाले सहमते हुए से मिनट दो मिनट कुर्सी के अग्रभाग पर टिकते और तश्तरी से पान उठाते हुए उठकर खड़े हो जाते। वह जाते-जाते खींसे निपोरते हुए चेहरे पर कृतज्ञता का भाव लाकर कहते, “अच्छा, तो आज्ञा दीजिए।” साहब रस्मी तौर पर कहते, “अच्छा! जाइएगा।” और फिर हाथ की दो ऊंगलियां आगंतुक की ओर बढ़ा देते जिन्हे वह झुककर छूते हुए आभार व्यक्त करते हुए हॉल से बाहर हो जाता।
चूंकि आशा और बच्चे मेम साब के साथ बंगले के भीतरी भाग में चले गए थे इसलिए मैं साहब और उनके मुलाकातियों के बीच में बुरा फंस गया था। आने वालों की दीनहीन मुद्राओं को दिलचस्पी या गैरदिलचस्पी से देखते रहने के अलावा मैं और कर भी क्या सकता था?
साहब के बंगले के बाहर पों पों की आवाज से मैं जान जाता था कि कोई लम्बी या छोटी गाड़ी और आकर ठहरी है और यह सिलसिला जल्दी खत्म होने वाला भी नहीं लगता था। आने वालों में नगर के अत्यन्त सम्पन्न उद्योगपति थे जो ‘डायरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज’ के पुरखों तक को खरीदकर नीलाम कर सकते थे। पर वह जानते थे कि अफसर से उलझने में उनकी कोई शान नहीं थी क्योंकि खीसे निपोरने की सुई तो दुधारी तलवार को भी अंगूठा दिखा सकती थी।
मेरे लिए वार्तालाप का प्रसंग तो दूर तक नहीं था। चूंकि मैं सपरिवार साहब की जीप में बैठकर आया था इसलिए स्वयं उनका कृपाभाजन था। मैं जानता था कि उपकृत का चुप रहना ही बेहतर है-क्योंकि कृतज्ञताज्ञापन की मूर्खता करके वह जो कुछ कहता है अवांछित भावुकता का प्रदर्शन ही होता है और कहने वाले को और भी अहमक बना देता है।
फलों और मिठाईयों के साथ सलाम ठोंकने वालों का तांता बंध गया था। साहब इस सबसे बोर दिखाई पड़ रहे थे या फिर उन्हें मुझसे बातें न कर पाने पर खेद हो रहा था। नौकर से बोले, “वत्स बाबू के लिए कुछ लाओ।”
कुछ ही देर बाद चार बड़ी-बड़ी प्लेटों में बहुत-सी मिठाईया, फल और दीगर लवाजमात मेरे सामने आ गए। मैं अकेला आदमी और इतना सरंजाम। मैं कौतुक से हंस पड़ा, तो साहब मेरी हंसी में योग देते हुए बोले , ‘खाइए ना’ परसों लखनऊ से आते वक्त ‘चौधरी’ के यहां से लेता आया था। यह आपका शेयर है।
साहब के चेहरे पर अनोखा संतोष झलक रहा था। मानो उनकी लखनऊ से लाई हुई मिठाई सही पात्र के सामने पहुंच गई हो। मेरा संकोच देखकर बोले, “मैं जानता हूं-आप ‘राइटर’ लोग मिठाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। आप लोग ठहरे पीने-पिलाने वाले, खाने के नाम पर तो राइटर लोग एक तरह से माफीनामा ही होते हैं। फिर वह हंसते हुए बोले, “मोहन मीकिंज” के यहां से कुछ बढ़िया माल आया है-कहिए तो दो-एक बोतलें रखवा दूं? लेकिन कहीं मुझ पर ही कोई कहानी न लिख मारिएगा।”
मैंने उनकी दिल्लगी पर एक पुरजोर खोखला ठहाका लगाया। साहब की बतकही सुनने वाले एक सज्जन जो उठकर जाने की फिराक में थे। मुझे घूरकर देखने लगे और मेरे कुरते की उड़ी हुई रंगत देखकर बोले-“क्या सिरीमान जी अफसाने लिखते हैं?”
साहब ने उनकी बोसीदा जिज्ञासा को कोई भाव नहीं दिया और बेदिली से टालनेवाले लहजे में बोले “हां साहब, इनकी क्या पूछते हो।”
“तभी तो…..! कहकर वह सज्जन उठ खड़े हुए। पता नही ‘तभी तो…..’ से उनका क्या अभिप्राय था। हो सकता है वह कहना चाहते हों, “तभी तो अफसाना लिखने वाला आदमी इतना फटीचर होता है।”
साहब का आग्रह देखकर मैंने प्लेट से मिठाई का एक टुकड़ा उठा लिया और चलने की इजाजत चाहने लगा। साहब के दिल में लेखक को उपकृत करने का इरादा शायद बहुत गहरा था। इसलिए उन्होंने दूसरे मुलाकातियों की तरह मुझे टरकाने की कोशिश नहीं की बल्कि हंसकर बोले-“अरे साहब ऐसी भी क्या जल्दी है? चले जाना, अभी तो आपकी श्रीमती जी भी अन्दर ही हैं। “योर फैमिली इज हीयर व्हाई डु यू मेक सो हरी?”
काफी देर बाद हम लोग साहब की जीप में बैठकर उनके बंगले से बाहर निकले तो हमने देखा आसपास के अफसरों की कोठियों के बाहर बहुत सी कारें खड़ी हैं और उनमें मिठाइयों के डिब्बे और टोकरियां भरी हुई हैं। यह बस्ती सरकारी अमलों की थीं। डायरेक्टर साहब की बगल में जज साहब, एसडीएम और इन्कम टैक्स कमिश्नर के बंगले रौनक अफरोज थे। एक-एक बंगला हजारों गज जमीन घेरे हुए था। दीवाली के त्यौहार से हफ्तों पहले से इस बस्ती में कारों और सरकारी जीपों का तांता लगा रहता है। दीवाली का मुबारकबाद लम्बे खुमार की तरह बरकरार रहता है। पता नहीं अफसरान इतनी मिठाई और दीगर उपहारों का क्या करते हैं? मिठाई और मेवा का यह अम्बार देखकर अजीब सी बात दिमाग में आती है कि शायद अफसर लोग फालतू मिठाई हलवाइयों की दुकानों पर वापस भिजवाकर रुपए खरे कर लेते होंगे। मगर ऐसा बकवासी खयाल मेरे जैसे मामूली आदमी का बेजा कयास ही हो सकता है। साहबों की खुशहाली देखकर कौन सोच सकता है कि वह मिठाई फरोख्त करेंगे। मैं हर साल यही सोच कर रह जाता हूं कि अगले वर्ष इस रहस्य की गुत्थी जरूर सुलझाऊंगा। पर साथ ही यह खयाल भी आ जाता है कि आजादी से पहले अंग्रेज साहबान के यहां भी तो बड़े दिन पर अनाप-शनाप डालियां आया करती थीं।
यकायक मेरे बेटे का आश्चर्यजनक वाक्य मेेरे कानों से टकराया “पापा कितने सारे डिब्बे?” वह कारों की ओर संकेत कर रहा था। मैंने हड़बड़ाकर बच्चे की बात पर गौर किया। मैं अपनी बगल में जीप चलाते ड्राइवर का चेहरा देखने लगा। पर उसके चेहरे पर बच्चे की बात की कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी-गोया उसने कुछ सुना ही नहीं हो।
ड्राइवर का चेहरा मुझे कुछ सख्त और तना हुआ सा लगा। हो सकता है वह ऊब अयाचित लोगों को ढोने की बेगार से जुड़ी हुई हो। मेरे पांवों के पास सामान के थैले रखे थे। उन झोलों को देखकर मुझे अजीब सी हया महसूस हुई। साहब के सुसज्जित ड्रांइग रूम में यह कैसे बेहूदा लग रहे थे-जैसे फर्स्ट क्लास के डिब्बे में कोई गठरी-मुठरी वाला देहाती घुस आया हो। चूंकि मेरा अपना लिबास भी उन थैलों से जुड़ता था, इसलिए मैंने स्वयं को भी थैलोें की तरह ही साहब के उस आलीशान कक्ष में अवांछित महसूस किया था।
दोनों बच्चे आपस में बतिया रहे थे। राजीव कह रहा था, “नीता जरा देर में आण्टी जी के घर में कितने डिब्बे आ गए। सौ से भी ज्यादा थे ना?”
नीता उसके अज्ञान पर हंसी, ‘हट पग्गल, तैंने क्या डिब्बों की गिनती की थी?”
“क्यों सारी अलमारी तो भर गई थीं।” आगे की स्थिति शायद राजीव की समझ में नहीं आई। वह आशा से पूछने लगा, ‘मम्मी नरेश दादा और नीरु जीजी इतनी सारी मिठाई का क्या करेेंगे?”
नीता ने सयाने की तरह हाथ हिलाकर कहा ‘मम्मी इसे इतना भी पता नहीं- खाएंगे और क्या करेंगे?”
आशा ने दोनों बच्चों को हल्के से झिड़क दिया। दोनों सहमकर चुप हो गए। बच्चों का मिठाई को लेकर बातें करना मेरे मन में त्रिशूल की तरह गड़ रहा था। इन कम्बख्तों को आखिर कितनी मिठाई चाहिए?
जितनी मिठाई लेकर मैं पिछली रात घर में घुसा था वह तो शायद इन दोनों से कई दिनों तक भी न खाई जा सके-फिर ये मिठाई का जिक्र इतने लालच से क्यों कर रहे हैं? डायरेक्टर साहब के घर में बैठकर उनकी जहनियत को एकदम घटिया और अतिरिक्त लालची खयाल कर रहा था। लम्पट ने हराम का माल वसूल करना ही अपना धंधा बना रखा है। लेकिन मेरे बच्चे क्या उसी जहनियत के शिकार नहीं हो गए थे?
मेरे सिर में अजीब तरह की घूं घूं बजने लगी। मैंने सिर को झटका देकर रुग्णता से बचने की कोशिश की। पर मैं यह सोचने से नहीं बच सका कि तंगदस्ती और जिस विपन्नता को मैं झूठे गर्व से सिर पर उठाए घूम रहा हूं वह किसी वास्तविक गौरव की स्थिति नहीं है। टुच्चेपन को नकारने के बजाय मेरे बच्चे अनजाने ही उसी गर्त में जा गिरे थे।
जीप मेरे मकान के सामने जाकर ठहर गई। ड्राइवर मेरा मकान जानता था। पहले भी एक दो बार छोड़कर जा चुका था। जीप से जब सब उतर गए तो मैं थैले उठाने के लिए आगे बढ़ा। ड्राइवर ने थैले मुझे नहीं उठाने दिए बल्कि आदर सहित बोला, “साहब, आप ऊपर चलिए झोले पहुंच जाएंगे।”
रोजमर्रा की तरह सांझ आई और उजास कुछ वक्त के लिए एक खास बिन्दु पर ठहर गई। अंधेरा घिरने के साथ चारों तरफ गहमागहमी बढ़ने लगी। आस पड़ोस में दीवाली का उल्लास पटाखों और फुलझडियों की चिंगारियों के रूप में प्रकट होने लगा।
मैंने जानबुझकर अंधकार घिरने दिया। मैंने सोचा देर से दिए जलाने से वह रात को देर तक जलेंगे और दूसरों के मुकाबले हमारे दीयों की रोशनी ज्यादा देर तक ठहरी रहेगी।
दोनों बच्चे बार-बार आकर पूछने लगे “पापा अब दिए उलटकर सीधे कर दें-उनका पानी सूख गया है।” लेकिन मैंने उन्हे आसपास की रोशनी और आकाश की ऊचांइयों में सूं सूं सर्र सर्र करके छूटने वाली आतिशबाजी दिखलाकर बहला दिया।
होते होते रात पूरी तरह घिर आई और बहुत सी मुंडेरों के दीपक बुझने भी लगे। “अब दीये जलाने का सही वक्त आ गया” कहते हुए मैंने एलान किया। मैंने बच्चों से कहा “चलो दीयों की पूरी कतार उलटकर सीधी करो। मैं लक्ष्मी पूजन करने बैठा तो बच्चों ने दीपक जलाने का कोई आग्रह नहीं किया।
सब दीए जला दिए गए। मैंने जलते दीपकों पर अक्षत फेंकने को उन्हें खीलें दी तो उन्होंने उन्हें अपने आसपास ही बिखरा दिया। आशा ने जलते दीपकों की ओर खाना बनाते बनाते दूर से ही हाथ जोड़ दिये।
दोंनों बच्चे ऊंघने लगे थे मैंने उन्हें हिलाडुलाकर मिठाई के छोटे छोटे टुकड़े खाने को दिए और मैं उन्हें वहीं छोड़कर घर के भीतर बाहर और छत की मुंडेरों पर दीये रखने चला गया। लौटकर मैंने देखा राजीव वहीं लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों के सामने फर्श पर गुडीमुडी होकर सोया पड़ा था और पसीजी हुई मिठाई का टुकड़ा उसकी मुट्ठी में जकड़ा हुआ था।
नीता मुझे वहां नजर नहीं आई। एकाएक मुझे फूलझड़ी और पटाखों की याद आई तो कमरे की अलमारी से उन्हें उठाने के लिए लपका। नीता फुलझड़ी का पैकेट हाथ में पकड़े पलंग की पाटी पर सिर टिकाए खड़े-खड़े ही सो रही थी। नए कपड़ों में सजीबजी उस गुड़िया को मैंने लाख जगाने की कोशिश की मगर उसकी नींद नहीं टूटी। एक बार उसने आंखें जरूर मुलमुलाई मगर तुरन्त ही बंद कर ली। फुलझड़ियों का पैकेट उसकी पकड़ से छूटकर फर्श पर गिर गया।
पूरी बस्ती में धूं धां सर्र सर्र की गूंज से कानों के पर्दे फटे जाते थे और ऊपर आकाश में बहुवर्णी प्रकाश की जगमगाहट फैल रही थी। लेकिन उन निरीह बच्चों के लिए संरक्षित मिठाई और पटाखे-फुलझडियां अब उनके किसी काम के नहीं थे।
मेरे मुंह से एक लम्बी सांस बेसाख्ता निकल गई और न जाने कितनी दूर तक अंधेरे का सैलाब छोड़ती चली गई।