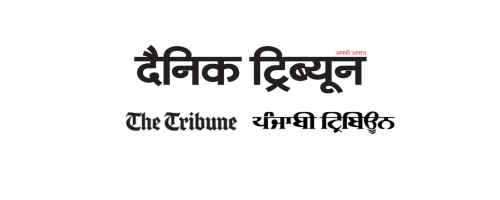अरुण नैथानी
काव्य की विभिन्न विधाओं में दखल रखने वाले माधव कौशिक पिछले दो दशक से अधिक समय से चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के विभिन्न पदों को सुशोभित करते रहे हैं। अब उन पर बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। एक-दो नहीं बल्कि चौबीस भारतीय भाषाओं की संरक्षक संस्था राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद के गुरुतर दायित्व की। जिसके लिये हाल ही में वे चयनित हुए हैं। वैसे राष्ट्रीय साहित्य अकादमी में सचिव व उपाध्यक्ष की भूमिका वे पहले ही निभा चुके हैं। वे स्वीकारते रहे हैं कि दैनिक ट्रिब्यून से उनका करीब तीन दशक से ज्यादा पुराना व गहरा नाता रहा है। जिसमें वे न केवल काव्य की विभिन्न विधाओं में लगातार लिखते रहे बल्कि व्यंग्य के कॉलम में भी उनकी भागीदारी रही है। फिलहाल वे चडीगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी हैं। अकादमी के दफ्तर में उनकी ताजपोशी, पद की चुनौती और भावी योजनाओं को लेकर विस्तृत बातचीत हुई। वार्ता के कुछ चुनींदा अंश।
साहित्यिक पृष्ठभूमि और सृजन यात्रा
साहित्य की दुनिया में आने का कारण जहां दुनिया-जहान के प्रति मेरी गहरी संवेदनशीलता थी, वहीं घर का ऊर्जावान माहौल। पिताजी का साहित्य से खासा लगाव था। मेरा मानना है कि हमारा व्यक्तित्व परिवार व परिवेश की उपज होता है। सृजन का पहला मूल स्रोत वहीं से ग्रहण करता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि साहित्यिक थी। पिता शिक्षक थे तथा उर्दू व पर्शियन के विद्वान थे। खूब किताबें व पत्रिकाएं आती थीं। मां स्वाध्याय करती थीं। वे हमें खूब कहानियां सुनाती थीं। उस दौर में भिवानी का जो वातावरण था वह भी बहुत साहित्यिक था। कालेज में पढ़ाने वाले गुरुवर भी साहित्यकार थे, मसलन सतनाम खुमार, उदयभानु हंस जैसे शिक्षक थे। भिवानी की साहित्यिक संस्था ‘अदबी संगम’ ने उस माहौल में बहुत प्रभावित किया। वर्ष 1980 में चंडीगढ़ आने के बाद उस समय जो वातावरण मिला, उसका मेरी सृजन यात्रा में खास योगदान रहा है। दैनिक ट्रिब्यून में बहुत साल तक मेरा कॉलम चला। व्यंग्य के एक कॉलम ‘सागर में गागर’ के लिये बहुत साल व्यंग्य लिखे। तब ‘मध्या’ कॉलम रमेश नैयर जी देखते थे, उसमें खूब लिखा। ग़ज़ल के लिये स्पेशल कॉलम रहा। मेरे सृजन के लिये नर्सरी का काम किया दैनिक ट्रिब्यून ने। उसके बाद जनसत्ता आया तो एक कॉलम चला ‘ग़ज़लियात’, पुष्प कुमार ‘पुष्प’ देखते थे साहित्य के पेज। ये अखबार मेरी सृजन की पृष्ठभूमि में रहे। फिर तमाम राष्ट्रीय पत्रिकाओं धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान,सारिका, कादंबनी आदि में लगातार रचनाएं प्रकाशित होती रहीं। वर्ष 1986 में पहला काव्य संग्रह ‘आईनों के शहर में’ आया। डाॅ. यश गुलाटी की साहित्यिक संस्था साक्षी के साथ काफी समय तक जुड़ा रहा। मेरी सृजन यात्रा में चंडीगढ़ के साहित्यिक माहौल ने बड़ा योगदान दिया।
दिलकश ग़ज़ल का रचना लोक
जहां तक काव्य, विशेष रूप से ग़ज़ल विधा को चुनने की बात है, एक तो घर में उर्दू की पृष्ठभूमि सहज रूप से प्राप्त हुई। काव्य का छंद शास्त्र घर में सीखने का मौका मिला तो आगे सृजन में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैंने साहित्य की हर विधा में लिखा। कविता की हर विधा में लिखा। नवगीत, मुक्तक, छंद आदि। ‘सुनो राधिका’ व ‘लौट आओ पार्थ’ रचनाएं मुक्त छंद में हैं। यह बात ठीक है कि ग़ज़लकार के रूप में मान्यता ज्यादा मिली। ग़ज़ल संग्रह ही डेढ़ दर्जन से ज्यादा प्रकाशित हुए। एक कारण और भी है कि ग़ज़ल का छंद इतना प्रभावशाली कि दो मिसरों में अपनी बात लोगों तक पहुंचा देता है। इसकी लोकप्रियता की वजह सहजता से दिलों को छूना है। उसकी वजह से ज्यादा प्रिय रहा।
पैशन से प्रोफेशन का तालमेल
मैं यह बात नहीं मानता कि यदि सरकारी सेवा में न जाता तो विपुल साहित्य रच पाता। इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। मैंने पहले जस्टिस सुरेंद्र सिंह की किताब में इंटरव्यू में लिखा भी था। पिताश्री का सुझाव रहा था कि हर लेखक को काम करना चाहिए। यदि व्यक्ति नौकरी न करे तो पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह के लिये समझौते करने पड़ते हैं। निस्संदेह समझौते करने वाला रचनाकार अच्छा साहित्य नहीं रच सकता। रचनाकार को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। मेरे साथ अच्छी बात यह रही कि मेरा प्रोफेशन व पैशन एक ही रहा, क्योंकि राजभाषा विभाग में काम करते हुए विभागीय पत्रिका ‘सुंगधा’ का संपादन किया। वर्ष 1995 से साहित्य अकादमी से जुड़ गया। सचिव, उपाध्यक्ष व अध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वहन किया। जितनी भी नौकरियां की, साहित्यिक संस्थानों में कीं और उनकी पत्रिका व सृजन कार्यों का संपादन किया। नौकरी मेरे लिये एक तरह वरदान साबित हुई।
अन्यत्र भी भारतीय साहित्य के अध्येता
जहां तक अकादमी के दायित्वों के लिये विदेश यात्राओं के दौरान तुलनात्मक सृजन के अनुभवों की बात है तो यह सुखद अनुभव रहा। वर्ष 2008 से 2012 तक हिंदी साहित्य परामर्श मंडल का सदस्य व संयोजक रहा। उसके बाद वर्ष 2018 से 2022 तक राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का उपाध्यक्ष रहा। इन वर्षों में मैंने शारजाह, आबूधाबी, जोहान्सबर्ग, मैक्सिको में विश्व लेखक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। मेरा अनुभव ये रहा कि भारतीय साहित्य पूरी दुनिया में पूरे चाव से पढ़ा जाता है। उसकी प्रतिष्ठा सर्वत्र है। विशेष तौर पर रवींद्रनाथ टेगौर व प्रेमचंद जी की, दो ऐसे रचनाकार हैं कि जिन्हें हर देश में सम्मान से पढ़ा जाता है। लेकिन भारतीय साहित्य का जितना अनुवाद अंग्रेजी व अन्य विदेशी भाषाओं में होना चाहिए, उस दृष्टि से काम नहीं हुआ।
अनुवाद से सार्थक सेतु का निर्माण
कैसा लगता है जब खंड व्यंग्य ‘सुनो राधिका’ का अनुवाद संस्कृत, उड़िया, अंग्रेजी,पंजाबी व अन्य भाषाओं में हुआ, आप इसको किस तरह से देखते हैं, के सवाल पर माधव कौशिक की प्रतिक्रिया थी कि निस्संदेह, अनुवाद के माध्यम से भारतीय साहित्य की एकात्मकता सिद्ध होती है। जितने भी अनुवाद हुए मेरी रचनाओं व दूसरे लोगों के, वे हमारी भाषाओं की आधारभूमि तैयार करते हैं। निस्संदेह, भारतीय भाषाओं में खूब अनुवाद होना चाहिए। तभी देश की 24 भाषाओं में रचनाओं के आवागमन हेतु सार्थक सेतु का निर्माण होगा। साहित्य अकादमी गत सत्तर सालों से इस काम को बहुत प्रभावशाली तरीके से कर रही है। जिस भी कृति को अकादमी पुरस्कार मिलता है,उसका 24 अन्य भाषाओं में अनुवाद होता है।
प्रतिष्ठा के साथ पारदर्शिता भी
अभी आपने पुरस्कारों का जिक्र किया, निस्संदेह अकादमी के पुरस्कार की बड़ी प्रतिष्ठा है, क्या करेंगे साख व पारदर्शिता के लिये? इस पर जवाब था कि साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में चार पुरस्कार प्रदान करती है। एक श्रेष्ठ कृति, दूसरा बाल साहित्य, तीसरा अनुवाद और चौथा युवा पुरस्कार होता है। इसके अलावा एक भाषा सम्मान भी है। ये पुरस्कार उन भाषाओं में दिया जाता है, जिनकी लिपि नहीं है। इन पुरस्कार का चयन एक विश्वसनीय प्रक्रिया के अधीन होता है। एक पुस्तक लगभग 65 विद्वानों के हाथ से गुजरती है। साहित्य अकादमी के पुरस्कार की प्रतिष्ठा बड़ी है, भले ही राशि एक लाख रुपये ही है।
चंडीगढ़ का उदार-विशाल साहित्यिक फलक
अपनी सृजन यात्रा में चंडीगढ़ की साहित्यिक संस्थाओं कितना योगदान मानते हैं? इस विषय पर विचार थे- जैसे मैंने बताया कि परिवेश का अवदान किसी भी रचनाकार के लिये महत्वपूर्ण होता है। चंडीगढ़ का योगदान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह भारत का एक शहर है जिसमें भाषायी दुर्भावना नहीं है। हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी व उर्दू यानी चार भाषाओं के लेखक एक साथ सृजन में रत हैं। दूसरा ये भी है कि इस सोच के चलते चंडीगढ़ का साहित्यिक व सांस्कृतिक महत्व पिछले 25 वर्ष बहुत अधिक विकसित हुआ। जिसका फलक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला है। निश्चित रूप से ऐसे माहौल में रहने और काम करने का आनन्द भी अलग है और एक तरह से इसे सफलता की नींव भी कह सकते हैं।
संतोष के साथ दायित्व का बोध
साहित्य अकादमी की जिस कुर्सी पर आप विराजमान हुए, उसकी शुरुआत पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व डॉ. राधाकृष्णन आदि दिग्गजों से होती है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं? इस मामले में भावनाएं व्यक्त की – मेरा मानना है कि जो भी रचनाकार बहुत नीचे से ऊपर जाता है, उसमें हर्ष का अतिरेक ज्यादा नहीं होता है, जिम्मेदारी अधिक होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं भी ऐसा ही अनुभव कर रहा हूं। यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। कुल 24 भाषाओं के रचनाकार एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। एक तरह से सभी भाषाओं के प्रति और उनके साहित्य की जिम्मेदारी है। एक बात जरूर है कि संतोष का भाव है। कुछ तो काम किया। चुनाव के बाद इस जीत का श्रेय सभी भारतीय भाषाओं के लेखकों को दिया।
साहित्यिक गतिविधियों को संबल
हरियाणा से इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले आप पहले साहित्यकार हैं। चंडीगढ़ का आप पर विशेष अधिकार है। इनके लिये कुछ खास सोचा है? तो बताया कि निश्चित रूप से प्रयास होगा। कोशिश होगी कि चंडीगढ़ और हरियाणा के विभिन्न शहरों में राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के अधिक आयोजन हों। साथ ही इस पूरे अंचल के विस्मृत साहित्यकारों को सम्मान पूर्वक याद किया जाये।
किताबों से भरा एकाकीपन का शून्य
आपने एक साक्षात्कार में जिक्र किया था कि मां के निधन के बाद अकेलापन दूर करने के लिये मैंने किताबों में डूब जाना पसंद किया और आज सौ पेज पढ़े बिना आपको नींद नहीं आती? वाकई, ये सच है। जब मैं फर्स्ट ईअर में था तो मां का निधन हो गया। विकट समय था। तब उस अकेलेपन को दूर करने मैं लगभग पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठा रहता था। बीए तक आते-आते सारे हिंदी व अंग्रेजी के क्लासिक पढ़ लिये थे। यह एक ऐसा हादसा था जिसने मुझे पुस्तकों के नजदीक ला खड़ा किया। संभवत: अच्छा पाठक लेखन की पृष्ठभूमि में काम आया।
तकनीक के दौर की नई पीढ़ी
आपने एजी पंजाब में ज्वाइन करने से पहले भिवानी में अध्यापन भी किया। आज पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले अभिजात्य वर्ग व नेताओं के बच्चे भारतीय साहित्य से कट रहे हैं। विदेशी भाषा व उसके सृजनकार उनके नायक हैं। वे भारतीय साहित्य से कटेंगे तो भारतीय संस्कृति से भी कटेंगे? इस पर विचार थे- निस्संदेह, पिछले कुछ वर्षों में ऐसा कुछ हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कह सकते हैं पिछले कुछ दशकों में साहित्य के प्रति नई पीढ़ी का रुझान कम हुआ। लेकिन नई तकनीक और भूमंडलीकरण की प्रवृत्तियों ने हमारे साहित्य को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। अब मोबाइल में पूरी दुनिया का साहित्य मौजूद है। पढ़ना चाहें तो पूरा पुस्तकालय व्यक्ति की जेब में मौजूद है। दूसरा कारण अंग्रेजी के वर्चस्व का है। उसने भारतीय भाषाओं को थोड़ा हाशिये पर धकेला जरूर है लेकिन अब स्थिति निरंतर बदलाव की ओर है। नई शिक्षा नीति के अच्छे परिणाम जल्दी हमारे सामने आएंगे।
भारतीय भाषाओं में रोजगार
कहीं अंग्रेजी की ओर रुझान रोजगार की मजबूरी के रूप में देखते हैं, के विषय पर उत्तर था- अब धीरे-धीरे स्थिति बदल रही है। आज हिंदी व भारतीय भाषाओं में रोजगार सृजित हो रहे हैं। समाचार पत्र व मीडिया की अन्य धाराओं में अधिक अवसर मिल रहे हैं। इनके अतिरिक्त मीडिया के अलावा पर्यटन आदि अन्य बहुत से क्षेत्रों में हिंदी व भारतीय भाषाओं में नये अवसर पैदा हो रहे हैं।
सोशल मीडिया का अनुकूल प्रभाव
आपको लगता है कि सोशल मीडिया के वर्चस्व से धीर-गंभीर साहित्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है? मेरा मानना है कि सोशल मीडिया के दौर में साहित्य की परिधि का विस्तार ही हुआ। पुस्तकें शेल्फ के बजाय अब किंडल संस्करण में खूब मिल रही हैं। पुस्तकों का विक्रय दस गुना बढ़ा है। साहित्य अकादमी ने पिछले वित्त वर्ष में 20 करोड़ रुपये की किताबें बेची हैं। ऊपरी तौर पर ऐसा जरूर लगता है कि स्थिति ठीक नहीं है। जबकि स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत ही है।
लेखन की दुनिया में उम्मीद के अंकुर
ज्यादा साहित्य स्वांत सुखाय के लिये लिखा जा रहा है, के प्रचलित संदेह के बावजूद मेरा मानना है कि थोड़ी सी अराजक स्थितियों के बावजूद अब भी भारतीय भाषाओं में गंभीर लेखन हो रहा। साहित्य अकादमी के दो आयोजन महत्वपूर्ण हैं, एक प्रकाशन ‘नवांकुर’ के माध्यम से और दूसरा युवा साहित्य के माध्यम से। इसके अंतर्गत जो नई पुस्तकें प्रकाशन के लिये आती हैं, उसे देखकर लगता है कि आज की युवा पीढ़ी बहुत अधिक जागरूक व प्रतिबद्ध है। समय की नब्ज को पकड़कर चलने वाली है। युवाओं ने भाषा को नई ऊर्जा प्रदान की है। वहीं कथ्य को भी विस्तार दिया है।
सतत परिवर्तनशीलता
मौजूदा समय में साहित्य के मानकों की परिभाषा क्या हो, का सवाल अहम है। दरअसल, साहित्य सृजन में जो स्थितियां हैं, वे समय के अनुरूप हमेशा परिवर्तनशील होती हैं। हम भोजपत्र से डिजिटल युग तक आए हैं। हर तकनीक के साथ साहित्य की विधाओं का रूपाकार बदलता है। भाषा के सरोकार बदलते हैं। सामाजिक सरोकार भी बदलते हैं। इन सब बदलावों के बीच गंभीर साहित्य पहले भी था और आज भी। सदा से साहित्य समाज का मार्गदर्शन करता रहा है। समाज को प्रतबिंबित भी करता है। मैं मानकर चलता हूं कि सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य का भविष्य उज्ज्वल है। विश्व स्तरीय साहित्य के समकक्ष है। विश्व साहित्य में गरिमापूर्ण स्थान प्राप्त करने लगा है।
चित्रांकन : संदीप जोशी