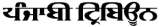सतत जागरूकता से बचेगी जनतंत्र की गरिमा
राजनेताओं को यह अहसास कराया ही जाना चाहिए कि जनता को अपनी मुट्ठी में समझने की उनकी प्रवृत्ति देश के जागरूक मतदाता को स्वीकार नहीं है। जनतांत्रिक मूल्यों- मर्यादाओं का तकाज़ा है कि नेता अपनी सीमाएं समझें और जनता अपनी...
राजनेताओं को यह अहसास कराया ही जाना चाहिए कि जनता को अपनी मुट्ठी में समझने की उनकी प्रवृत्ति देश के जागरूक मतदाता को स्वीकार नहीं है। जनतांत्रिक मूल्यों- मर्यादाओं का तकाज़ा है कि नेता अपनी सीमाएं समझें और जनता अपनी शक्ति को पहचाने।
बिहार के चुनाव परिणाम पर ‘रेवड़ी’ का क्या और कितना असर पड़ता है यह तो मतपत्रों की गणना के बाद ही पता चलेगा, पर यह एक खुला रहस्य है कि हमारे राजनीतिक दल यह मानकर चलते हैं कि देश का मतदाता रेवड़ियों से रिझाया जा सकता है। देखा जाये तो एक तरह से यह देश के मतदाता का अपमान ही है कि उसके बारे में ऐसी धारणा बन रही है। ऐसा नहीं है कि यह स्थिति अचानक बन गयी है, अर्से से हमारे राजनीतिक दल इस रेवड़ी- संस्कृति का सहारा लेकर चुनाव जीतने का प्रयास करते रहे हैं। शुरुआती दौर में यह काम चोरी- छिपे ढंग से होता था। मतदान से पहले की रात को न जाने क्या-क्या बंटता था मतदाताओं के बीच। अब भी ऐसा होता है, पर अब और भी रास्ते अपना लिये गये हैं, मतदाताओं को ‘खरीदने’ के– उदाहरण के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण के नाम पर बिहार के ‘सुशासन बाबू’ ने राज्य की लगभग डेढ़ करोड़ महिलाओं को दस-दस हज़ार रुपये नकद बांट दिये। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी ऐसे प्रयोग हो चुके हैं।
यही सब देखते हुए यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या खैरात बांटकर चुनाव जीते जा सकते हैं? भले ही कुछ राजनीतिक-विश्लेषक यह कहते रहें कि ऐसा नहीं हो सकता, पर इस धारणा से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे राजनेता यही मानते हैं कि खैरात काम आती है। अब तो हमारे सत्ताशीर्ष भी यह मान चुके लगते हैं कि चुनाव के अवसर पर रेवड़ियां बांटना ग़लत नहीं है!
बात सिर्फ रेवड़ी-संस्कृति तक सीमित नहीं है। चुनाव जीतने के लिए जिस तरह जाति और धर्म का सहारा लिया जा रहा है, वह एक तरह से हमारे लोकतंत्र का मज़ाक उड़ाना ही है। जातियों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन और धर्म की दुहाई देकर मतदाता को भ्रमित करने की कोशिशें बिहार के इस चुनाव प्रचार में लगातार हुई हैं। यहीं यह बात भी गौर करने लायक है कि चुनाव में ठोस मुद्दे उठाने के बजाय किसी ‘जंगल राज’ और वोटों की कथित ‘चोरी’ जैसी बातों का सहारा लेना राजनीतिक दलों को कहीं अधिक उपयोगी लगा है।
सत्तारूढ़ पक्ष से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपनी उपलब्धियों को आधार बनाकर मतदाता के समक्ष वोट मांगने जायेगा। पर देखा यह गया है कि सत्तारूढ़ पक्ष विपक्ष की बीस साल की पुरानी सरकार के ‘जंगल-राज’ का डर दिखाकर वोट पाने की उम्मीद कर रहा है। यह मान भी लें कि लालू-राबड़ी की सरकार का कथित जंगल-राज बहुत बुरा था, तब भी यह सवाल तो उठता ही है कि आज की युवा पीढ़ी को दो दशक पुराने उस अनुभव के आधार पर कोई निर्णय लेने के लिए कैसे कहा जा सकता है? विपक्ष से यदि कोई सवाल किया जाता है तो वह यह होना चाहिए कि उसके पास शासन का बेहतर विकल्प क्या है? यह मतदाता का अपमान नहीं तो और क्या है कि बिहार की वर्तमान सरकार की दस हज़ार रुपये की ‘रिश्वत’ के मुकाबले में विपक्ष तीस हज़ार रुपये नकद देने का प्रलोभन दे रहा है?
चुनाव जनतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होते हैं। रेवड़ियों, रिश्वत और घिसे-पिटे आरोपों के सहारे चुनाव जीतने की कल्पना ही इस उत्सव की गरिमा, महत्ता और पवित्रता को नष्ट कर देती है। यह सचमुच हैरानी की बात है कि नीतियों और नीयत के बजाय समाज को बांटने वाले नारों को चुनाव जीतने का आधार बनाया जाता है।
चुनाव का परिणाम क्या होगा यह तो आने वाला कल ही बतायेगा, पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि सुदृढ़ जनतंत्र की दुहाई देने वाले देश में घटिया मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाना अपने आप में किसी शर्म से कम नहीं है। सत्तारूढ़ पक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा बीस साल पुरानी सरकार की कथित विफलता थी और विपक्ष ने भी ठोस वैकल्पिक नीतियों को सामने रखने के बजाय ‘वोट चोरी’ जैसे कमजोर मुद्दे को अपना हथियार बनाया। विपक्ष ने बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दे को उठाया अवश्य, पर मतदाता में यह विश्वास नहीं जगा पाया कि वह बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था दे सकता है। इसी तरह सत्तारूढ़ पक्ष का ‘घुसपैठियों’ वाला मुद्दा भी बहुत ज्यादा कारगर नहीं लगा। वह इस सवाल का जवाब देने में भी विफल रहा कि उसके इक्कीस साल के शासन में वह घुसपैठियों को देश से निकाल क्यों नहीं पाया? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि इतने सारे घुसपैठिये देश में आ कैसे गये? इस सवाल का जवाब देश के गृहमंत्री को देना था, पर उनके पास जवाब था ही नहीं! हैरानी की बात तो यह है कि विपक्ष भी उस मज़बूती के साथ इस सवाल को नहीं उठा पाया, जो इस मुद्दे का लाभ उठाने के लिए ज़रूरी थी।
चुनाव-परिणाम भले ही कुछ भी हों, लेकिन सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष दोनों ने चुनाव-प्रचार के दौरान कुल मिलाकर घटिया रण-नीति का ही परिचय दिया है। जनतंत्र की सफलता का तकाज़ा है कि स्वस्थ राजनीति की संभावनाओं को साकार बनाने की दिशा में कुछ ठोस सोचा जाये, कुछ ठोस किया जाये। यह दुर्भाग्य ही है कि ‘ठोस’ के नाम पर हमारे पास घटिया शब्दावली, घटिया नारे और घटिया तौर-तरीके हैं।
बात सिर्फ बिहार के इन चुनावों तक ही सीमित नहीं है। हमारी राजनीति में सब जगह यह गिरावट आई है। एक तरह की गुरिल्ला शैली अपना ली है राजनेताओं ने– झपट्टा मार कर कहीं निकल जाओ वाली शैली। कुछ भी कह कर, कुछ भी कर के उसे भुला देना इस शैली की विशेषता है। मान लिया गया है कि मतदाता की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। यह स्थिति बदलनी चाहिए। राजनेताओं की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगना ही चाहिए कि जुमलों के सहारे चुनाव जीता जा सकता है। राजनेताओं को यह अहसास कराया ही जाना चाहिए कि जनता को अपनी मुट्ठी में समझने की उनकी प्रवृत्ति देश के जागरूक मतदाता को स्वीकार नहीं है। जनतांत्रिक मूल्यों- मर्यादाओं का तकाज़ा है कि नेता अपनी सीमाएं समझें और जनता अपनी शक्ति को पहचाने। यह चिंता की बात है कि स्वस्थ राजनीति की जगह घटिया जुमलों वाली बीमार राजनीति पर हावी होती जा रही है। मान लिया गया है कि युद्ध और प्यार की तरह राजनीति में भी सब कुछ जायज है। चुनाव-दर-चुनाव यह स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। राजनेताओं के इस विश्वास के खोखलेपन को उजागर करना ही होगा कि वे जो कहेंगे-करेंगे जनता उसे स्वीकार कर लेगी।
सतत जागरूकता जनतंत्र के बने रहने की सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी शर्त है। हमारी राजनीति के झंडाबरदार इस शर्त को झुठलाने पर लगे हैं। बिहार के इस चुनाव-प्रचार के दौरान राजनीतिक घटियापन का एक कीर्तिमान ही स्थापित हुआ है। चुनाव-परिणाम चाहे कुछ भी हों, इस बात की चिंता तो देश के जागरूक नागरिक को करनी ही होगी कि हमारी राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है–इस गिरावट को रोकना ही होगा।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।