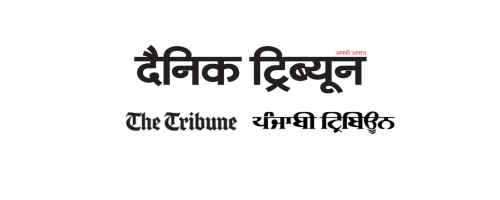आज अतीत में झांकने का वक्त है। हमारी पीढ़ी के लिए इसका मतलब है आज़ादी के उदय को देखना। हमारी वह पीढ़ी जिसे उन दिनों इस बात का कोई इल्म ही नहीं था कि आजादी के पूर्ण प्रभाव का अर्थ क्या होता है। आज़ादी की उस सुबह के बाद हम इसकी किरणों के तले पले-बढ़े हुए हैं। हम अपने माता-पिता से सुनते थे कि इस आज़ादी से उनके काम-धंधे और तौर-तरीके में किस तरह के बदलाव आये। सरकारी और सामाजिक स्तरों पर भेदभाव बंद हो गया था और भारत की जनता अपने मामलों की कर्ता-धर्ता स्वयं बन गयी थी।
लोकतंत्र, स्वतंत्रता और बराबरी का सबसे बढ़िया अनुभव उन लोगों को ही होता है जो इन अधिकारों से वंचित से रखे गये। पिछली सदी के चालीसवेंें दशक के अंत और पचासवें के शुरू में हम जैसे स्कूली बच्चों को नयी-नवेली मिली आज़ादी की कहानियां, देश के बंटवारे की कहानियां सुनाई जाती थीं। दूसरा विश्वयुद्ध कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ था परंतु यह शीतयुद्ध की शुरुआत थी। पहली बार परमाणु अस्त्र इस्तेमाल किये गये और इनके साथ ही अमेरिका और रूस की सेनाओं का भय हृदय में घर कर लेता था। आज़ादी का अहसास फिर भी हो ही जाता था क्योंकि पुरानी औपनिवेशिक शक्तियां युद्ध की तबाही में अपनी-अपनी ऊर्जा और मानवशक्ति गंवा कर एक-एक करके वापस जा रही थीं। साथ ही दुनियाभर में आज़ादी और लोकतंत्र के ध्वज फहराये जा रहे थे। इसके साथ ही रूस और चीन की साम्यवाद की बदलती विचारधारा आगे आ रही थी, जिसकी लपेट में लगभग समस्त पूर्वी यूरोप आ रहा था। इसके बाद जाे कुछ भी हुआ वह अब भले ही इतिहास का अंग है फिर भी यह तो कहना ही होगा कि यूरोप के बड़े हिस्से का नेतृत्व प्रतिस्पर्धा में पड़ी इन दोनों विचारधाराओं ने किया। उधर राष्ट्रमंडल और उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में कल्याणकारी शासन का दबदबा रहा। ऐसे मंजर में हमारे आयु वर्ग ने पढ़ाई की और फिर रोजगार हासिल किया। इस उम्र वर्ग में देशभक्ति का जज्बा जोश मार रहा था और अपने बड़े-बुजुर्गों के पदचिन्हों पर चलने की अभिलाषा भी हमारे भीतर थी। व्यवसाय का चुनाव करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। दसवीं पास करने के बाद सशस्त्र बलों की पृष्ठभूमि वाले नौजवान नेशनल डिफेंस अकादमी में दाखिला ले लेते थे, जबकि अन्य युवाआें को मेडिकल या इंजीनियरिंग में से किसी एक का चुनाव करना होता था। हमारे में से कई एक आर्ट-ह्यूमेनिटीज़ वर्ग का चुनाव कर लेते थे जिसके बाद करिअर बनाने के लिए सिविल सर्विसेज या फिर अध्यापन के व्यवसाय का चुनाव करना पड़ता था। विद्यार्थियों की संख्या के दृष्टिगत उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाओं की संख्या उन दिनों ज्यादा नहीं होती थी। देश की कुल आबादी लगभग 34 करोड़ थी (जो बढ़कर अब 140 करोड़ को छू रही है) पर इस आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में रहता था, जिसकी शिक्षा तक पहुंच नाममात्र या बिल्कुल ही नहीं थी। परिणामस्वरूप मामूली सी शिक्षा हासिल करने वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती थी। शुरू के कुछ वर्षों के बाद जब धीरे-धीरे सार्वजनिक क्षेत्र इस मैदान में प्रवेश करने लगा तब प्रोफेशनल, हुनरमंद वर्ग के लिए नये रास्ते खुलने लगे। प्राइवेट सेक्टर महज दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, हैदराबाद और चेन्नई जैसे कुछ महानगरों तक सीमित था। शहरों और कस्बों में मध्यम स्तर के उद्योग स्थापित होने लगे और इसके साथ ही इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन स्नातक करने वाले युवा ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में जाने लगे। आतिथ्य सत्कार क्षेत्र तीव्रता से चमकने लगा और यह भी युवाओं का पसंदीदा ठिकाना बनने लगा। शहरों और कस्बों की व्यवस्था ठीक-ठाक चल रही थी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन अभी शुरू नहीं हुआ था। कृषि ग्रामीण आबादी के जीवनयापन का मुख्य साधन था और रोजी-रोटी का एकमात्र हुनर रखने वाले छोटे-छोटे टुकड़ों की जमीन वाले लोगों का साधन भी खेतीबाड़ी ही था। लोहार, बढ़ई, मिस्त्री और कृषि श्रमिक भी खेतीबाड़ी पर ही निर्भर थे। यह सभी वर्ग एक इकाई की भांति एक-दूसरे पर निर्भर थे। किसान लोग फसलों की बुआई और कटाई के वक्त दो बार उक्त वर्गों को नकदी या वस्तु के तौर पर मेहनताना भी दिया करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी चलती थी।
भले ही मैं एक आदर्श किस्म की तस्वीर तो नहीं खींचना चाहता परंतु यह सच्चाई है कि उस दौर में इतनी ज्यादा असमानता नहीं थी जो आज समाज में देखने को मिलती है। शहरों में झोपड़पट्टियां या झुग्गी कॉलोनियां नहीं थीं। भिन्न-भिन्न आर्थिक दर्जे के तबके तो मौजूद थे परंतु जिंदगी बहुत सादगीनुमा थी, और गैरबराबरी का तो नामोनिशान नहीं था।
हरित क्रांति ने शुरुआती दौर में कृषि को खूब प्रोत्साहित किया लेकिन यह बहुत देर तक नहीं चल सका। क्योंकि खेतीबाड़ी-उत्पादन की दर से आबादी की वृद्धि अधिक तेजी से हो रही थी। कालांतर में दिन-प्रतिदिन कृषि भूमि टुकड़ों में बंटने लगी और आमदन में भी गिरावट दिखाई देने लगी। ग्रामीण युवा वर्ग नौकरियों की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे। सबसे पहले अकुशल श्रमिक गांवों से निकलकर फैक्टरी जैसे कामधंधों में लग गये। उसके बाद अर्द्धकुशल श्रमिकों ने भी शहरों का रुख करना शुरू कर दिया जिससे शहरी क्षेत्रों में उनकी आबादी बढ़ने लगी। उनमें से कई एक को नौकरियां भी मिलीं जबकि बाकी बेरोजगार ही रह गये। गांवों में जीवनयापन और कठिन होने के साथ ही पलायन में वृद्धि होने लगी जिसके परिणामस्वरूप शहरों का बुनियादी ढांचा चरमराने लगा। जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि और पलायन के परिणामस्वरूप शहरों में झोपड़पट्टियां बनने लगीं, अपराध, नामुराद बीमारियां घर करने लगीं और गरीबी व लाचारी के कुरूप अमानवीय चरित्र सामने आने लगे। वक्त के इस दौर में जनता वोट बैंक के रूप में चुनावी मंसूबों के लिए सियासी दलों के चंगुल में फंसने लगी। शिक्षा का ढांचा, विशेषकर ग्रामीण भारत में समय की गति के साथ विकसित न हो पाया। शिक्षण्ा संस्थाओं का काम नवीनतम टेक्नोलॉजी से सुसज्जित योग्य प्रोफेशनल पैदा करना ही नहीं होता बल्कि ऐसे विद्यार्थी तैयार करना होता है जो आंतरिक सोच-विचार का सामर्थ्य रखते हों। परंतु अगले दौर में जो निकला वह था रट्टामार स्कूल और (कुछेक को छोड़कर) निम्न स्तर की अनेक संस्थाएं। आज भी यह तथ्य पूर्णत: सामने है। इसमें बदलाव लाने के लिए ऐसे अध्यापकों की दरकार है जो बच्चों की रुचि को निखार सकते हों। हमारे विश्वविद्यालयों में उच्च स्तर के अध्यापन वर्ग और अनुसंधान सुविधाओं की आवश्यकता है। नोबेल पुरस्कार जीतने और चोटी के ज्यादातर एग्जिक्यूटिव विकसित देशों के विश्वविद्यालयों से ही होते हैं। जब मैं यूपीएससी (2002-07) में था तो हमें बताया गया था कि आईआईटीज़ (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) में अध्यापकों के 30 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं। मुझे तो यह भय है कि अब जबकि आईआईटीज़ की संख्या और बढ़ गयी है तो रिक्त पदों की स्थिति और बदतर होना तो स्वाभाविक ही होगा। अब बताइये, अध्यापकों की अनुपस्थिति में आईआईटीज़ खोलने से भला क्या फायदा? इसी तरह सर्वव्यापी स्वास्थ्य प्रणाली यकीनी बनाने की आवश्यकता है।
अब आखिर हम चलें किस ओर? जहां बढ़ती आबादी का दबाव हो और 50 प्रतिशत से अधिक आबादी को गेहूं और चावल देकर उनका जीवन चलाना पड़ रहा हो, ऐसे में हम एक पर्याप्त आमदनी वाला देश कैसे बन सकते हैं। इसका उत्तर शिक्षा और सेहत के क्षेत्र में ढूंढ़ना होगा। ऐसे दौर में जहां सभी सियासी दल रियायती सुख-सुविधाएं देने की होड़ में हों तो कराेड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर हम कैसे निकाल सकेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हमारे युवा वर्ग के सामर्थ्य और कारोबारी प्रमुखों के अनुभव में ही ढूंढ़ा जा सकता है। जब तक हमारे अिधकतर नौजवान अपने जीवन को सुधारने के लिए विदेशी सरजमीं की ओर देखते रहेंगे तब तक हमारी लीडरशिप हमें नाकाम ही करती रहेगी, इससे बौद्धिक शक्ति का निकास जारी रहेगा और हम धक्के ही खाते रहेंगे। याद रहे कि जी-7 देशों की आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव दुनिया के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों पर टिकी हुई है। उनके ऐसे संस्थान हैं जाे विश्व की होनहार प्रतिभाओंं को अपनी ओर आकर्षित करने के योग्य हैं। इसी वजह से उन देशों के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रणाली मौजूद है। हम विदेशों में सफलता के झंडे फहराने वाले युवाओं की ओर आशा भरी नजरों से देखते हैं लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि दरअसल प्रवासी होने के बावजूद ये विद्यार्थी वहां की शिक्षण संस्थाओं एवं अनुसंधान सुविधाओं की बदौलत उपलब्धियां हासिल करने योग्य बनते हैं।
आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे युवा उद्यमियों को लालफीताशाही के भंवर में फंसाया जा रहा है और ऐसे में उनकी समस्त रचनात्मकता दम तोड़ देती है? आखिर उन्हें ‘एक लाइसेंस’ की खातिर अंतहीन प्रतीक्षा में खड़े क्यों रहना पड़ता है? सरकार की भूमिका तो रास्ता साफ करने वाली होनी चाहिए। क्या नौकरशाही और सियासी नेतृत्व को आवश्यक माहौल तैयार करने में मददगार नहीं होना चाहिए? इसके लिए किसी बजट की जरूरत नहीं बल्कि सही वातावरण निर्मित करने और प्रोत्साहित करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। युवा वर्ग ऐसी नींव होते हैं जिस पर देशों का निर्माण किया जाता है और यह नींव शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रोत्साहन से ही मजबूत होती है। एक दिन मैं किसी विदेशी चैनल पर ताईवान की एक प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनी के सीईओ का इंटरव्यू सुन रहा था। जब उससे पूछा गया कि विश्व का सबसे बेहतरीन सेमीकंडक्टर तैयार करने का रहस्य आखिर है क्याzwj;? तो उसका दोटूक जवाब था- ‘शिक्षा’… स्कूली स्तर से लेकर उच्च स्तर तक बस केवल शिक्षा। उसका इंटरव्यू सुनने के बाद अगर आप अपने शहर या गांव के निकटवर्ती सरकारी स्कूल में जाकर देखें तो आपको पता चल जायेगा कि आखिर हमारे अंडर ग्रेजुएट विदेशों की ओर पलायन कर क्यों रहे हैं। हम इस कमी के लिए जीडीपी, महंगाई एवं विदेशी मुद्रा भंडार इत्यादि के आंकड़ों का भले ही कितना ही तर्क-वितर्क देते रहें, मगर बेरोजगारों, शिक्षितों और अशिक्षित युवाओं के लिए यह महज खोखले शब्द ही माने जायेंगे। नये भारत के लिए हमें शिक्षित, स्वस्थ और सजग युवा तैयार करने और एक नये दृष्टिकोण एवं नये संकल्प की जरूरत है। ऐसे नौजवान ही हमें विश्व मंच पर अपना सही लक्ष्य दिला सकते हैं। लब्बोलुआब यह है कि हमें सेहत और शिक्षा की उत्साहजनक एवं महत्वाकांक्षी योजना और राष्ट्रीय स्तर पर ढांचा बनाने की जरूरत है, जिससे लाखों लोगों को नौकरियां मिल सकें और देश विकास के रास्ते पर पेशकदमी कर सके। मैं अपने विचार एफडीआर की नयी डील की पंक्तियों से समाप्त करना चाहूंगा जैसा कि एफडीआर ने कहा ‘हम अपने युवाओं के लिए भविष्य का निर्माण हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन हम भविष्य के लिए युवाओं को तैयार अवश्य कर सकते हैं।’
लेखक यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एवं मणिपुर के पूर्व राज्यपाल हैं।