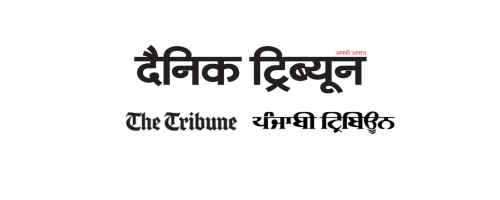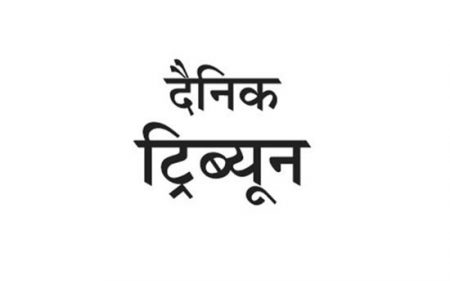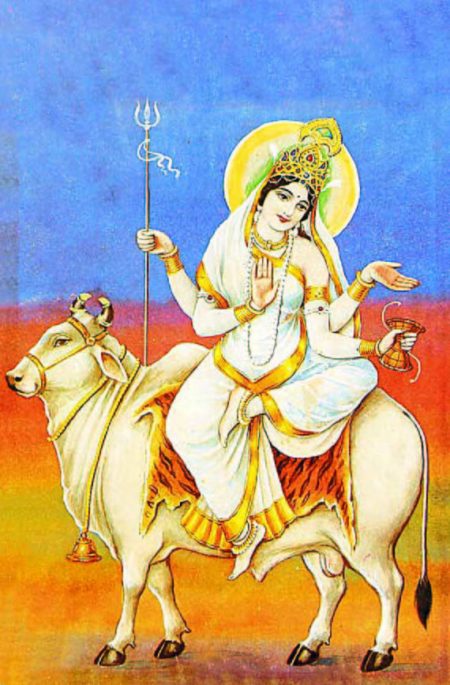अशोक ‘प्रवृद्ध’
वैदिक मतानुसार जीवित चेतन पितरों अर्थातzwj;् जीते हुए ज्ञानी पुरुषों का श्रद्धापूर्वक भोजनादि से सत्कार करना श्राद्ध करना है। वैदिक मत में जीवित चेतन पितरों, ज्ञाननिष्ठ सत्त्वगुणी पुरुषों का, जो लोक-नाम स्थान है, वही पितृलोक है। जिस प्रदेश में मानस कर्म में प्रधान विचारशील ज्ञानी लोग निवास करते हैं, वह पितृलोक है अथवा उन पितरों के समुदाय मेल का नाम पितृलोक है। पौराणिक ग्रन्थों में जिनके लिये मरने के पश्चात शास्त्रों में पितृलोक में जाना लिखा है, वे शरीर छोड़ने के पश्चात पितृजनों के समुदाय अथवा प्रदेश में अर्थातzwj;् पितरों के घरों में जाकर जन्म लेते हैं। मनुस्मृति में उत्पादक, यज्ञोपवीत कराने वाला, विद्यादाता, अन्नदाता और भय से बचाने वाला, ये पांच पिता माने गये हैं। इस प्रकार पितृ शब्द योगरूढ़ है, और अपने उत्पादक पिता में रूढ़ि भी है। लौकिक व्यवहार में पिता शब्द से प्रकरणानुसार जनक, यज्ञोपवीत कराने, अन्न देने व भय से बचाने वाले का ग्रहण होता है। परन्तु श्राद्ध कर्म में विशेषकर पितृ शब्द से विद्यादाता का ग्रहण होता है। अपने उत्पादक पिता की सेवा शुश्रूषा तो सबको सदैव करनी ही चाहिए। ज्ञान अथवा विद्या देने वाले ज्ञानी पिता का भी भोजनादि से प्रतिदिन सत्कार करना चाहिए, वही श्राद्ध है।
श्राद्ध कर्म में पूजने योग्य दो ही हैं– पितृ और देव। वाणी के कर्म में प्रवीण, पढ़ाने और उपदेश करने में सदा प्रवृत्त अर्थातzwj;् पढ़ाने और उपदेशादि वाणी के कर्म द्वारा विद्या का प्रचार करके जगत का उपकार करने के लिए प्रतिक्षण प्रवृत्त पुरुष देवता कहलाते हैं। वाकzwj;्, वाणी, सरस्वती, विद्या आदि एकार्थक शब्दों के मद्देनजर विद्यावान लोगों को देव मानना सैद्धांतिक रूप से ठीक ही है। मानसकर्म ज्ञान में सदा रमण करने, मन ही मन में शुद्ध आनन्द की लहरियों का अनुभव करने, अच्छे-बुरे का सदा विवेक से निर्णय करने, अल्पभाषी, अथवा वाणी को वश में करके मौन रहने वाले, जगत के उपकार हेतु सम्यकzwj;् ज्ञान व अनुभव प्राप्त विषयों को सरल कर प्रचलित करने वाले पितर हैं।
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जिनमें सत्य बोलना, हितकारी वाक्य बोलना, प्रियवाणी बोलना और वेदादिशास्त्र पढ़ना इन्हीं चार प्रसंगों में वाणी का व्यय करना, किन्तु क्रोधादिपूर्वक नहीं बोलना ये गुण जिनमें हो वे देव हैं। और मानस विचार में तत्पर रहें अर्थातzwj;् मन के तीन दोष– किसी दूसरे की वस्तु को लेने की तृष्णा, दूसरों का अनिष्ट विचार और व्यर्थ असम्भव विचारndash; ये दोष जिनमें न हों तथा मानस तीन गुण– सब प्राणियों पर दया, निरपेक्ष व संतोष और शुभकर्मों परमात्मा की उपासनादि में श्रद्धाभक्ति, जिनमें विशेष कर हों, वे पितर कहलाते हैं। जिनकी वाणी सब प्रकार शुद्ध है, वे देव और जिनका मन सब प्रकार शुद्ध है, वे पितृ कहलाते हैं। मानस विचार की रक्षा वाणी से होती है, इसीलिए पितृ कार्य का रक्षक देवकार्य को माना है, तथा देव को ऋषि और पितृ को मुनि भी कहा जाता है।
मनुस्मृति तृतीय अध्याय श्राद्ध प्रकरण में कहा गया है कि सत्त्वगुण की प्रधानता होने से बुद्धिवर्द्धक तथा खाने योग्य कव्य पदार्थों को प्रयत्न के साथ ज्ञानियों को खिलाना चाहिए और होमने योग्य वस्तु चारों प्रकार के विद्वानों को खिलानी चाहिए। उपनिषदों में भी कहा गया है– आत्मज्ञानी की पूजा करें। उपनिषदों के इस वचन से भी ज्ञानी लोगों का ही सत्कार सिद्ध होता है। सत्य-असत्य का विवेक करने वाले ज्ञानीजनों की सम्यकzwj;् श्रद्धा, भक्ति से सेवा करने वाले सेवकों पर प्रसन्न होकर वे कल्याण करने के लिए मन लगाते हैं। श्रेष्ठमार्ग उपदेश से जता देते हैं कि यह काम ऐसे करना चाहिए। इसी कारण ज्ञानयुक्त पितृजनों की अन्नादि दान से श्रद्धापूर्वक सेवा-शुश्रूषा करनी चाहिए। प्राणियों का प्राण अन्न के ही आश्रय होने के कारण सब सत्कारों में भोजनार्थ अन्न से सत्कार करना ही सबमें मुख्य माना गया है। इसीलिए तर्पण और श्राद्ध में अन्न, जल से सत्कार करना मुख्य है।
कालान्तर में वैदिक ज्ञान से दूर होने से तर्पण व श्राद्ध की इस प्राचीन परम्परा में विकृति आ गई, और मृत्यु को प्राप्त लोगों के नाम से पिंड देने की परम्परा चल पड़ी। वैदिक विद्वान वेदविरोधी इन प्रसंगों को प्रक्षिप्त मानते हैं और कहते हैं कि भोजन से ज्ञानी पितृ लोगों का श्राद्ध करना अत्यन्त उचित है।
पौराणिक मत में आश्विन कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर अमावस्या तक की अवधि को पितृपक्ष माना जाता है। इस काल में पितरों के लिए श्रद्धा से श्राद्ध करना पुण्यकर्म माना गया है। मनुस्मृति के अनुसार नित्य अन्न, जल, दूध अथवा खीर, फल और कन्दमूलों से पितृ नाम ज्ञानी पुरुषों का प्रीतिपूर्वक श्रद्धा से सत्कार करें।
पाणिनीय सूत्र में श्राद्धे शरदः कहा गया है। इस सूत्र का आशय यह है कि ऋतुवाचक शरद शब्द से श्राद्ध अर्थ में ठञzwj;् प्रत्यय होता है। शरद ऋतु में नैमित्तिक श्राद्ध की विशेषता समझनी चाहिए। अर्थातzwj;् साधनों के ठीक-ठीक न मिलने आदि पर श्राद्ध का नैमित्तिक करना कहा गया है। भोजन करने योग्य वस्तु सर्वोपरि उत्तम पदार्थ, वस्तु सब दूध से बनते हैं। और वर्षा ऋतु के होने से गौ आदि पशुओं के भक्ष्य घासादि की अधिकता से दूध अधिक उत्पन्न होता है। श्राद्ध में खीर आदि पुष्ट वस्तुओं का विधान किया गया है। अन्नों के बीच उत्तम माने जाने वाले चावल भी वर्षा की अधिकता से शरद ऋतु में ही उत्पन्न होते हैं। वर्तमान में श्राद्ध नित्य कर्म के रूप में कम और नैमित्तिक कर्म के रूप में ही होता ज्यादा दिखाई देता है।